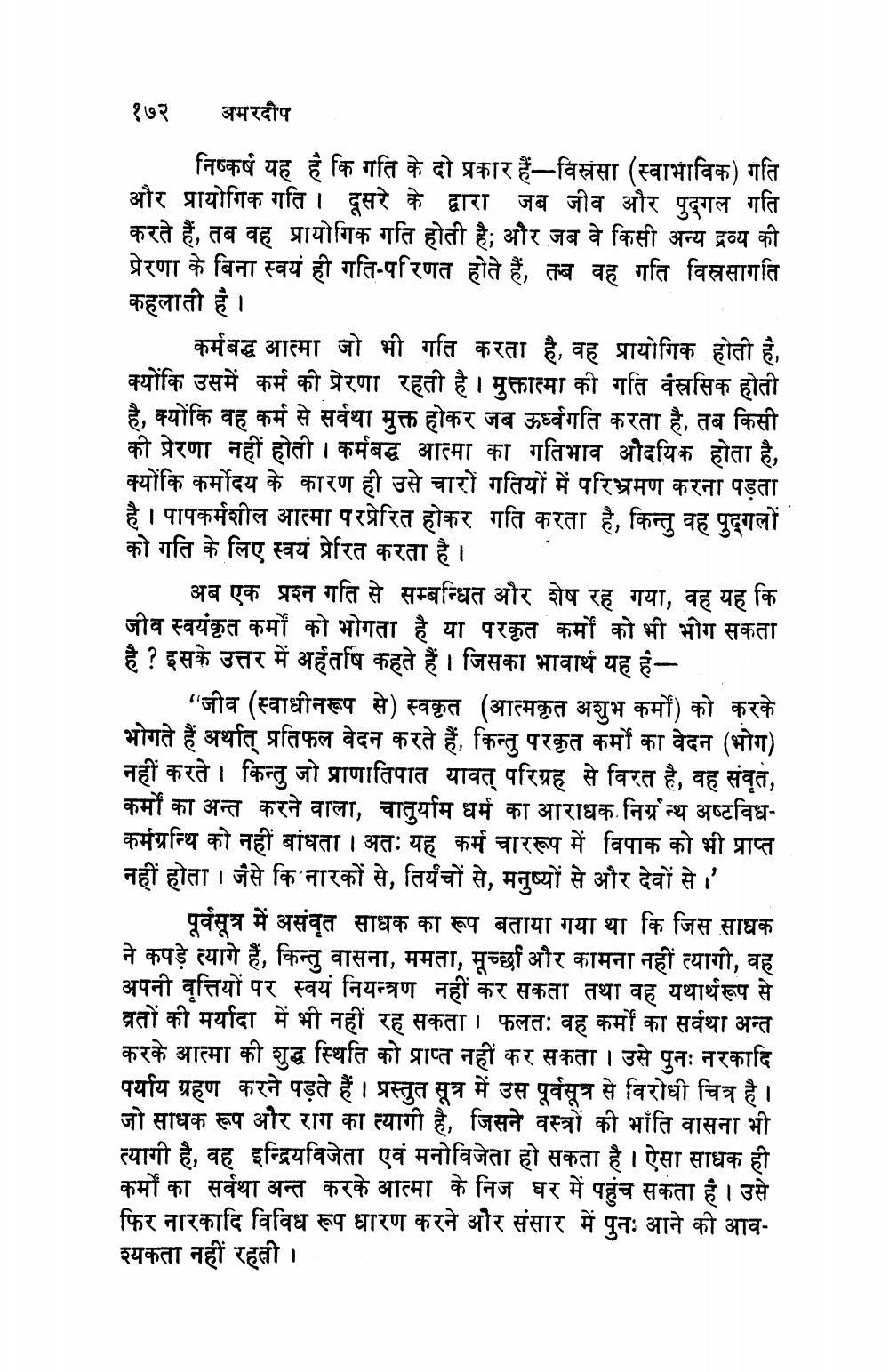________________
१७२ अमरदीप
निष्कर्ष यह है कि गति के दो प्रकार हैं- विस्रंसा ( स्वाभाविक ) गति और प्रायोगिक गति । दूसरे के द्वारा जब जीव और पुद्गल गति करते हैं, तब वह प्रायोगिक गति होती है; और जब वे किसी अन्य द्रव्य की प्रेरणा के बिना स्वयं ही गति-परिणत होते हैं, तब वह गति विस्रसागति कहलाती है ।
कर्मबद्ध आत्मा जो भी गति करता है, वह प्रायोगिक होती है, क्योंकि उसमें कर्म की प्रेरणा रहती है । मुक्तात्मा की गति वैत्रसिक होती है, क्योंकि वह कर्म से सर्वथा मुक्त होकर जब ऊर्ध्वगति करता है, तब किसी की प्रेरणा नहीं होती । कर्मबद्ध आत्मा का गतिभाव औदयिक होता है, क्योंकि कर्मोदय के कारण ही उसे चारों गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है । पापकर्मशील आत्मा परप्रेरित होकर गति करता है, किन्तु वह पुद्गलों को गति के लिए स्वयं प्रेरित करता है ।
अब एक प्रश्न गति से सम्बन्धित और शेष रह गया, वह यह कि जीव स्वयंकृत कर्मों को भोगता है या परकृत कर्मों को भी भोग सकता है ? इसके उत्तर में अर्हतषि कहते हैं । जिसका भावार्थ यह है
" जीव (स्वाधीनरूप से) स्वकृत ( आत्मकृत अशुभ कर्मों) को करके भोगते हैं अर्थात् प्रतिफल वेदन करते हैं, किन्तु परकृत कर्मों का वेदन (भोग) नहीं करते । किन्तु जो प्राणातिपात यावत् परिग्रह से विरत है, वह संवृत, कर्मों का अन्त करने वाला, चातुर्याम धर्म का आराधक निर्ग्रन्थ अष्टविधकर्मग्रन्थि को नहीं बांधता । अतः यह कर्म चाररूप में विपाक को भी प्राप्त नहीं होता । जैसे कि नारकों से, तिर्यंचों से, मनुष्यों से और देवों से ।'
पूर्वसूत्र में असंवृत साधक का रूप बताया गया था कि जिस साधक नेकपड़े त्यागे हैं, किन्तु वासना, ममता, मूर्च्छा और कामना नहीं त्यागी, वह अपनी वृत्तियों पर स्वयं नियन्त्रण नहीं कर सकता तथा वह यथार्थ रूप से व्रतों की मर्यादा में भी नहीं रह सकता । फलतः वह कर्मों का सर्वथा अन्त करके आत्मा की शुद्ध स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता । उसे पुनः नरकादि पर्याय ग्रहण करने पड़ते हैं । प्रस्तुत सूत्र में उस पूर्वसूत्र से विरोधी चित्र है । जो साधक रूप और राग का त्यागी है, जिसने वस्त्रों की भाँति वासना भी त्यागी है, वह इन्द्रियविजेता एवं मनोविजेता हो सकता है । ऐसा साधक ही कर्मों का सर्वथा अन्त करके आत्मा के निज घर में पहुंच सकता है । उसे फिर नारकादि विविध रूप धारण करने और संसार में पुनः आने की आवश्यकता नहीं रहती ।