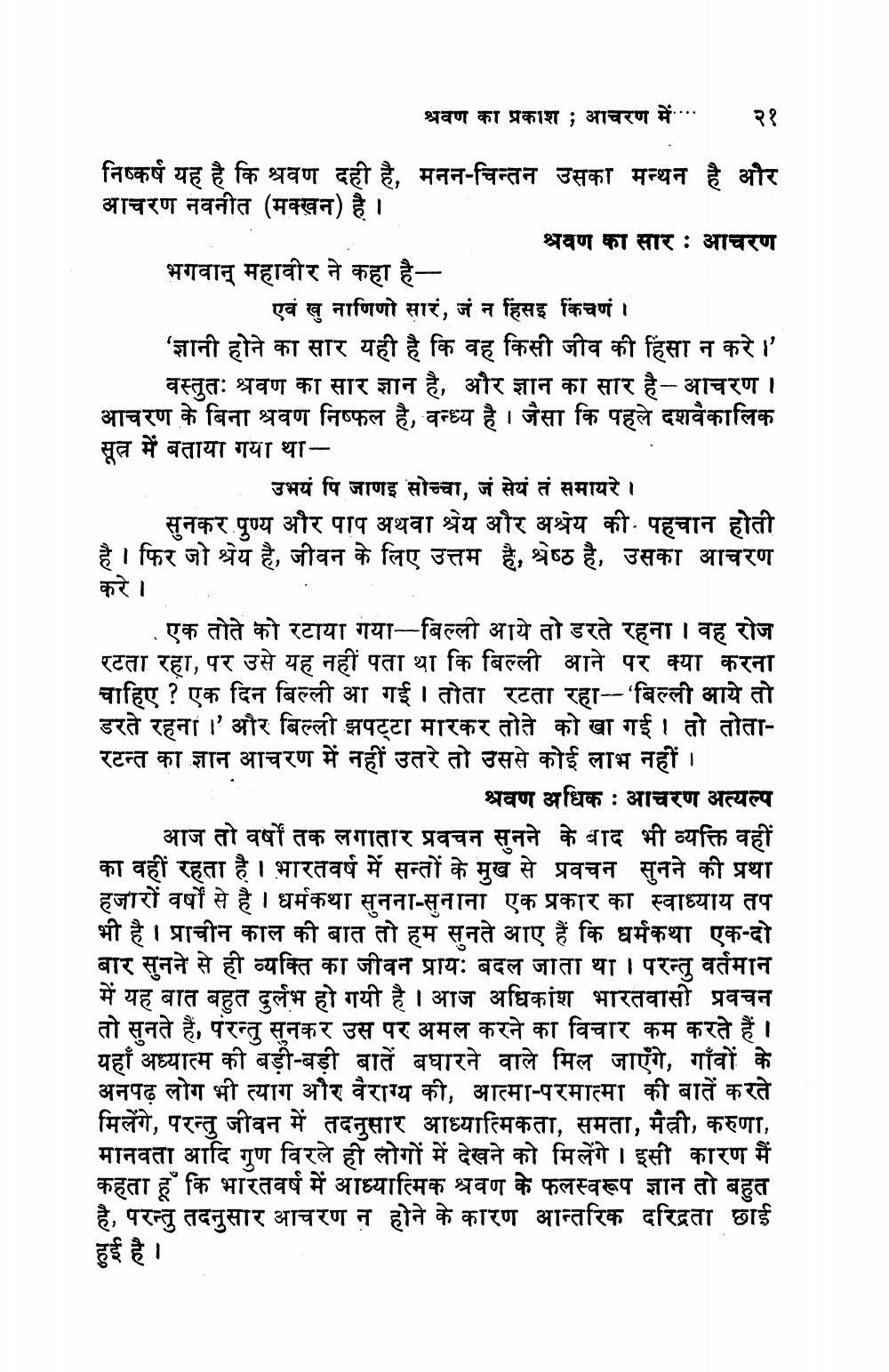________________
श्रवण का प्रकाश ; आचरण में ...
२१
निष्कर्ष यह है कि श्रवण दही है, मनन-चिन्तन उसका मन्थन है और आचरण नवनीत (मक्खन) है।
श्रवण का सार : आचरण भगवान् महावीर ने कहा है
एवं खु नाणिणो सारं, जं न हिंसइ किंचणं । 'ज्ञानी होने का सार यही है कि वह किसी जीव की हिंसा न करे।'
वस्तुतः श्रवण का सार ज्ञान है, और ज्ञान का सार है-आचरण । आचरण के बिना श्रवण निष्फल है, वन्ध्य है । जैसा कि पहले दशवैकालिक सूत्र में बताया गया था
उभयं पि जाणइ सोच्चा, जं सेयं तं समायरे । सुनकर पुण्य और पाप अथवा श्रेय और अश्रेय की. पहचान होती है। फिर जो श्रेय है, जीवन के लिए उत्तम है, श्रेष्ठ है, उसका आचरण करे।
एक तोते को रटाया गया-बिल्ली आये तो डरते रहना । वह रोज रटता रहा, पर उसे यह नहीं पता था कि बिल्ली आने पर क्या करना चाहिए ? एक दिन बिल्ली आ गई। तोता रटता रहा-'बिल्ली आये तो डरते रहना।' और बिल्ली झपट्टा मारकर तोते को खा गई। तो तोतारटन्त का ज्ञान आचरण में नहीं उतरे तो उससे कोई लाभ नहीं।
श्रवण अधिक : आचरण अत्यल्प आज तो वर्षों तक लगातार प्रवचन सुनने के बाद भी व्यक्ति वहीं का वहीं रहता है । भारतवर्ष में सन्तों के मुख से प्रवचन सुनने की प्रथा हजारों वर्षों से है । धर्मकथा सुनना-सुनाना एक प्रकार का स्वाध्याय तप भी है । प्राचीन काल की बात तो हम सुनते आए हैं कि धर्मकथा एक-दो बार सुनने से ही व्यक्ति का जीवन प्रायः बदल जाता था। परन्तु वर्तमान में यह बात बहुत दुर्लभ हो गयी है । आज अधिकांश भारतवासी प्रवचन तो सुनते हैं, परन्तु सुनकर उस पर अमल करने का विचार कम करते हैं । यहाँ अध्यात्म की बड़ी-बड़ी बातें बघारने वाले मिल जाएंगे, गाँवों के अनपढ़ लोग भी त्याग और वैराग्य की, आत्मा-परमात्मा की बातें करते मिलेंगे, परन्तु जीवन में तदनुसार आध्यात्मिकता, समता, मैत्री, करुणा, मानवता आदि गुण विरले ही लोगों में देखने को मिलेंगे। इसी कारण मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष में आध्यात्मिक श्रवण के फलस्वरूप ज्ञान तो बहुत है, परन्तु तदनुसार आचरण न होने के कारण आन्तरिक दरिद्रता छाई