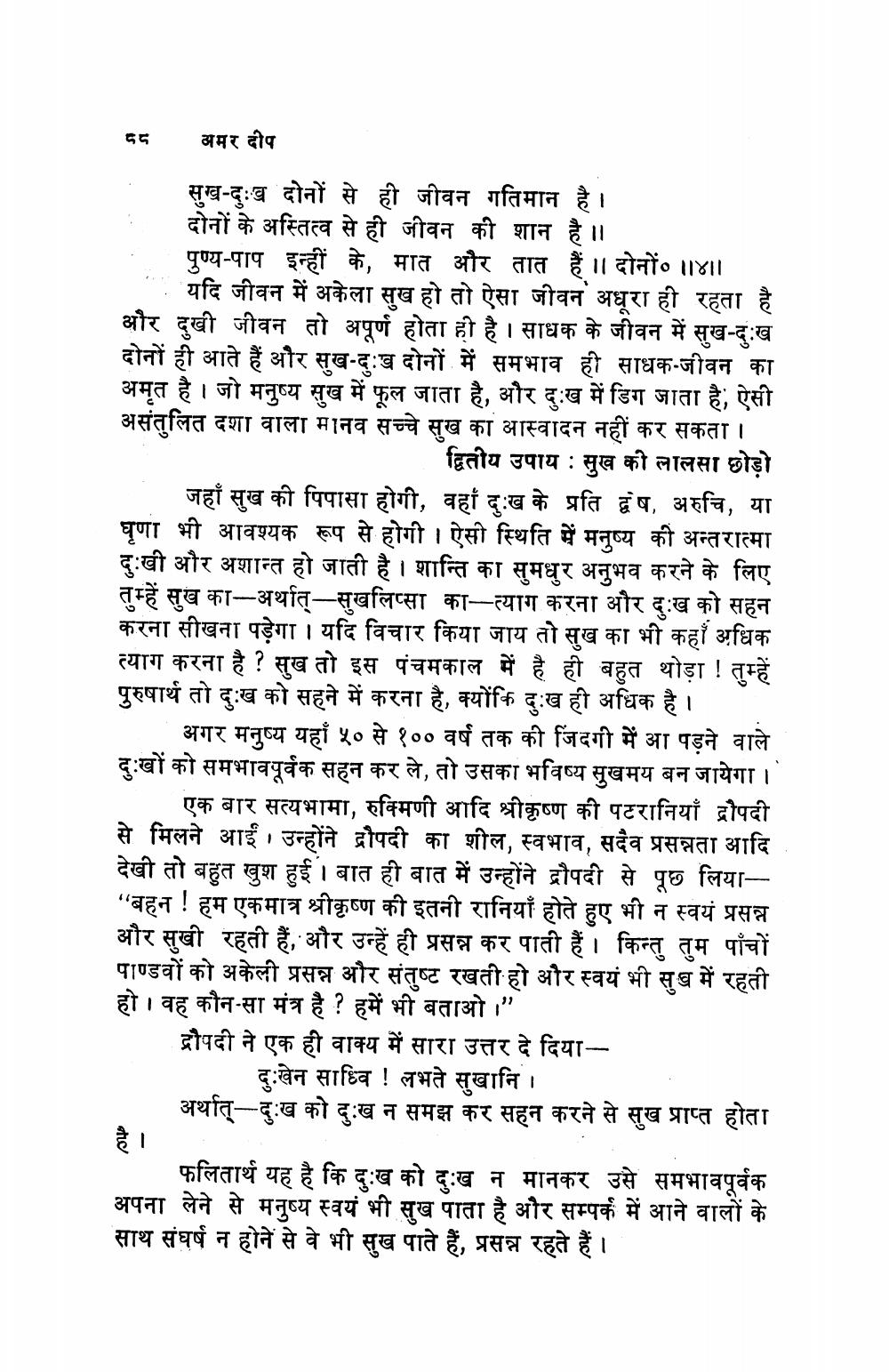________________
८८
अमर दीप
सुख-दुःख दोनों से ही जीवन गतिमान है। दोनों के अस्तित्व से ही जीवन की शान है। पुण्य-पाप इन्हीं के, मात और तात हैं। दोनों ॥४॥ . यदि जीवन में अकेला सुख हो तो ऐसा जीवन अधूरा ही रहता है और दुखी जीवन तो अपूर्ण होता ही है । साधक के जीवन में सुख-दुःख दोनों ही आते हैं और सुख-दुःख दोनों में समभाव ही साधक-जीवन का अमृत है । जो मनुष्य सुख में फूल जाता है, और दुःख में डिग जाता है, ऐसी असंतुलित दशा वाला मानव सच्चे सुख का आस्वादन नहीं कर सकता।
द्वितीय उपाय : सुख की लालसा छोड़ो जहाँ सुख की पिपासा होगी, वहाँ दुःख के प्रति द्वेष, अरुचि, या घणा भी आवश्यक रूप से होगी। ऐसी स्थिति में मनुष्य की अन्तरात्मा दुःखी और अशान्त हो जाती है। शान्ति का सुमधुर अनुभव करने के लिए तुम्हें सुख का-अर्थात्-सुखलिप्सा का त्याग करना और दुःख को सहन करना सीखना पड़ेगा। यदि विचार किया जाय तो सुख का भी कहाँ अधिक त्याग करना है ? सुख तो इस पंचमकाल में है ही बहुत थोड़ा ! तुम्हें पुरुषार्थ तो दुःख को सहने में करना है, क्योंकि दुःख ही अधिक है। _ अगर मनुष्य यहाँ ५० से १०० वर्ष तक की जिंदगी में आ पड़ने वाले दुःखों को समभावपूर्वक सहन कर ले, तो उसका भविष्य सुखमय बन जायेगा।
एक बार सत्यभामा, रुक्मिणी आदि श्रीकृष्ण की पटरानियाँ द्रौपदी से मिलने आईं। उन्होंने द्रौपदी का शील, स्वभाव, सदैव प्रसन्नता आदि देखी तो बहुत खुश हुई। बात ही बात में उन्होंने द्रौपदी से पूछ लिया"बहन ! हम एकमात्र श्रीकृष्ण की इतनी रानियाँ होते हुए भी न स्वयं प्रसन्न और सुखी रहती हैं, और उन्हें ही प्रसन्न कर पाती हैं। किन्तु तुम पाँचों पाण्डवों को अकेली प्रसन्न और संतुष्ट रखती हो और स्वयं भी सुख में रहती हो । वह कौन-सा मंत्र है ? हमें भी बताओ।" द्रौपदी ने एक ही वाक्य में सारा उत्तर दे दिया
दुःखेन साध्वि ! लभते सुखानि ।। अर्थात्-दुःख को दुःख न समझ कर सहन करने से सुख प्राप्त होता
फलितार्थ यह है कि दुःख को दुःख न मानकर उसे समभावपूर्वक अपना लेने से मनुष्य स्वयं भी सुख पाता है और सम्पर्क में आने वालों के साथ संघर्ष न होने से वे भी सुख पाते हैं, प्रसन्न रहते हैं।