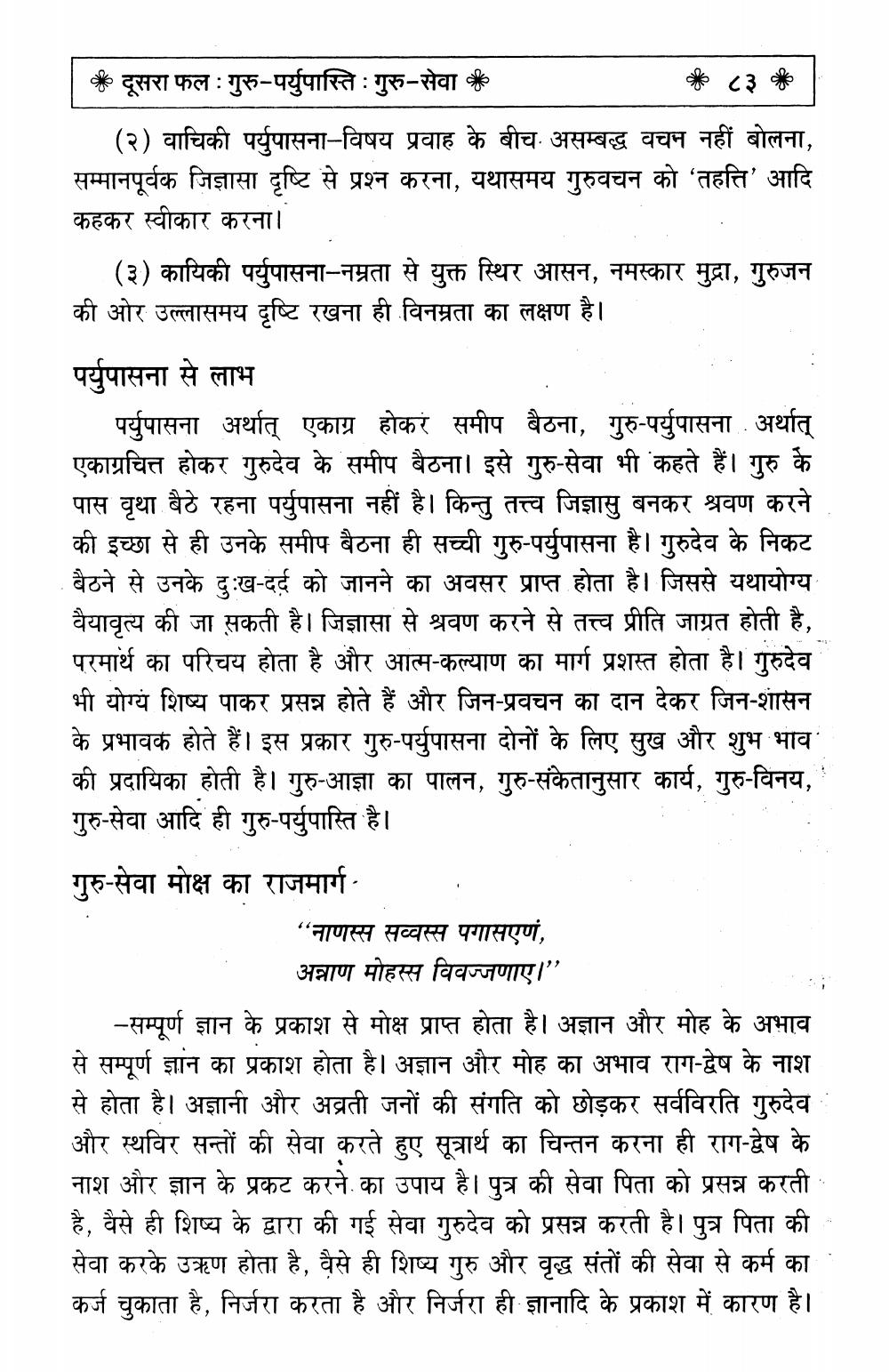________________
* दूसरा फल : गुरु-पर्युपास्ति : गुरु-सेवा *
* ८३ * (२) वाचिकी पर्युपासना-विषय प्रवाह के बीच असम्बद्ध वचन नहीं बोलना, सम्मानपूर्वक जिज्ञासा दृष्टि से प्रश्न करना, यथासमय गुरुवचन को 'तहत्ति' आदि कहकर स्वीकार करना।
(३) कायिकी पर्युपासना-नम्रता से युक्त स्थिर आसन, नमस्कार मुद्रा, गुरुजन की ओर उल्लासमय दृष्टि रखना ही विनम्रता का लक्षण है। पर्युपासना से लाभ
पर्युपासना अर्थात् एकाग्र होकर समीप बैठना, गुरु-पर्युपासना अर्थात् एकाग्रचित्त होकर गुरुदेव के समीप बैठना। इसे गुरु-सेवा भी कहते हैं। गुरु के पास वृथा बैठे रहना पर्युपासना नहीं है। किन्तु तत्त्व जिज्ञासु बनकर श्रवण करने की इच्छा से ही उनके समीप बैठना ही सच्ची गुरु-पर्युपासना है। गुरुदेव के निकट बैठने से उनके दुःख-दर्द को जानने का अवसर प्राप्त होता है। जिससे यथायोग्य वैयावृत्य की जा सकती है। जिज्ञासा से श्रवण करने से तत्त्व प्रीति जाग्रत होती है, परमार्थ का परिचय होता है और आत्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। गुरुदेव भी योग्य शिष्य पाकर प्रसन्न होते हैं और जिन-प्रवचन का दान देकर जिन-शासन के प्रभावक होते हैं। इस प्रकार गुरु-पर्युपासना दोनों के लिए सुख और शुभ भाव की प्रदायिका होती है। गुरु-आज्ञा का पालन, गुरु-संकेतानुसार कार्य, गुरु-विनय, गुरु-सेवा आदि ही गुरु-पर्युपास्ति है। गुरु-सेवा मोक्ष का राजमार्ग. .
__“नाणस्स सव्वस्स पगासएणं,
अन्नाण मोहस्स विवज्जणाए।" -सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाश से मोक्ष प्राप्त होता है। अज्ञान और मोह के अभाव से सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश होता है। अज्ञान और मोह का अभाव राग-द्वेष के नाश से होता है। अज्ञानी और अव्रती जनों की संगति को छोड़कर सर्वविरति गुरुदेव
और स्थविर सन्तों की सेवा करते हुए सूत्रार्थ का चिन्तन करना ही राग-द्वेष के नाश और ज्ञान के प्रकट करने का उपाय है। पुत्र की सेवा पिता को प्रसन्न करती है, वैसे ही शिष्य के द्वारा की गई सेवा गुरुदेव को प्रसन्न करती है। पुत्र पिता की सेवा करके उऋण होता है, वैसे ही शिष्य गुरु और वृद्ध संतों की सेवा से कर्म का कर्ज चुकाता है, निर्जरा करता है और निर्जरा ही ज्ञानादि के प्रकाश में कारण है।