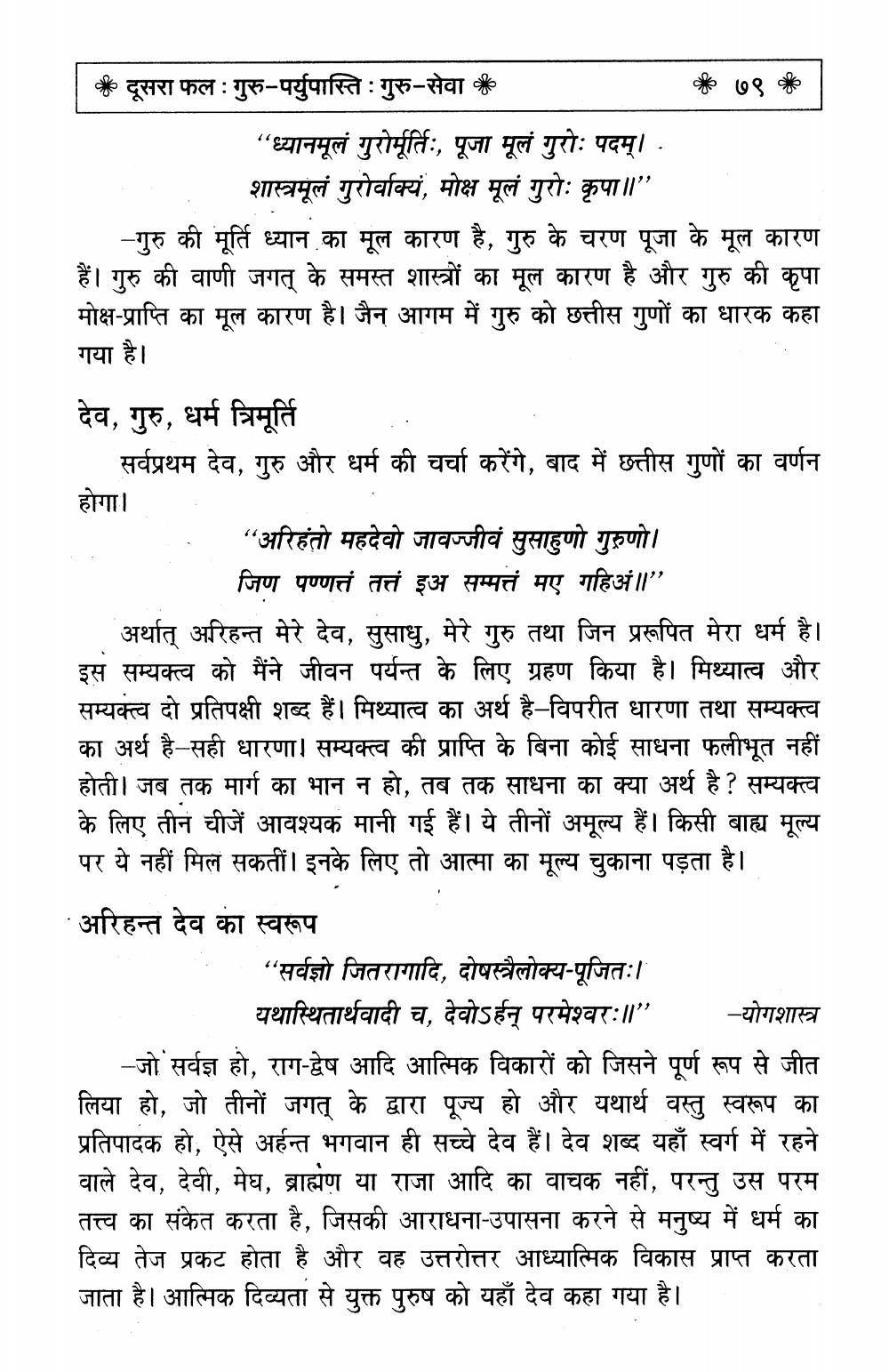________________
दूसरा फल: गुरु- पर्युपास्ति : गुरु-सेवा *
“ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजा मूलं गुरोः पदम् । शास्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरोः कृपा ॥”
- गुरु की मूर्ति ध्यान का मूल कारण है, गुरु के चरण पूजा के मूल कारण हैं। गुरु की वाणी जगत् के समस्त शास्त्रों का मूल कारण है और गुरु की कृपा मोक्ष - प्राप्ति का मूल कारण है। जैन आगम में गुरु को छत्तीस गुणों का धारक कहा गया है।
देव, गुरु, धर्म त्रिमूर्ति
सर्वप्रथम देव, गुरु और धर्म की चर्चा करेंगे, बाद में छत्तीस गुणों का वर्णन होगा।
“अरिहंतो महदेवो जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो ।
जिण पण्णत्तं तत्तं इअ सम्मत्तं मए गहिअं ॥”
७९
अर्थात् अरिहन्त मेरे देव, सुसाधु, मेरे गुरु तथा जिन प्ररूपित मेरा धर्म है। इस सम्यक्त्व को मैंने जीवन पर्यन्त के लिए ग्रहण किया है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दो प्रतिपक्षी शब्द हैं। मिथ्यात्व का अर्थ है - विपरीत धारणा तथा सम्यक्त्व का अर्थ है-सही धारणा । सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना कोई साधना फलीभूत नहीं होती। जब तक मार्ग का भान न हो, तब तक साधना का क्या अर्थ है ? सम्यक्त्व के लिए तीन चीजें आवश्यक मानी गई हैं। ये तीनों अमूल्य हैं। किसी बाह्य मूल्य पर ये नहीं मिल सकतीं। इनके लिए तो आत्मा का मूल्य चुकाना पड़ता है ।
अरिहन्त देव का स्वरूप
“सर्वज्ञो जितरागादि, दोषस्त्रैलोक्य - पूजितः । यथास्थितार्थवादी च, देवोऽर्हन् परमेश्वरः ॥”
- योगशास्त्र
- जो सर्वज्ञ हो, राग-द्वेष आदि आत्मिक विकारों को जिसने पूर्ण रूप से जीत लिया हो, जो तीनों जगत् के द्वारा पूज्य हो और यथार्थ वस्तु स्वरूप का प्रतिपादक हो, ऐसे अर्हन्त भगवान ही सच्चे देव हैं। देव शब्द यहाँ स्वर्ग में रहने वाले देव, देवी, मेघ, ब्राह्मण या राजा आदि का वाचक नहीं, परन्तु उस परम तत्त्व का संकेत करता है, जिसकी आराधना - उपासना करने से मनुष्य में धर्म का दिव्य तेज प्रकट होता है और वह उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास प्राप्त करता जाता है। आत्मिक दिव्यता से युक्त पुरुष को यहाँ देव कहा गया है।