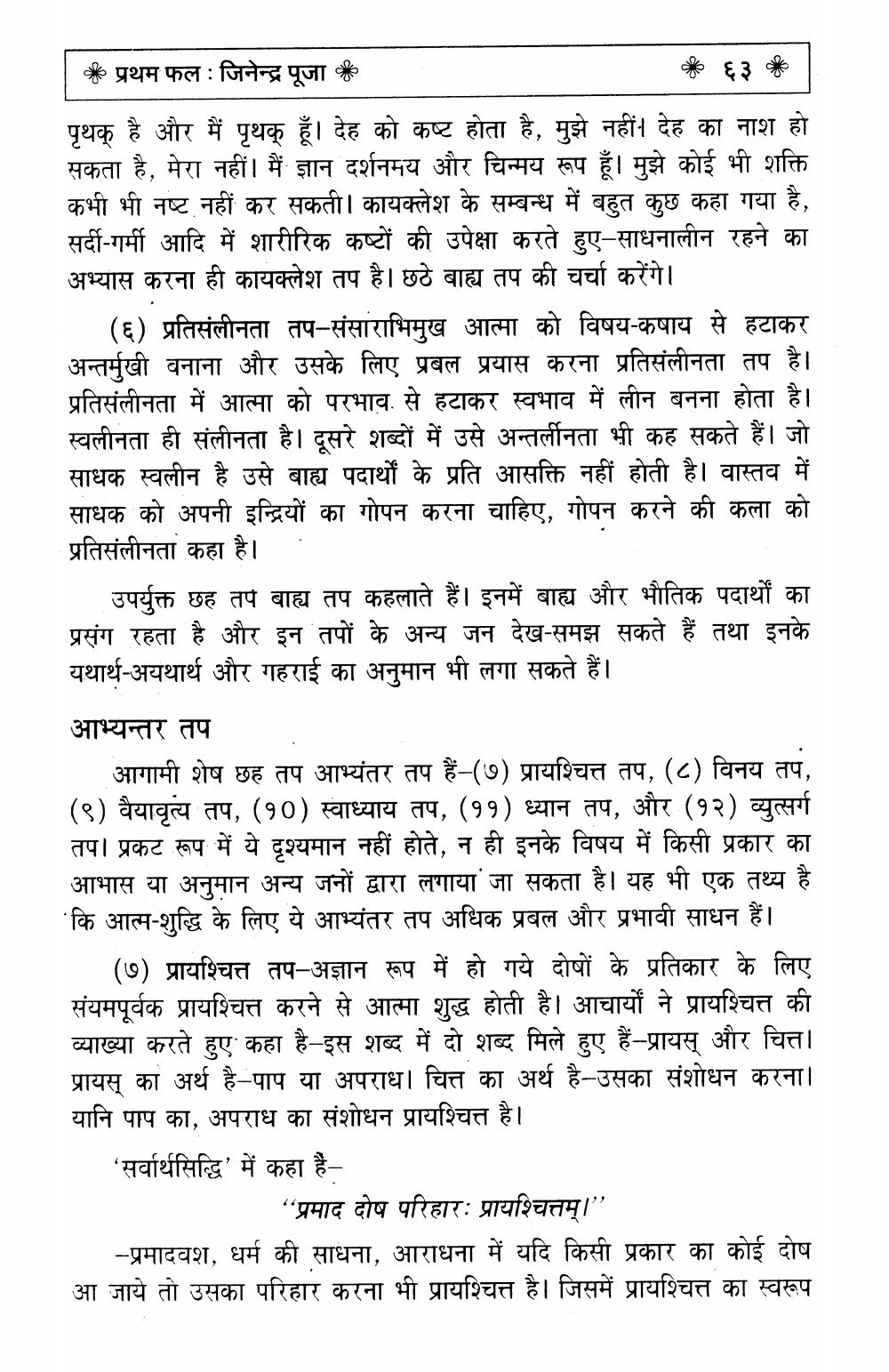________________
* प्रथम फल : जिनेन्द्र पूजा *
* ६३ * पृथक् है और मैं पृथक् हूँ। देह को कष्ट होता है, मुझे नहीं। देह का नाश हो सकता है, मेरा नहीं। मैं ज्ञान दर्शनमय और चिन्मय रूप हूँ। मुझे कोई भी शक्ति कभी भी नष्ट नहीं कर सकती। कायक्लेश के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है, सर्दी-गर्मी आदि में शारीरिक कष्टों की उपेक्षा करते हुए-साधनालीन रहने का अभ्यास करना ही कायक्लेश तप है। छठे बाह्य तप की चर्चा करेंगे।
(६) प्रतिसंलीनता तप-संसाराभिमुख आत्मा को विषय-कषाय से हटाकर अन्तर्मुखी बनाना और उसके लिए प्रबल प्रयास करना प्रतिसंलीनता तप है। प्रतिसंलीनता में आत्मा को परभाव से हटाकर स्वभाव में लीन बनना होता है। स्वलीनता ही संलीनता है। दूसरे शब्दों में उसे अन्तर्लीनता भी कह सकते हैं। जो साधक स्वलीन है उसे बाह्य पदार्थों के प्रति आसक्ति नहीं होती है। वास्तव में साधक को अपनी इन्द्रियों का गोपन करना चाहिए, गोपन करने की कला को प्रतिसंलीनता कहा है। ___ उपर्युक्त छह तप बाह्य तप कहलाते हैं। इनमें बाह्य और भौतिक पदार्थों का प्रसंग रहता है और इन तपों के अन्य जन देख-समझ सकते हैं तथा इनके यथार्थ-अयथार्थ और गहराई का अनुमान भी लगा सकते हैं।
आभ्यन्तर तप
आगामी शेष छह तप आभ्यंतर तप हैं-(७) प्रायश्चित्त तप, (८) विनय तप, (९) वैयावृत्य तप, (१०) स्वाध्याय तप, (११) ध्यान तप, और (१२) व्युत्सर्ग तप। प्रकट रूप में ये दृश्यमान नहीं होते, न ही इनके विषय में किसी प्रकार का आभास या अनुमान अन्य जनों द्वारा लगाया जा सकता है। यह भी एक तथ्य है कि आत्म-शुद्धि के लिए ये आभ्यंतर तप अधिक प्रबल और प्रभावी साधन हैं।
(७) प्रायश्चित्त तप-अज्ञान रूप में हो गये दोषों के प्रतिकार के लिए संयमपूर्वक प्रायश्चित्त करने से आत्मा शुद्ध होती है। आचार्यों ने प्रायश्चित्त की व्याख्या करते हुए कहा है-इस शब्द में दो शब्द मिले हुए हैं-प्रायस् और चित्त। प्रायस् का अर्थ है-पाप या अपराध। चित्त का अर्थ है-उसका संशोधन करना। यानि पाप का, अपराध का संशोधन प्रायश्चित्त है। ___ 'सर्वार्थसिद्धि' में कहा है
“प्रमाद दोष परिहारः प्रायश्चित्तम्।" -प्रमादवश, धर्म की साधना, आराधना में यदि किसी प्रकार का कोई दोष आ जाये तो उसका परिहार करना भी प्रायश्चित्त है। जिसमें प्रायश्चित्त का स्वरूप