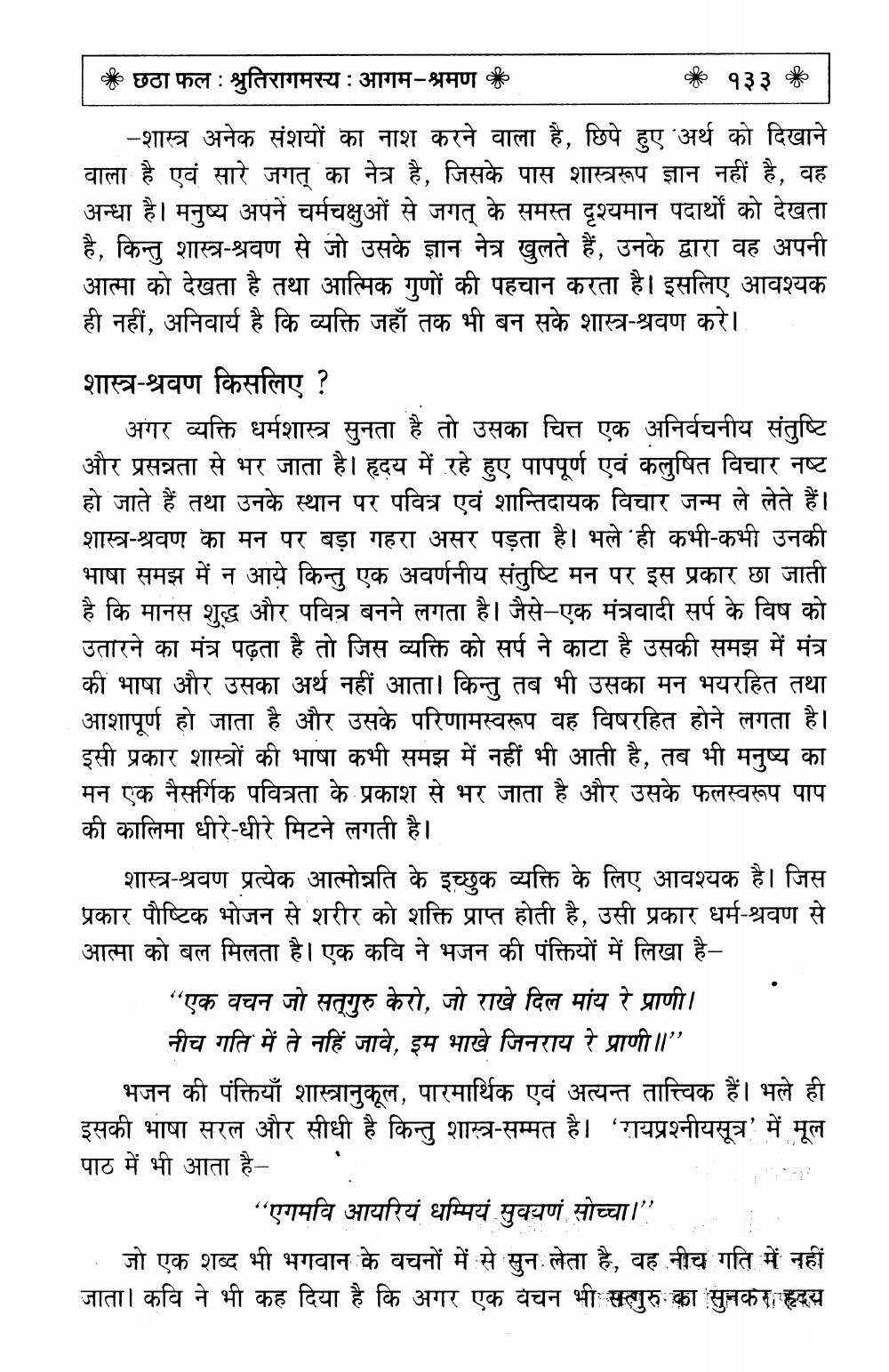________________
| * छठा फल : श्रुतिरागमस्य : आगम-श्रमण *
* १३३ * |
-शास्त्र अनेक संशयों का नाश करने वाला है, छिपे हुए अर्थ को दिखाने वाला है एवं सारे जगत् का नेत्र है, जिसके पास शास्त्ररूप ज्ञान नहीं है, वह अन्धा है। मनुष्य अपने चर्मचक्षुओं से जगत् के समस्त दृश्यमान पदार्थों को देखता है, किन्तु शास्त्र-श्रवण से जो उसके ज्ञान नेत्र खुलते हैं, उनके द्वारा वह अपनी आत्मा को देखता है तथा आत्मिक गुणों की पहचान करता है। इसलिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि व्यक्ति जहाँ तक भी बन सके शास्त्र-श्रवण करे। शास्त्र-श्रवण किसलिए?
अगर व्यक्ति धर्मशास्त्र सुनता है तो उसका चित्त एक अनिर्वचनीय संतुष्टि और प्रसन्नता से भर जाता है। हृदय में रहे हुए पापपूर्ण एवं कलुषित विचार नष्ट हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर पवित्र एवं शान्तिदायक विचार जन्म ले लेते हैं। शास्त्र-श्रवण का मन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। भले ही कभी-कभी उनकी भाषा समझ में न आये किन्तु एक अवर्णनीय संतुष्टि मन पर इस प्रकार छा जाती है कि मानस शुद्ध और पवित्र बनने लगता है। जैसे-एक मंत्रवादी सर्प के विष को उतारने का मंत्र पढ़ता है तो जिस व्यक्ति को सर्प ने काटा है उसकी समझ में मंत्र की भाषा और उसका अर्थ नहीं आता। किन्तु तब भी उसका मन भयरहित तथा आशापूर्ण हो जाता है और उसके परिणामस्वरूप वह विषरहित होने लगता है। इसी प्रकार शास्त्रों की भाषा कभी समझ में नहीं भी आती है, तब भी मनुष्य का मन एक नैसर्गिक पवित्रता के प्रकाश से भर जाता है और उसके फलस्वरूप पाप की कालिमा धीरे-धीरे मिटने लगती है।
शास्त्र-श्रवण प्रत्येक आत्मोन्नति के इच्छुक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार पौष्टिक भोजन से शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार धर्म-श्रवण से आत्मा को बल मिलता है। एक कवि ने भजन की पंक्तियों में लिखा है
“एक वचन जो सत्गुरु केरो, जो राखे दिल मांय रे प्राणी।
नीच गति में ते नहिं जावे, इम भाखे जिनराय रे प्राणी॥" भजन की पंक्तियाँ शास्त्रानुकूल, पारमार्थिक एवं अत्यन्त तात्त्विक हैं। भले ही इसकी भाषा सरल और सीधी है किन्तु शास्त्र-सम्मत है। ‘गयप्रश्नीयसूत्र' में मूल पाठ में भी आता है
“एगमवि आयरियं धम्मियं सुक्यणं सोच्चा।" जो एक शब्द भी भगवान के वचनों में से सुन लेता है, वह नीच गति में नहीं जाता। कवि ने भी कह दिया है कि अगर एक वचन भी सत्गुरु का सुनकर हृदय