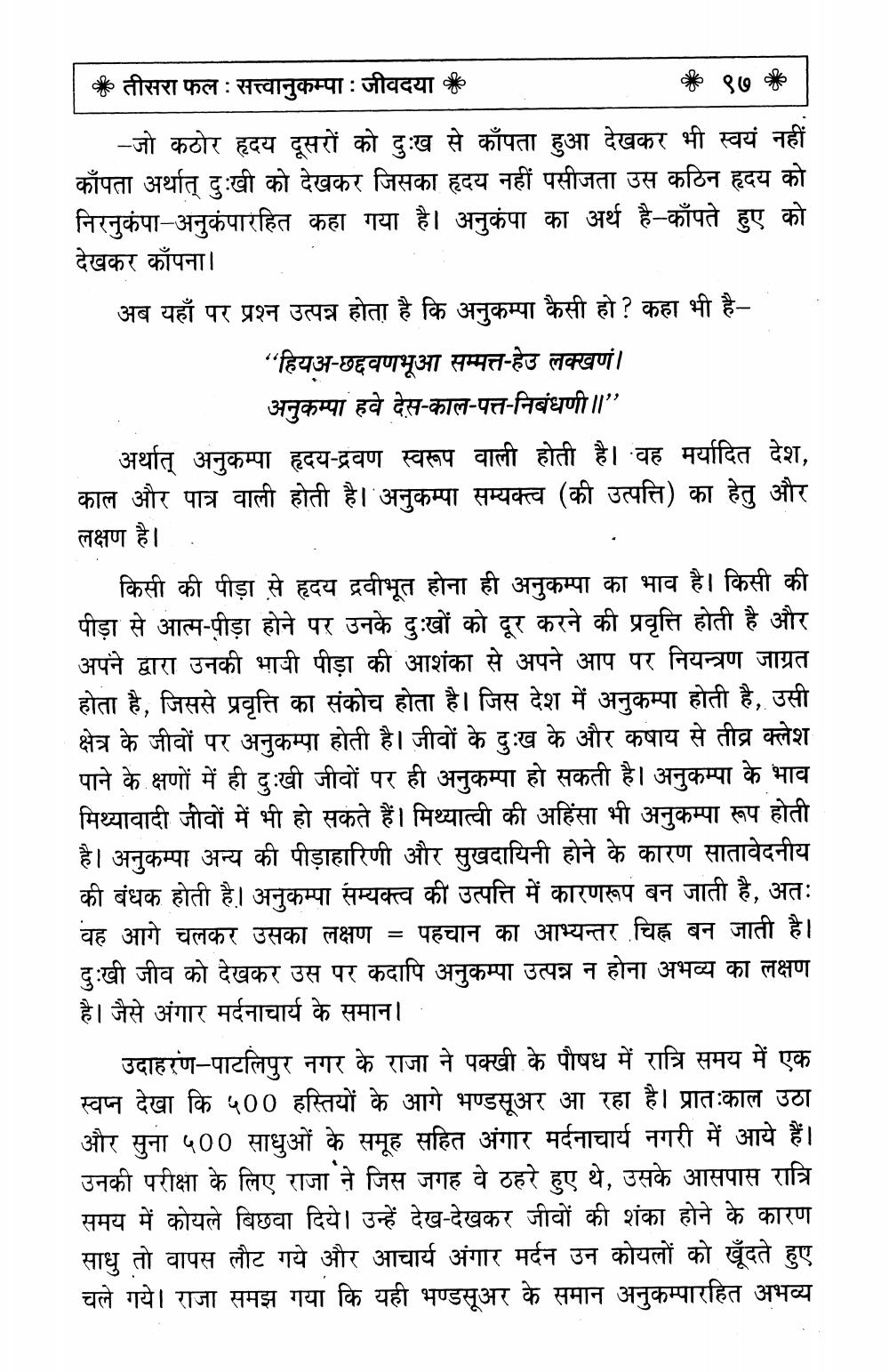________________
| * तीसरा फल : सत्त्वानुकम्पा : जीवदया *
* ९७ * -जो कठोर हृदय दूसरों को दुःख से काँपता हुआ देखकर भी स्वयं नहीं काँपता अर्थात् दुःखी को देखकर जिसका हृदय नहीं पसीजता उस कठिन हृदय को निरनुकंपा-अनुकंपारहित कहा गया है। अनुकंपा का अर्थ है-काँपते हुए को देखकर काँपना। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि अनुकम्पा कैसी हो? कहा भी है
"हियअ-छद्दवणभूआ सम्मत्त-हेउ लक्खणं।
अनुकम्पा हवे देस-काल-पत्त-निबंधणी॥" अर्थात् अनुकम्पा हृदय-द्रवण स्वरूप वाली होती है। वह मर्यादित देश. काल और पात्र वाली होती है। अनुकम्पा सम्यक्त्व (की उत्पत्ति) का हेतु और लक्षण है।
किसी की पीड़ा से हृदय द्रवीभूत होना ही अनुकम्पा का भाव है। किसी की पीड़ा से आत्म-पीड़ा होने पर उनके दुःखों को दूर करने की प्रवृत्ति होती है और अपने द्वारा उनकी भावी पीड़ा की आशंका से अपने आप पर नियन्त्रण जाग्रत होता है, जिससे प्रवृत्ति का संकोच होता है। जिस देश में अनुकम्पा होती है, उसी क्षेत्र के जीवों पर अनुकम्पा होती है। जीवों के दुःख के और कषाय से तीव्र क्लेश पाने के क्षणों में ही दुःखी जीवों पर ही अनुकम्पा हो सकती है। अनुकम्पा के भाव मिथ्यावादी जीवों में भी हो सकते हैं। मिथ्यात्वी की अहिंसा भी अनुकम्पा रूप होती है। अनुकम्पा अन्य की पीड़ाहारिणी और सुखदायिनी होने के कारण सातावेदनीय की बंधक होती है। अनुकम्पा सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारणरूप बन जाती है, अतः वह आगे चलकर उसका लक्षण = पहचान का आभ्यन्तर चिह्न बन जाती है। दुःखी जीव को देखकर उस पर कदापि अनुकम्पा उत्पन्न न होना अभव्य का लक्षण है। जैसे अंगार मर्दनाचार्य के समान।
उदाहरण-पाटलिपुर नगर के राजा ने पक्खी के पौषध में रात्रि समय में एक स्वप्न देखा कि ५00 हस्तियों के आगे भण्डसूअर आ रहा है। प्रातःकाल उठा
और सुना ५00 साधुओं के समूह सहित अंगार मर्दनाचार्य नगरी में आये हैं। उनकी परीक्षा के लिए राजा ने जिस जगह वे ठहरे हुए थे, उसके आसपास रात्रि समय में कोयले बिछवा दिये। उन्हें देख-देखकर जीवों की शंका होने के कारण साधु तो वापस लौट गये और आचार्य अंगार मर्दन उन कोयलों को खूदते हुए चले गये। राजा समझ गया कि यही भण्डसूअर के समान अनुकम्पारहित अभव्य