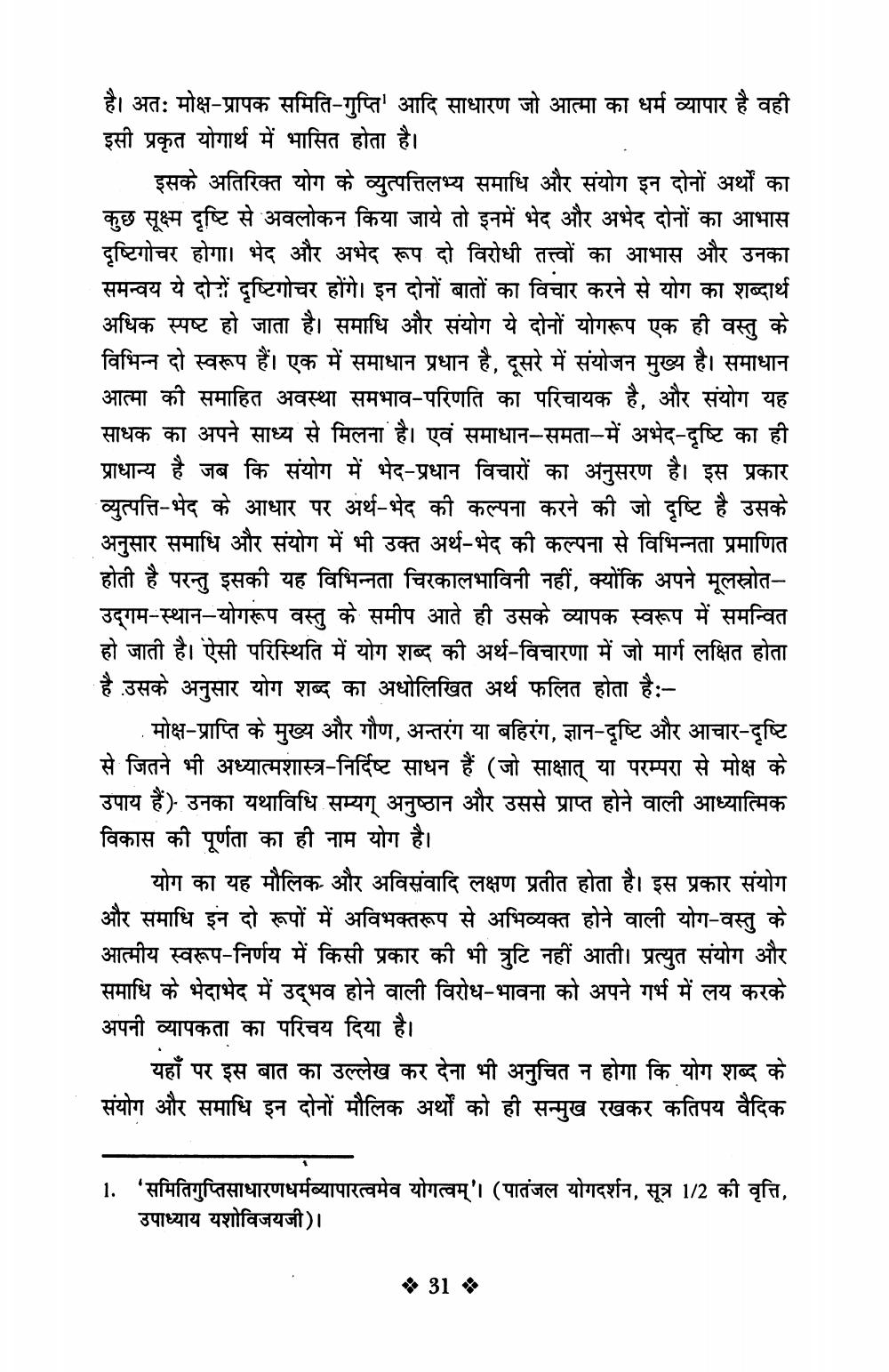________________
है। अतः मोक्ष-प्रापक समिति - गुप्ति' आदि साधारण जो आत्मा का धर्म व्यापार है वही इसी प्रकृत योगार्थ में भासित होता है।
इसके अतिरिक्त योग के व्युत्पत्तिलभ्य समाधि और संयोग इन दोनों अर्थों का कुछ सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाये तो इनमें भेद और अभेद दोनों का आभास दृष्टिगोचर होगा । भेद और अभेद रूप दो विरोधी तत्त्वों का आभास और उनका समन्वय ये दोनों दृष्टिगोचर होंगे। इन दोनों बातों का विचार करने से योग का शब्दार्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है। समाधि और संयोग ये दोनों योगरूप एक ही वस्तु के विभिन्न दो स्वरूप हैं। एक में समाधान प्रधान है, दूसरे में संयोजन मुख्य है। समाधान आत्मा की समाहित अवस्था समभाव - परिणति का परिचायक है, और संयोग यह साधक का अपने साध्य से मिलना है। एवं समाधान - समता - में अभेद - दृष्टि का ही प्राधान्य है जब कि संयोग में भेद - प्रधान विचारों का अनुसरण है। इस प्रकार व्युत्पत्ति-भेद के आधार पर अर्थ-भेद की कल्पना करने की जो दृष्टि है उसके अनुसार समाधि और संयोग में भी उक्त अर्थ-भेद की कल्पना से विभिन्नता प्रमाणित होती है परन्तु इसकी यह विभिन्नता चिरकालभाविनी नहीं, क्योंकि अपने मूलस्रोतउद्गम-स्थान-योगरूप वस्तु के समीप आते ही उसके व्यापक स्वरूप में समन्वित हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में योग शब्द की अर्थ- विचारणा में जो मार्ग लक्षित होता है उसके अनुसार योग शब्द का अधोलिखित अर्थ फलित होता है:
. मोक्ष - प्राप्ति के मुख्य और गौण, अन्तरंग या बहिरंग, ज्ञान- दृष्टि और आचार - दृष्टि से जितने भी अध्यात्मशास्त्र - निर्दिष्ट साधन हैं (जो साक्षात् या परम्परा से मोक्ष के उपाय हैं) उनका यथाविधि सम्यग् अनुष्ठान और उससे प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक विकास की पूर्णता का ही नाम योग है।
योग का यह मौलिक और अविसंवादि लक्षण प्रतीत होता है। इस प्रकार संयोग और समाधि इन दो रूपों में अविभक्तरूप से अभिव्यक्त होने वाली योग-वस्तु के आत्मीय स्वरूप-निर्णय में किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं आती । प्रत्युत संयोग और समाधि के भेदाभेद में उद्भव होने वाली विरोध - भावना को अपने गर्भ में लय करके अपनी व्यापकता का परिचय दिया है।
यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना भी अनुचित न होगा कि योग शब्द के संयोग और समाधि इन दोनों मौलिक अर्थों को ही सन्मुख रखकर कतिपय वैदिक
1. 'समितिगुप्तिसाधारणधर्मव्यापारत्वमेव योगत्वम्'। (पातंजल योगदर्शन, सूत्र 1/2 की वृत्ति, उपाध्याय यशोविजयजी ) ।
❖ 31 ❖