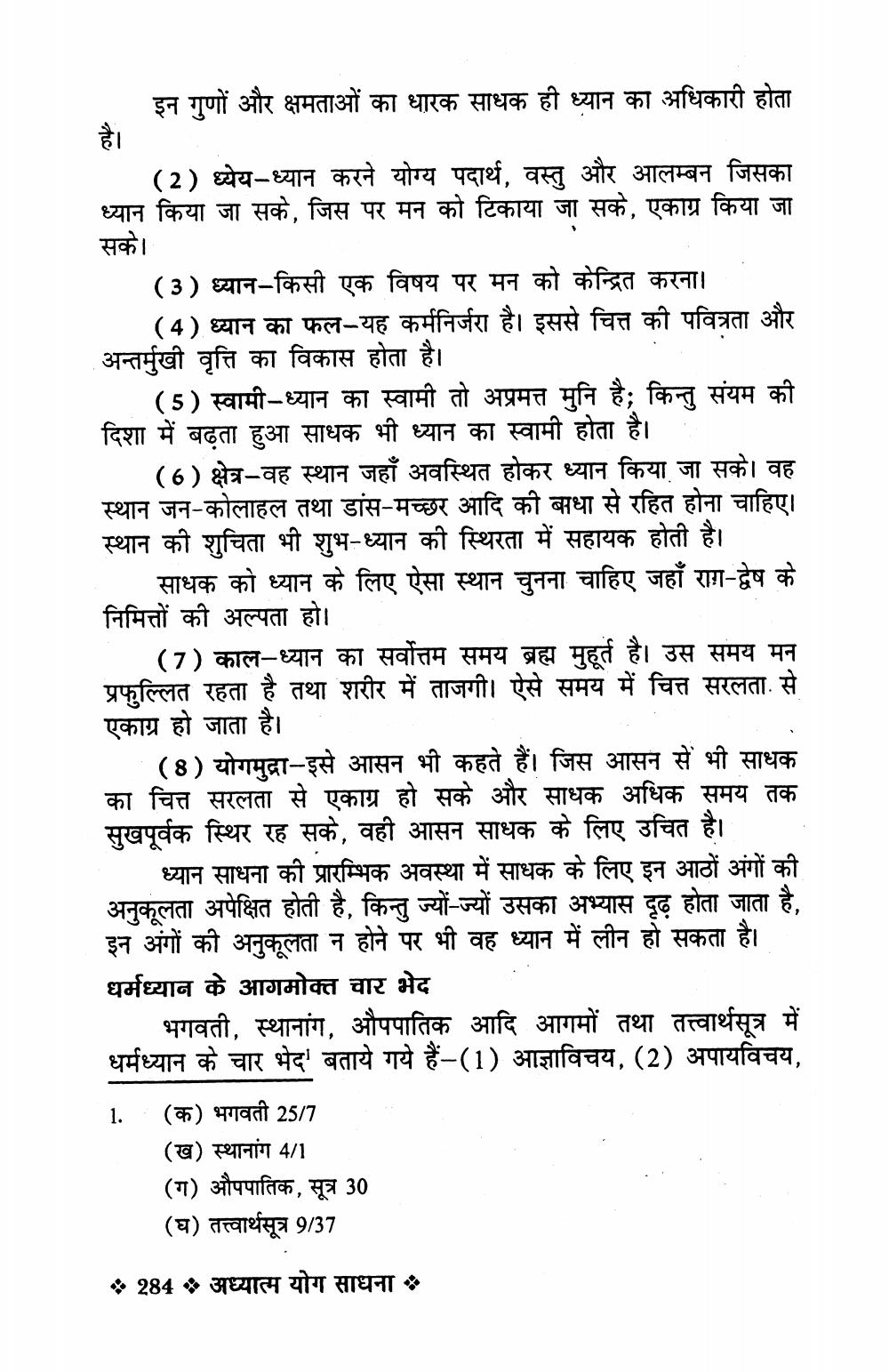________________
इन गुणों और क्षमताओं का धारक साधक ही ध्यान का अधिकारी होता
(2) ध्येय-ध्यान करने योग्य पदार्थ, वस्तु और आलम्बन जिसका ध्यान किया जा सके, जिस पर मन को टिकाया जा सके, एकाग्र किया जा सके।
(3) ध्यान-किसी एक विषय पर मन को केन्द्रित करना।
(4) ध्यान का फल-यह कर्मनिर्जरा है। इससे चित्त की पवित्रता और अन्तर्मुखी वृत्ति का विकास होता है।
(5) स्वामी-ध्यान का स्वामी तो अप्रमत्त मुनि है; किन्तु संयम की दिशा में बढ़ता हुआ साधक भी ध्यान का स्वामी होता है।
(6) क्षेत्र-वह स्थान जहाँ अवस्थित होकर ध्यान किया जा सके। वह स्थान जन-कोलाहल तथा डांस-मच्छर आदि की बाधा से रहित होना चाहिए। स्थान की शुचिता भी शुभ-ध्यान की स्थिरता में सहायक होती है।
साधक को ध्यान के लिए ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ राग-द्वेष के निमित्तों की अल्पता हो।
(7) काल-ध्यान का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय मन प्रफुल्लित रहता है तथा शरीर में ताजगी। ऐसे समय में चित्त सरलता. से एकाग्र हो जाता है। ___(8) योगमुद्रा-इसे आसन भी कहते हैं। जिस आसन से भी साधक का चित्त सरलता से एकाग्र हो सके और साधक अधिक समय तक सुखपूर्वक स्थिर रह सके, वही आसन साधक के लिए उचित है।
ध्यान साधना की प्रारम्भिक अवस्था में साधक के लिए इन आठों अंगों की अनुकूलता अपेक्षित होती है, किन्तु ज्यों-ज्यों उसका अभ्यास दृढ़ होता जाता है, इन अंगों की अनुकूलता न होने पर भी वह ध्यान में लीन हो सकता है। धर्मध्यान के आगमोक्त चार भेद।
भगवती, स्थानांग, औपपातिक आदि आगमों तथा तत्त्वार्थसूत्र में धर्मध्यान के चार भेद बताये गये हैं-(1) आज्ञाविचय, (2) अपायविचय, 1. (क) भगवती 25/7
(ख) स्थानांग 4/1 (ग) औपपातिक, सूत्र 30 (घ) तत्त्वार्थसूत्र 9/37
*284 अध्यात्म योग साधना