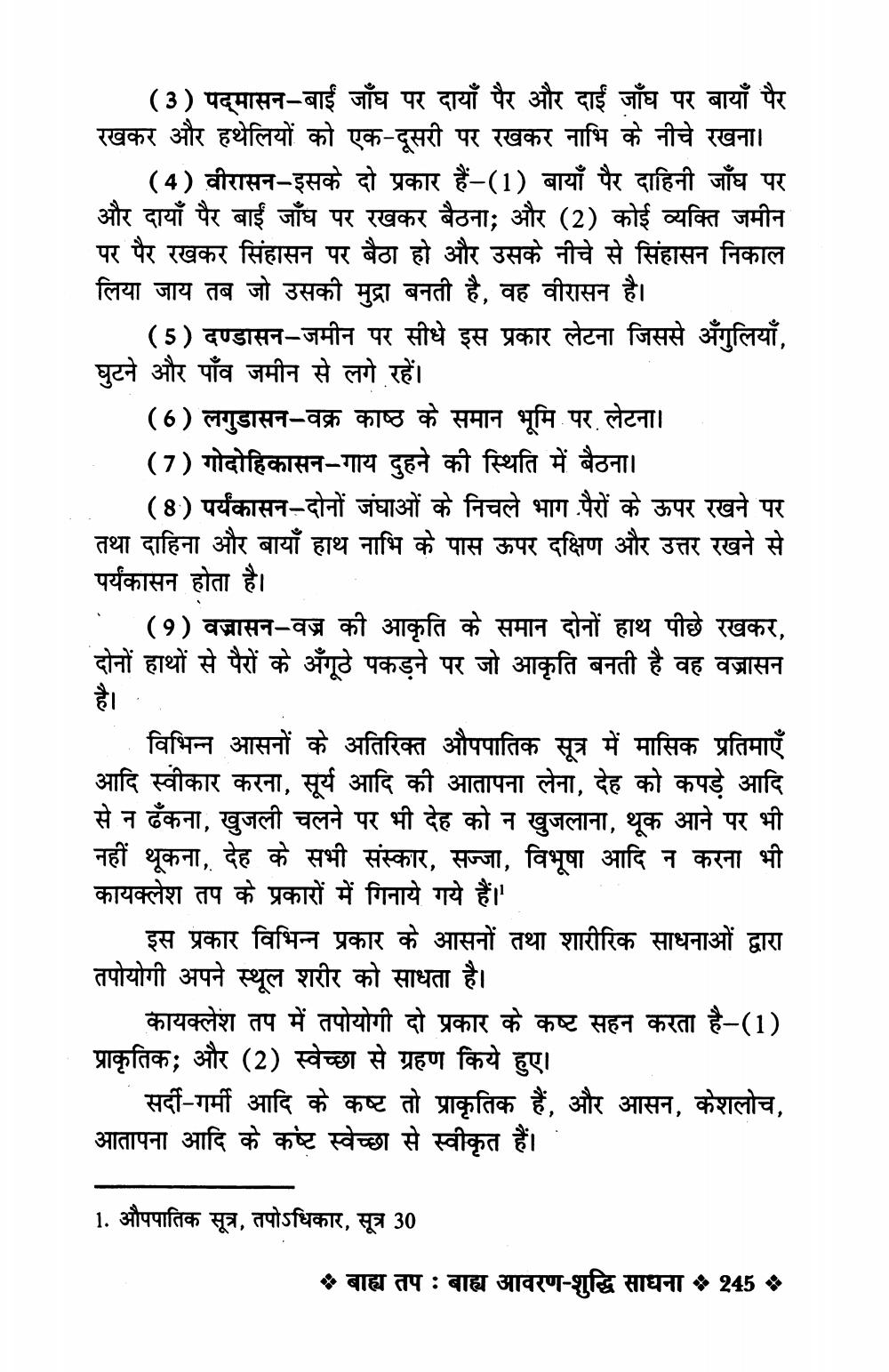________________
(3) पद्मासन-बाईं जाँघ पर दायाँ पैर और दाईं जाँघ पर बायाँ पैर रखकर और हथेलियों को एक-दूसरी पर रखकर नाभि के नीचे रखना।
(4) वीरासन-इसके दो प्रकार हैं-(1) बायाँ पैर दाहिनी जाँघ पर और दायाँ पैर बाईं जाँघ पर रखकर बैठना; और (2) कोई व्यक्ति जमीन पर पैर रखकर सिंहासन पर बैठा हो और उसके नीचे से सिंहासन निकाल लिया जाय तब जो उसकी मुद्रा बनती है, वह वीरासन है।
(5) दण्डासन-जमीन पर सीधे इस प्रकार लेटना जिससे अँगुलियाँ, घुटने और पाँव जमीन से लगे रहें।
(6) लगुडासन-वक्र काष्ठ के समान भूमि पर लेटना। (7) गोदोहिकासन-गाय दुहने की स्थिति में बैठना।
(8) पर्यंकासन-दोनों जंघाओं के निचले भाग पैरों के ऊपर रखने पर तथा दाहिना और बायाँ हाथ नाभि के पास ऊपर दक्षिण और उत्तर रखने से पर्यंकासन होता है। - (9) वज्रासन-वज्र की आकृति के समान दोनों हाथ पीछे रखकर, दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ने पर जो आकृति बनती है वह वज्रासन
विभिन्न आसनों के अतिरिक्त औपपातिक सूत्र में मासिक प्रतिमाएँ आदि स्वीकार करना, सूर्य आदि की आतापना लेना, देह को कपड़े आदि से न ढंकना, खुजली चलने पर भी देह को न खुजलाना, थूक आने पर भी नहीं थूकना, देह के सभी संस्कार, सज्जा, विभूषा आदि न करना भी कायक्लेश तप के प्रकारों में गिनाये गये हैं।' __इस प्रकार विभिन्न प्रकार के आसनों तथा शारीरिक साधनाओं द्वारा तपोयोगी अपने स्थूल शरीर को साधता है।
कायक्लेश तप में तपोयोगी दो प्रकार के कष्ट सहन करता है-(1) प्राकृतिक; और (2) स्वेच्छा से ग्रहण किये हुए।
सर्दी-गर्मी आदि के कष्ट तो प्राकृतिक हैं, और आसन, केशलोच, आतापना आदि के कष्ट स्वेच्छा से स्वीकृत हैं।
1. औपपातिक सूत्र, तपोऽधिकार, सूत्र 30
* बाह्य तप : बाह्य आवरण-शुद्धि साधना *245 *