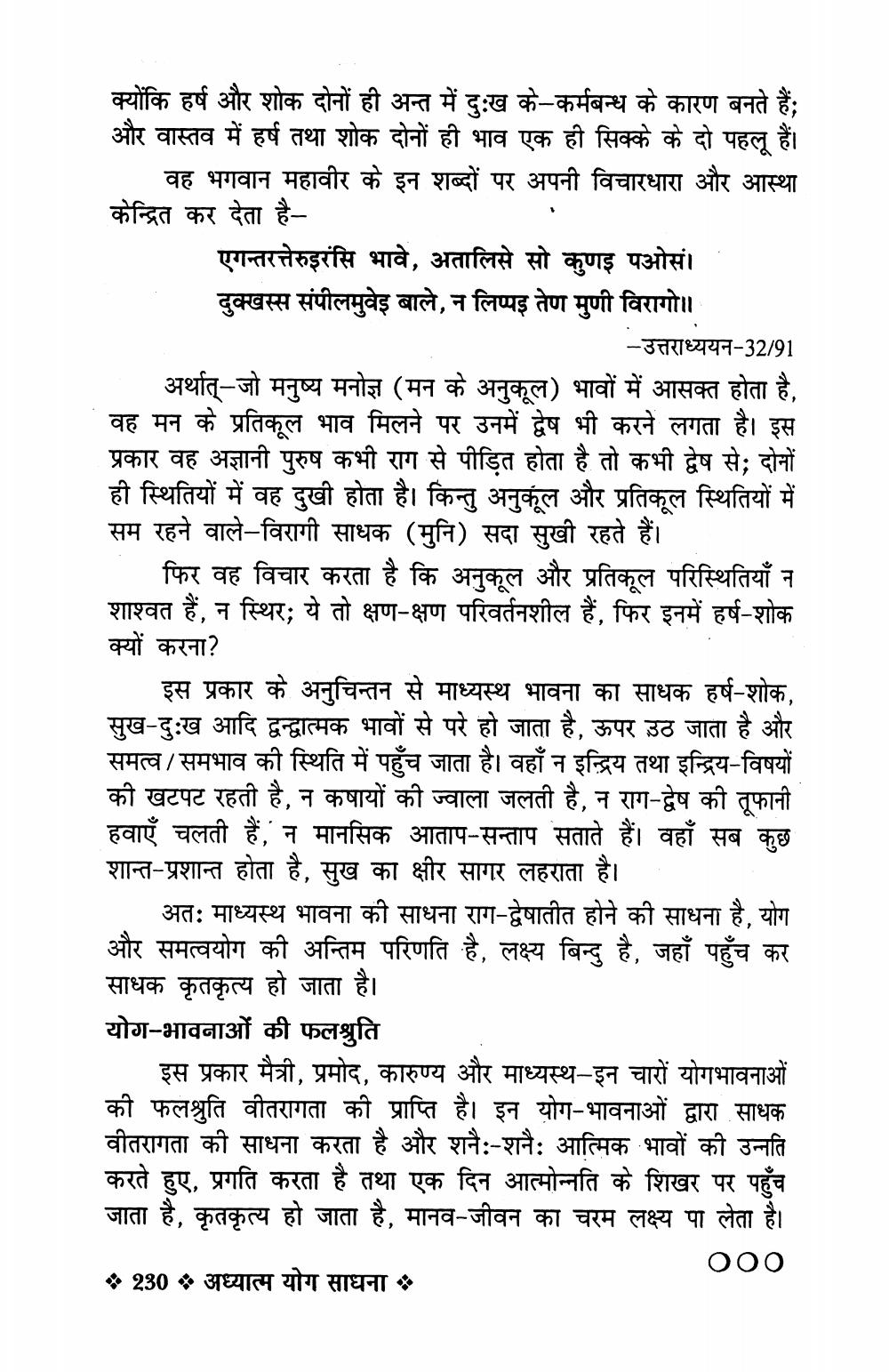________________
क्योंकि हर्ष और शोक दोनों ही अन्त में दुःख के - कर्मबन्ध के कारण बनते हैं; और वास्तव में हर्ष तथा शोक दोनों ही भाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वह भगवान महावीर के इन शब्दों पर अपनी विचारधारा और आस्था केन्द्रित कर देता है
एगन्तरत्तेरुइरंसि भावे, अतालिसे सो कुणइ पओसं । दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले, न लिप्पड़ तेण मुणी विरागो ॥
-उत्तराध्ययन-32/91
अर्थात्-जो मनुष्य मनोज्ञ ( मन के अनुकूल ) भावों में आसक्त होता है, वह मन के प्रतिकूल भाव मिलने पर उनमें द्वेष भी करने लगता है। इस प्रकार वह अज्ञानी पुरुष कभी राग से पीड़ित होता है तो कभी द्वेष से ; दोनों ही स्थितियों में वह दुखी होता है । किन्तु अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों में सम रहने वाले - विरागी साधक ( मुनि) सदा सुखी रहते हैं।
फिर वह विचार करता है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ न शाश्वत हैं, न स्थिर; ये तो क्षण-क्षण परिवर्तनशील हैं, फिर इनमें हर्ष - शोक क्यों करना ?
इस प्रकार के अनुचिन्तन से माध्यस्थ भावना का साधक हर्ष - शोक, सुख - दुःख आदि द्वन्द्वात्मक भावों से परे हो जाता है, ऊपर उठ जाता है और समत्व/समभाव की स्थिति में पहुँच जाता है। वहाँ न इन्द्रिय तथा इन्द्रिय-विषयों की खटपट रहती है, न कषायों की ज्वाला जलती है, न राग-द्वेष की तूफानी हवाएँ चलती हैं, न मानसिक आताप - सन्ताप सताते हैं। वहाँ सब कुछ शान्त - प्रशान्त होता है, सुख का क्षीर सागर लहराता है।
अतः माध्यस्थ भावना की साधना राग-द्वेषातीत होने की साधना है, योग और समत्वयोग की अन्तिम परिणति है, लक्ष्य बिन्दु है, जहाँ पहुँच कर साधक कृतकृत्य हो जाता है।
योग-भावनाओं की फलश्रुति
इस प्रकार मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ - इन चारों योगभावनाओं की फलश्रुति वीतरागता की प्राप्ति है। इन योग - भावनाओं द्वारा साधक वीतरागता की साधना करता है और शनैः-शनैः आत्मिक भावों की उन्नति करते हुए, प्रगति करता है तथा एक दिन आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, मानव-जीवन का चरम लक्ष्य पा लेता है ।
०००
230 अध्यात्म योग साधना