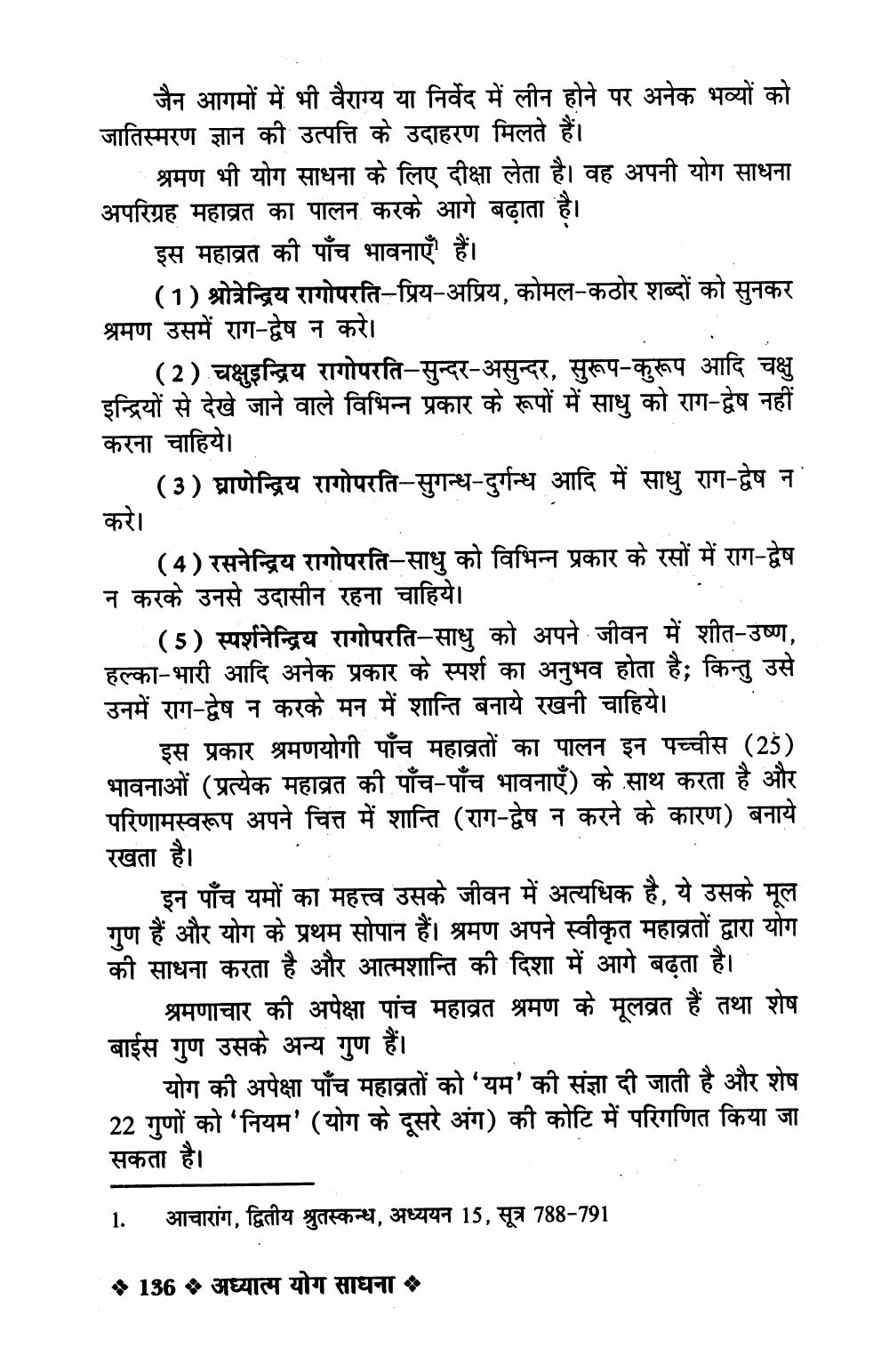________________
जैन आगमों में भी वैराग्य या निर्वेद में लीन होने पर अनेक भव्यों को जातिस्मरण ज्ञान की उत्पत्ति के उदाहरण मिलते हैं।
श्रमण भी योग साधना के लिए दीक्षा लेता है। वह अपनी योग साधना अपरिग्रह महाव्रत का पालन करके आगे बढ़ाता है।
इस महाव्रत की पाँच भावनाएँ हैं।
(1) श्रोत्रेन्द्रिय रागोपरति-प्रिय-अप्रिय, कोमल-कठोर शब्दों को सुनकर श्रमण उसमें राग-द्वेष न करे।
(2) चक्षुइन्द्रिय रागोपरति-सुन्दर-असुन्दर, सुरूप-कुरूप आदि चक्षु इन्द्रियों से देखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के रूपों में साधु को राग-द्वेष नहीं करना चाहिये। ___(3) घ्राणेन्द्रिय रागोपरति-सुगन्ध-दुर्गन्ध आदि में साधु राग-द्वेष न करे।
(4) रसनेन्द्रिय रागोपरति-साधु को विभिन्न प्रकार के रसों में राग-द्वेष न करके उनसे उदासीन रहना चाहिये।
(5) स्पर्शनेन्द्रिय रागोपरति-साधु को अपने जीवन में शीत-उष्ण, हल्का-भारी आदि अनेक प्रकार के स्पर्श का अनुभव होता है; किन्तु उसे उनमें राग-द्वेष न करके मन में शान्ति बनाये रखनी चाहिये।
इस प्रकार श्रमणयोगी पाँच महाव्रतों का पालन इन पच्चीस (25) भावनाओं (प्रत्येक महाव्रत की पाँच-पाँच भावनाएँ) के साथ करता है और परिणामस्वरूप अपने चित्त में शान्ति (राग-द्वेष न करने के कारण) बनाये रखता है।
इन पाँच यमों का महत्त्व उसके जीवन में अत्यधिक है, ये उसके मूल गुण हैं और योग के प्रथम सोपान हैं। श्रमण अपने स्वीकृत महाव्रतों द्वारा योग की साधना करता है और आत्मशान्ति की दिशा में आगे बढ़ता है।
श्रमणाचार की अपेक्षा पांच महाव्रत श्रमण के मूलव्रत हैं तथा शेष बाईस गुण उसके अन्य गुण हैं।
योग की अपेक्षा पाँच महाव्रतों को 'यम' की संज्ञा दी जाती है और शेष 22 गुणों को 'नियम' (योग के दूसरे अंग) की कोटि में परिगणित किया जा सकता है।
1.
आचारांग, द्वितीय श्रुतस्कन्ध, अध्ययन 15, सूत्र 788-791
* 136 * अध्यात्म योग साधना -