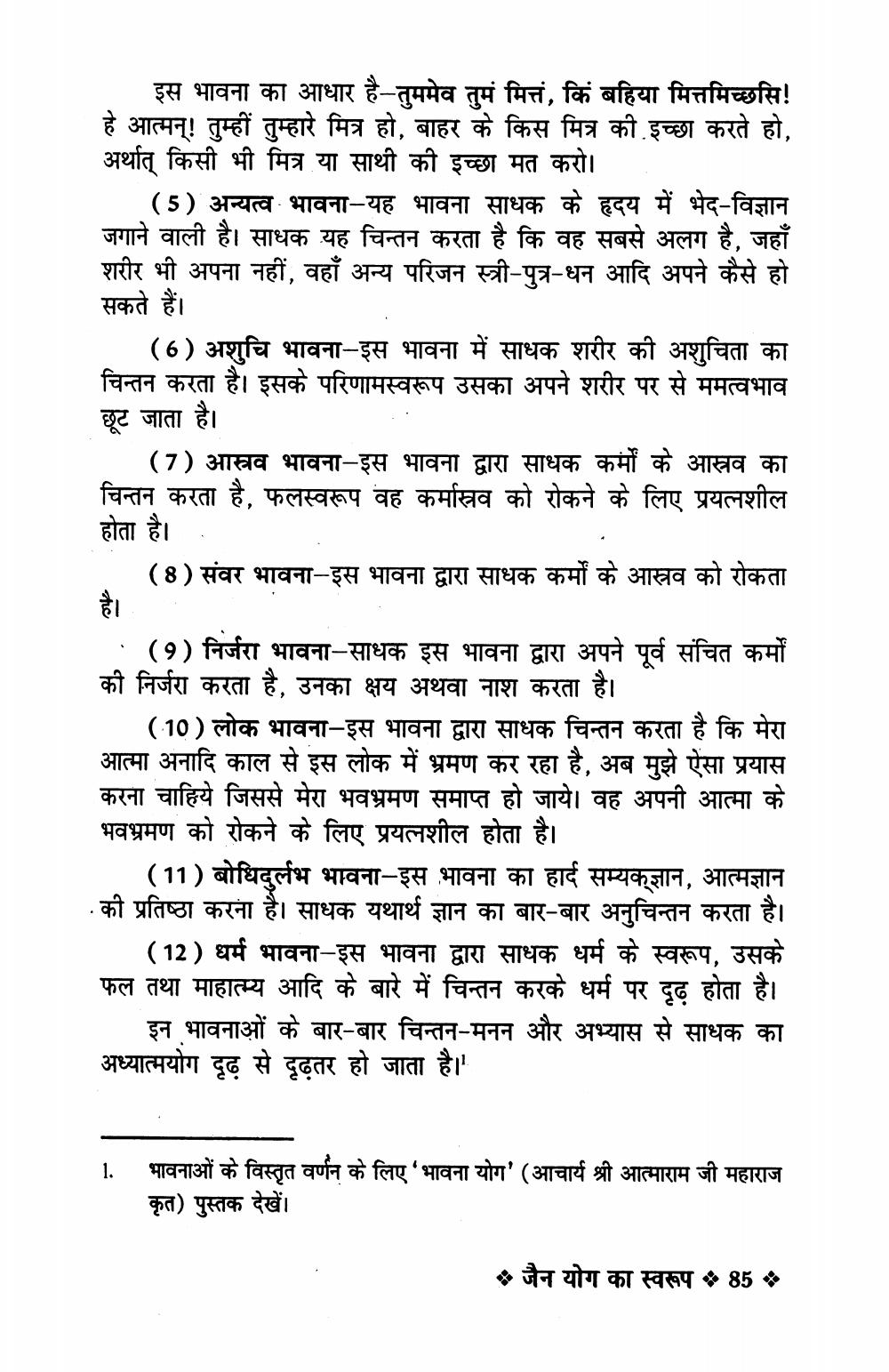________________
इस भावना का आधार है - तुममेव तुमं मित्तं, किं बहिया मित्तमिच्छसि ! हे आत्मन्! तुम्हीं तुम्हारे मित्र हो, बाहर के किस मित्र की इच्छा करते हो, अर्थात् किसी भी मित्र या साथी की इच्छा मत करो ।
(5) अन्यत्व भावना - यह भावना साधक के हृदय में भेद - विज्ञान जगाने वाली है। साधक यह चिन्तन करता है कि वह सबसे अलग है, जहाँ शरीर भी अपना नहीं, वहाँ अन्य परिजन स्त्री- पुत्र -धन आदि अपने कैसे हो सकते हैं।
(6) अशुचि भावना - इस भावना में साधक शरीर की अशुचिता का चिन्तन करता है। इसके परिणामस्वरूप उसका अपने शरीर पर से ममत्वभाव छूट जाता है।
(7) आस्रव भावना - इस भावना द्वारा साधक कर्मों के आस्रव का चिन्तन करता है, फलस्वरूप वह कर्मास्रव को रोकने के लिए प्रयत्नशील होता है।
( 8 ) संवर भावना - इस भावना द्वारा साधक कर्मों के आस्रव को रोकता
है।
(१) निर्जरा भावना-साधक इस भावना द्वारा अपने पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करता है, उनका क्षय अथवा नाश करता है।
(10) लोक भावना - इस भावना द्वारा साधक चिन्तन करता है कि मेरा आत्मा अनादि काल से इस लोक में भ्रमण कर रहा है, अब मुझे ऐसा प्रयास करना चाहिये जिससे मेरा भवभ्रमण समाप्त हो जाये। वह अपनी आत्मा के भवभ्रमण को रोकने के लिए प्रयत्नशील होता है।
( 11 ) बोधिदुर्लभ भावना - इस भावना का हार्द सम्यक्ज्ञान, आत्मज्ञान . की प्रतिष्ठा करना है। साधक यथार्थ ज्ञान का बार-बार अनुचिन्तन करता है । (12) धर्म भावना - इस भावना द्वारा साधक धर्म के स्वरूप, उसके फल तथा माहात्म्य आदि के बारे में चिन्तन करके धर्म पर दृढ़ होता है। इन भावनाओं के बार - बार चिन्तन-मनन और अभ्यास से साधक का अध्यात्मयोग दृढ़ से दृढ़तर हो जाता है ।'
1. भावनाओं के विस्तृत वर्णन के लिए 'भावना योग' (आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज कृत) पुस्तक देखें।
जैन योग का स्वरूप 85