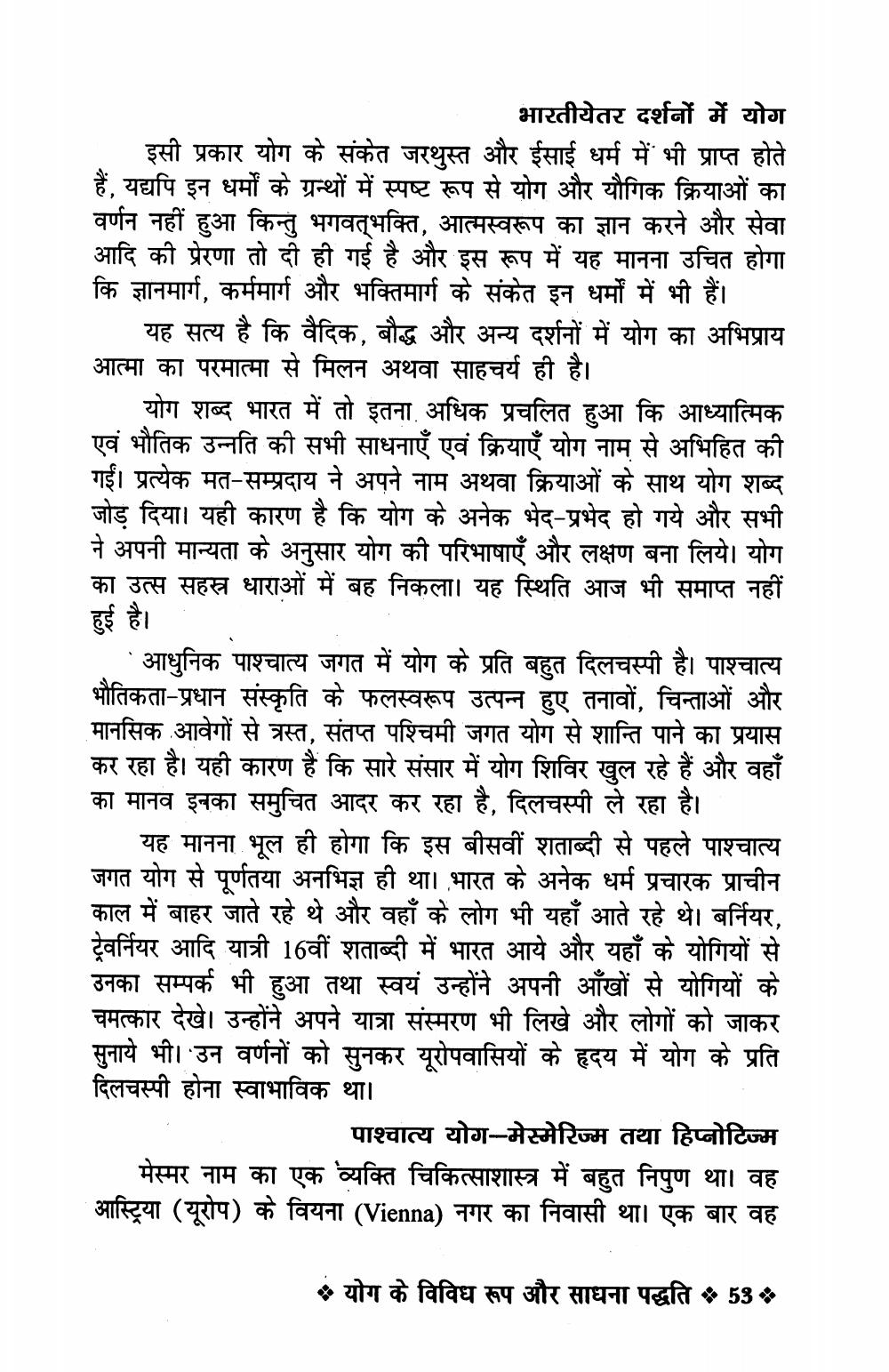________________
भारतीयेतर दर्शनों में योग ___ इसी प्रकार योग के संकेत जरथुस्त और ईसाई धर्म में भी प्राप्त होते हैं, यद्यपि इन धर्मों के ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से योग और यौगिक क्रियाओं का वर्णन नहीं हुआ किन्तु भगवत्भक्ति, आत्मस्वरूप का ज्ञान करने और सेवा आदि की प्रेरणा तो दी ही गई है और इस रूप में यह मानना उचित होगा कि ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग के संकेत इन धर्मों में भी हैं।
यह सत्य है कि वैदिक, बौद्ध और अन्य दर्शनों में योग का अभिप्राय आत्मा का परमात्मा से मिलन अथवा साहचर्य ही है।
योग शब्द भारत में तो इतना अधिक प्रचलित हुआ कि आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति की सभी साधनाएँ एवं क्रियाएँ योग नाम से अभिहित की गईं। प्रत्येक मत-सम्प्रदाय ने अपने नाम अथवा क्रियाओं के साथ योग शब्द जोड़ दिया। यही कारण है कि योग के अनेक भेद-प्रभेद हो गये और सभी ने अपनी मान्यता के अनुसार योग की परिभाषाएँ और लक्षण बना लिये। योग का उत्स सहस्र धाराओं में बह निकला। यह स्थिति आज भी समाप्त नहीं
• आधुनिक पाश्चात्य जगत में योग के प्रति बहुत दिलचस्पी है। पाश्चात्य भौतिकता-प्रधान संस्कृति के फलस्वरूप उत्पन्न हुए तनावों, चिन्ताओं और मानसिक आवेगों से त्रस्त, संतप्त पश्चिमी जगत योग से शान्ति पाने का प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि सारे संसार में योग शिविर खुल रहे हैं और वहाँ का मानव इनका समुचित आदर कर रहा है, दिलचस्पी ले रहा है।
यह मानना भूल ही होगा कि इस बीसवीं शताब्दी से पहले पाश्चात्य जगत योग से पूर्णतया अनभिज्ञ ही था। भारत के अनेक धर्म प्रचारक प्राचीन काल में बाहर जाते रहे थे और वहाँ के लोग भी यहाँ आते रहे थे। बर्नियर, ट्रेवर्नियर आदि यात्री 16वीं शताब्दी में भारत आये और यहाँ के योगियों से उनका सम्पर्क भी हुआ तथा स्वयं उन्होंने अपनी आँखों से योगियों के चमत्कार देखे। उन्होंने अपने यात्रा संस्मरण भी लिखे और लोगों को जाकर सुनाये भी। उन वर्णनों को सुनकर यूरोपवासियों के हृदय में योग के प्रति दिलचस्पी होना स्वाभाविक था।
पाश्चात्य योग-मेस्मेरिज्म तथा हिप्नोटिज्म मेस्मर नाम का एक व्यक्ति चिकित्साशास्त्र में बहुत निपुण था। वह आस्ट्रिया (यूरोप) के वियना (Vienna) नगर का निवासी था। एक बार वह
* योग के विविध रूप और साधना पद्धति - 53*