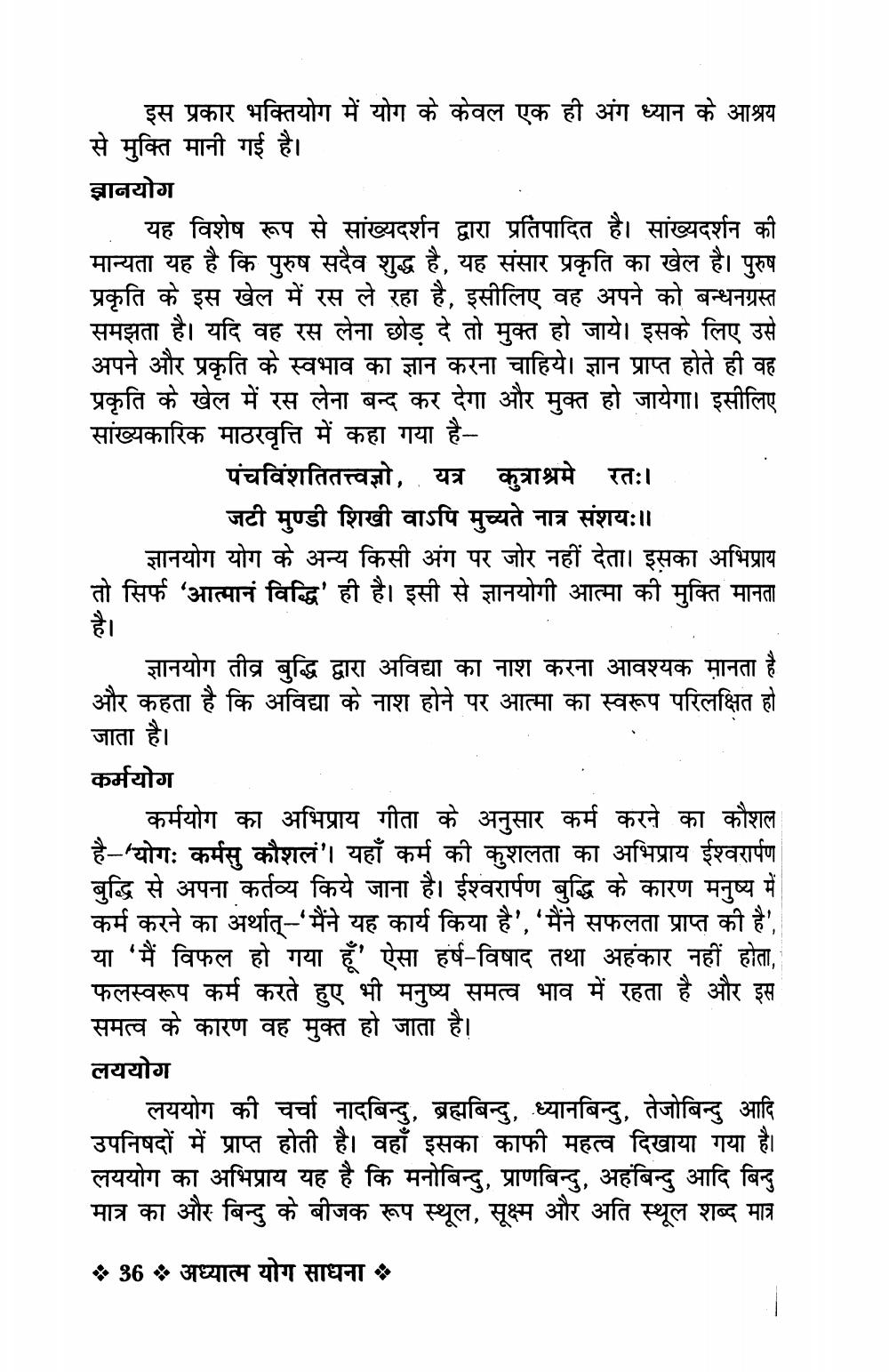________________
इस प्रकार भक्तियोग में योग के केवल एक ही अंग ध्यान के आश्रय से मुक्ति मानी गई है। ज्ञानयोग
यह विशेष रूप से सांख्यदर्शन द्वारा प्रतिपादित है। सांख्यदर्शन की मान्यता यह है कि पुरुष सदैव शुद्ध है, यह संसार प्रकृति का खेल है। पुरुष प्रकृति के इस खेल में रस ले रहा है, इसीलिए वह अपने को बन्धनग्रस्त समझता है। यदि वह रस लेना छोड़ दे तो मुक्त हो जाये। इसके लिए उसे अपने और प्रकृति के स्वभाव का ज्ञान करना चाहिये। ज्ञान प्राप्त होते ही वह प्रकृति के खेल में रस लेना बन्द कर देगा और मुक्त हो जायेगा। इसीलिए सांख्यकारिक माठरवृत्ति में कहा गया है
पंचविंशतितत्त्वज्ञो, यत्र कुत्राश्रमे रतः।
जटी मुण्डी शिखी वाऽपि मुच्यते नात्र संशयः॥ ज्ञानयोग योग के अन्य किसी अंग पर जोर नहीं देता। इसका अभिप्राय तो सिर्फ 'आत्मानं विद्धि' ही है। इसी से ज्ञानयोगी आत्मा की मुक्ति मानता
ज्ञानयोग तीव्र बुद्धि द्वारा अविद्या का नाश करना आवश्यक मानता है और कहता है कि अविद्या के नाश होने पर आत्मा का स्वरूप परिलक्षित हो जाता है। कर्मयोग
कर्मयोग का अभिप्राय गीता के अनुसार कर्म करने का कौशल है-'योगः कर्मस कौशलं'। यहाँ कर्म की कुशलता का अभिप्राय ईश्वरार्पण बुद्धि से अपना कर्तव्य किये जाना है। ईश्वरार्पण बुद्धि के कारण मनुष्य में कर्म करने का अर्थात्-'मैंने यह कार्य किया है', 'मैंने सफलता प्राप्त की है', या 'मैं विफल हो गया हूँ' ऐसा हर्ष-विषाद तथा अहंकार नहीं होता, फलस्वरूप कर्म करते हुए भी मनुष्य समत्व भाव में रहता है और इस समत्व के कारण वह मुक्त हो जाता है। लययोग
लययोग की चर्चा नादबिन्दु, ब्रह्मबिन्दु, ध्यानबिन्दु, तेजोबिन्दु आदि उपनिषदों में प्राप्त होती है। वहाँ इसका काफी महत्व दिखाया गया है। लययोग का अभिप्राय यह है कि मनोबिन्दु, प्राणबिन्दु, अहंबिन्दु आदि बिन्दु मात्र का और बिन्दु के बीजक रूप स्थूल, सूक्ष्म और अति स्थूल शब्द मात्र * 36 * अध्यात्म योग साधना *