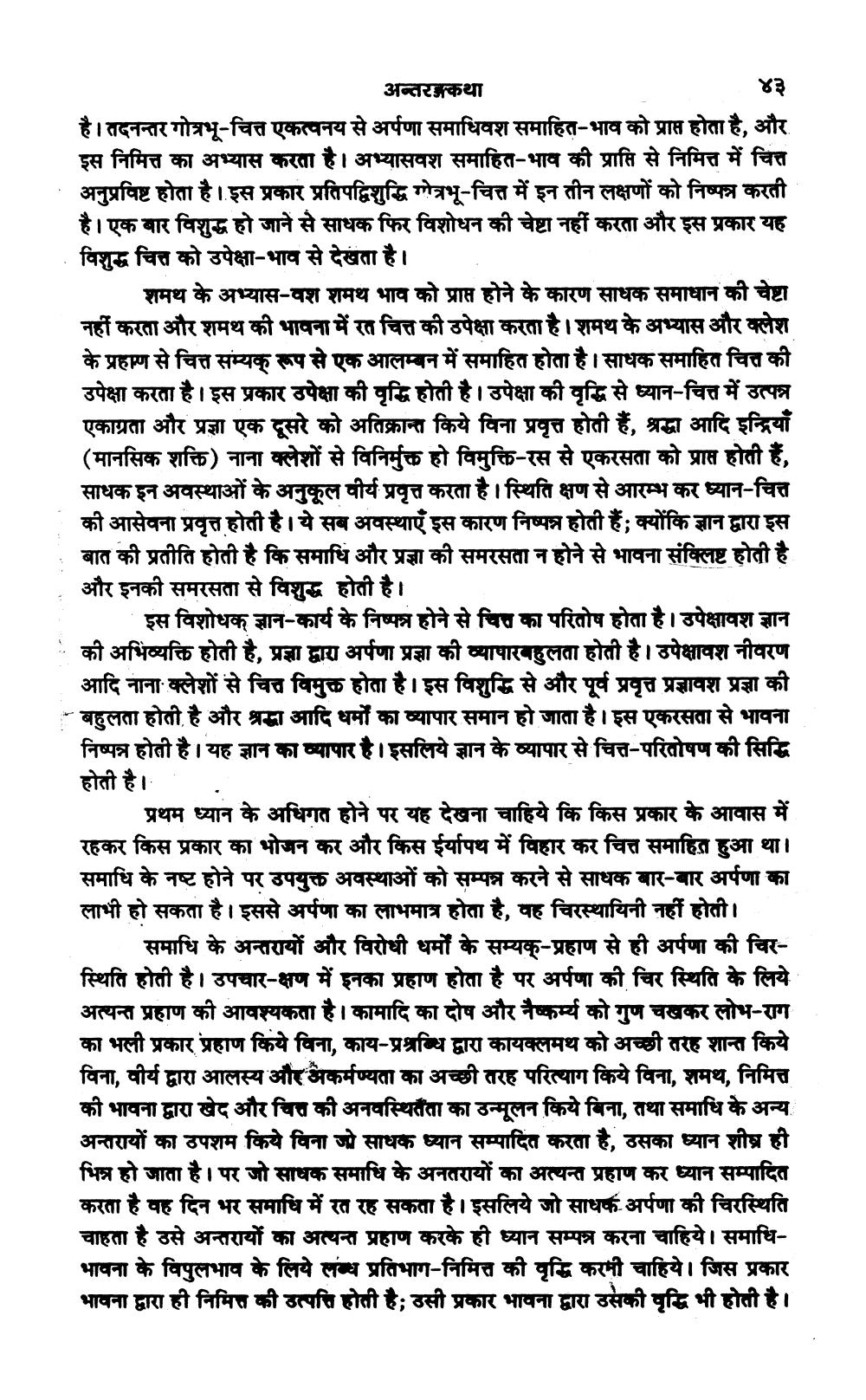________________
अन्तरङ्गकथा
४३ है। तदनन्तर गोत्रभू-चित्त एकत्वनय से अर्पणा समाधिवश समाहित-भाव को प्राप्त होता है, और इस निमित्त का अभ्यास करता है। अभ्यासवश समाहित-भाव की प्राति से निमित्त में चित्त अनुप्रविष्ट होता है। इस प्रकार प्रतिपद्विशुद्धि गोत्रभू-चित्त में इन तीन लक्षणों को निष्पन्न करती है। एक बार विशुद्ध हो जाने से साधक फिर विशोधन की चेष्टा नहीं करता और इस प्रकार यह विशुद्ध चित्त को उपेक्षा-भाव से देखता है।
शमथ के अभ्यास-वश शमथ भाव को प्राप्त होने के कारण साधक समाधान की चेष्टा नहीं करता और शमथ की भावना में रत चित्त की उपेक्षा करता है। शमथ के अभ्यास और क्लेश के प्रहाण से चित्त सम्यक् रूप से एक आलम्बन में समाहित होता है। साधक समाहित चित्त की उपेक्षा करता है। इस प्रकार उपेक्षा की वृद्धि होती है। उपेक्षा की वृद्धि से ध्यान-चित्त में उत्पन्न एकाग्रता और प्रज्ञा एक दूसरे को अतिक्रान्त किये विना प्रवृत्त होती हैं, श्रद्धा आदि इन्द्रियाँ (मानसिक शक्ति) नाना क्लेशों से विनिर्मुक्त हो विमुक्ति-रस से एकरसता को प्राप्त होती हैं, साधक इन अवस्थाओं के अनुकूल वीर्य प्रवृत्त करता है। स्थिति क्षण से आरम्भ कर ध्यान-चित्त की आसेवना प्रवृत्त होती है। ये सब अवस्थाएं इस कारण निष्पन्न होती हैं, क्योंकि ज्ञान द्वारा इस बात की प्रतीति होती है कि समाधि और प्रज्ञा की समरसता न होने से भावना संक्लिष्ट होती है और इनकी समरसता से विशुद्ध होती है।।
इस विशोधक ज्ञान-कार्य के निष्पन्न होने से चित्त का परितोष होता है। उपेक्षावश ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, प्रज्ञा द्वारा अर्पणा प्रज्ञा की व्यापारबहुलता होती है। उपेक्षावश नीवरण आदि नाना क्लेशों से चित्त विमुक्त होता है। इस विशुद्धि से और पूर्व प्रवृत्त प्रज्ञावश प्रज्ञा की बहुलता होती है और श्रद्धा आदिधर्मों का व्यापार समान हो जाता है। इस एकरसता से भावना निष्पन्न होती है। यह ज्ञान का व्यापार है। इसलिये ज्ञान के व्यापार से चित्त-परितोषण की सिद्धि होती है।
प्रथम ध्यान के अधिगत होने पर यह देखना चाहिये कि किस प्रकार के आवास में रहकर किस प्रकार का भोजन कर और किस ईर्यापथ में विहार कर चित्त समाहित हुआ था। समाधि के नष्ट होने पर उपयुक्त अवस्थाओं को सम्पन्न करने से साधक बार-बार अर्पणा का लाभी हो सकता है। इससे अर्पणा का लाभमात्र होता है, वह चिरस्थायिनी नहीं होती।
समाधि के अन्तरायों और विरोधी धर्मों के सम्यक्-प्रहाण से ही अर्पणा की चिरस्थिति होती है। उपचार-क्षण में इनका प्रहाण होता है पर अर्पणा की चिर स्थिति के लिये अत्यन्त प्रहाण की आवश्यकता है। कामादि का दोष और नैष्कर्म्य को गुण चखकर लोभ-राग का भली प्रकार प्रहाण किये विना, काय-प्रश्रब्धि द्वारा कायक्लमथ को अच्छी तरह शान्त किये विना, वीर्य द्वारा आलस्य और अकर्मण्यता का अच्छी तरह परित्याग किये विना, शमथ, निमित्त की भावना द्वारा खेद और चित की अनवस्थितता का उन्मूलन किये बिना, तथा समाधि के अन्य अन्तरायों का उपशम किये विना जो साधक ध्यान सम्पादित करता है, उसका ध्यान शीघ्र ही भिन्न हो जाता है। पर जो साधक समाधि के अनतरायों का अत्यन्त प्रहाण कर ध्यान सम्पादित करता है वह दिन भर समाधि में रत रह सकता है। इसलिये जो साधक अर्पणा की चिरस्थिति चाहता है उसे अन्तरायों का अत्यन्त प्रहाण करके ही ध्यान सम्पन्न करना चाहिये। समाधिभावना के विपुलभाव के लिये लब्ध प्रतिभाग-निमित्त की वृद्धि करनी चाहिये। जिस प्रकार भावना द्वारा ही निमित्त की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार भावना द्वारा उसकी वृद्धि भी होती है।