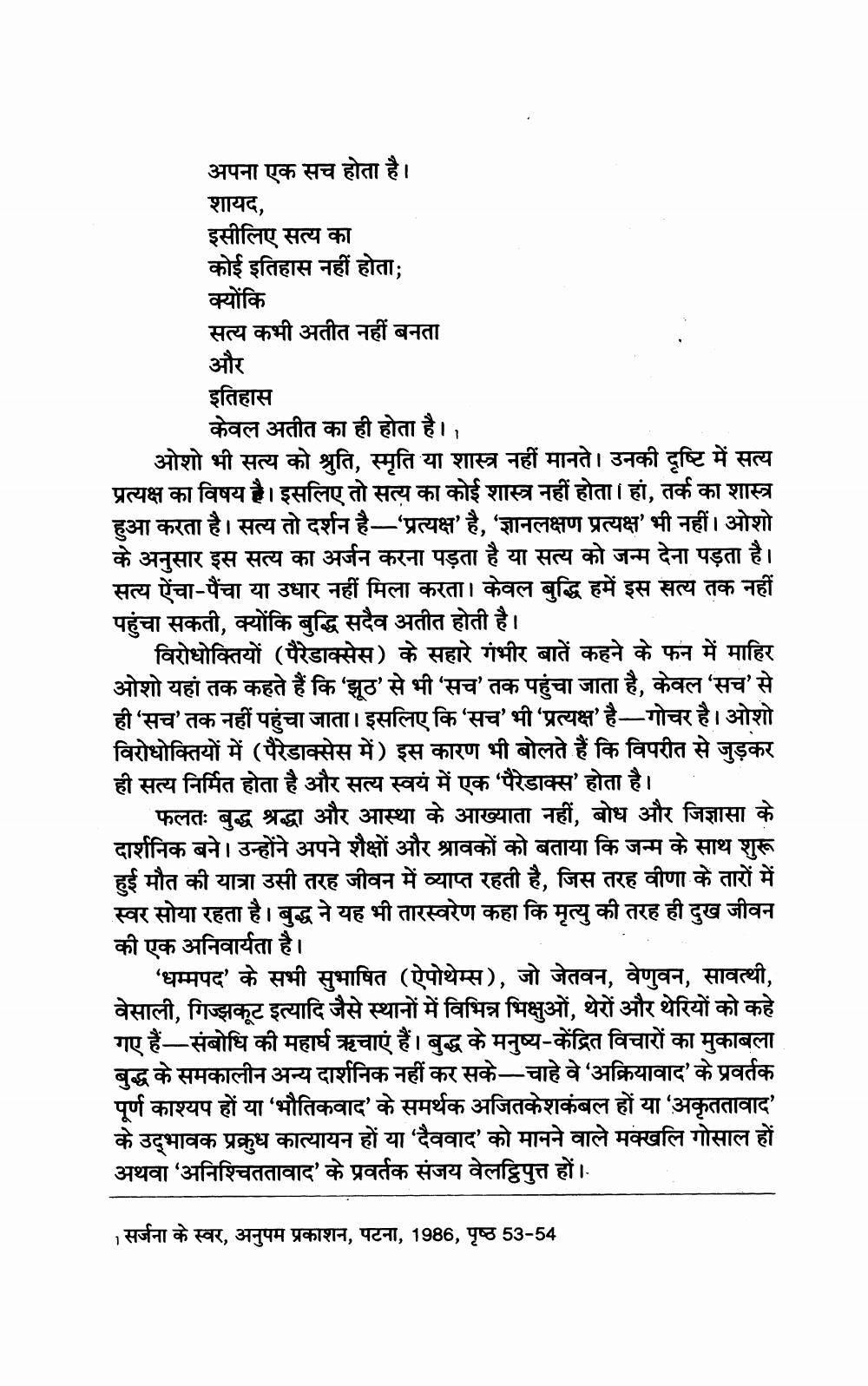________________
अपना एक सच होता है। शायद, इसीलिए सत्य का कोई इतिहास नहीं होता; क्योंकि सत्य कभी अतीत नहीं बनता और इतिहास
केवल अतीत का ही होता है।। ओशो भी सत्य को श्रुति, स्मृति या शास्त्र नहीं मानते। उनकी दृष्टि में सत्य प्रत्यक्ष का विषय है। इसलिए तो सत्य का कोई शास्त्र नहीं होता। हां, तर्क का शास्त्र हुआ करता है। सत्य तो दर्शन है-'प्रत्यक्ष' है, 'ज्ञानलक्षण प्रत्यक्ष' भी नहीं। ओशो के अनुसार इस सत्य का अर्जन करना पड़ता है या सत्य को जन्म देना पड़ता है। सत्य ऐंचा-पैंचा या उधार नहीं मिला करता। केवल बुद्धि हमें इस सत्य तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि बुद्धि सदैव अतीत होती है।
विरोधोक्तियों (पैरेडाक्सेस) के सहारे गंभीर बातें कहने के फन में माहिर ओशो यहां तक कहते हैं कि 'झूठ' से भी 'सच' तक पहुंचा जाता है, केवल 'सच' से ही 'सच' तक नहीं पहुंचा जाता। इसलिए कि 'सच' भी प्रत्यक्ष' है-गोचर है। ओशो विरोधोक्तियों में (पैरेडाक्सेस में) इस कारण भी बोलते हैं कि विपरीत से जुड़कर ही सत्य निर्मित होता है और सत्य स्वयं में एक पैरेडाक्स' होता है। ___ फलतः बुद्ध श्रद्धा और आस्था के आख्याता नहीं, बोध और जिज्ञासा के दार्शनिक बने। उन्होंने अपने शैक्षों और श्रावकों को बताया कि जन्म के साथ शुरू हुई मौत की यात्रा उसी तरह जीवन में व्याप्त रहती है, जिस तरह वीणा के तारों में स्वर सोया रहता है। बुद्ध ने यह भी तारस्वरेण कहा कि मृत्यु की तरह ही दुख जीवन की एक अनिवार्यता है।
_ 'धम्मपद' के सभी सुभाषित (ऐपोथेम्स), जो जेतवन, वेणुवन, सावत्थी, वेसाली, गिज्झकूट इत्यादि जैसे स्थानों में विभिन्न भिक्षुओं, थेरों और थेरियों को कहे गए हैं-संबोधि की महार्घ ऋचाएं हैं। बुद्ध के मनुष्य-केंद्रित विचारों का मुकाबला बुद्ध के समकालीन अन्य दार्शनिक नहीं कर सके-चाहे वे 'अक्रियावाद' के प्रवर्तक पूर्ण काश्यप हों या 'भौतिकवाद' के समर्थक अजितकेशकंबल हों या 'अकृततावाद' के उद्भावक प्रक्रुध कात्यायन हों या 'दैववाद' को मानने वाले मक्खलि गोसाल हों अथवा 'अनिश्चिततावाद' के प्रवर्तक संजय वेलट्ठिपुत्त हों।।
सर्जना के स्वर, अनुपम प्रकाशन, पटना, 1986, पृष्ठ 53-54