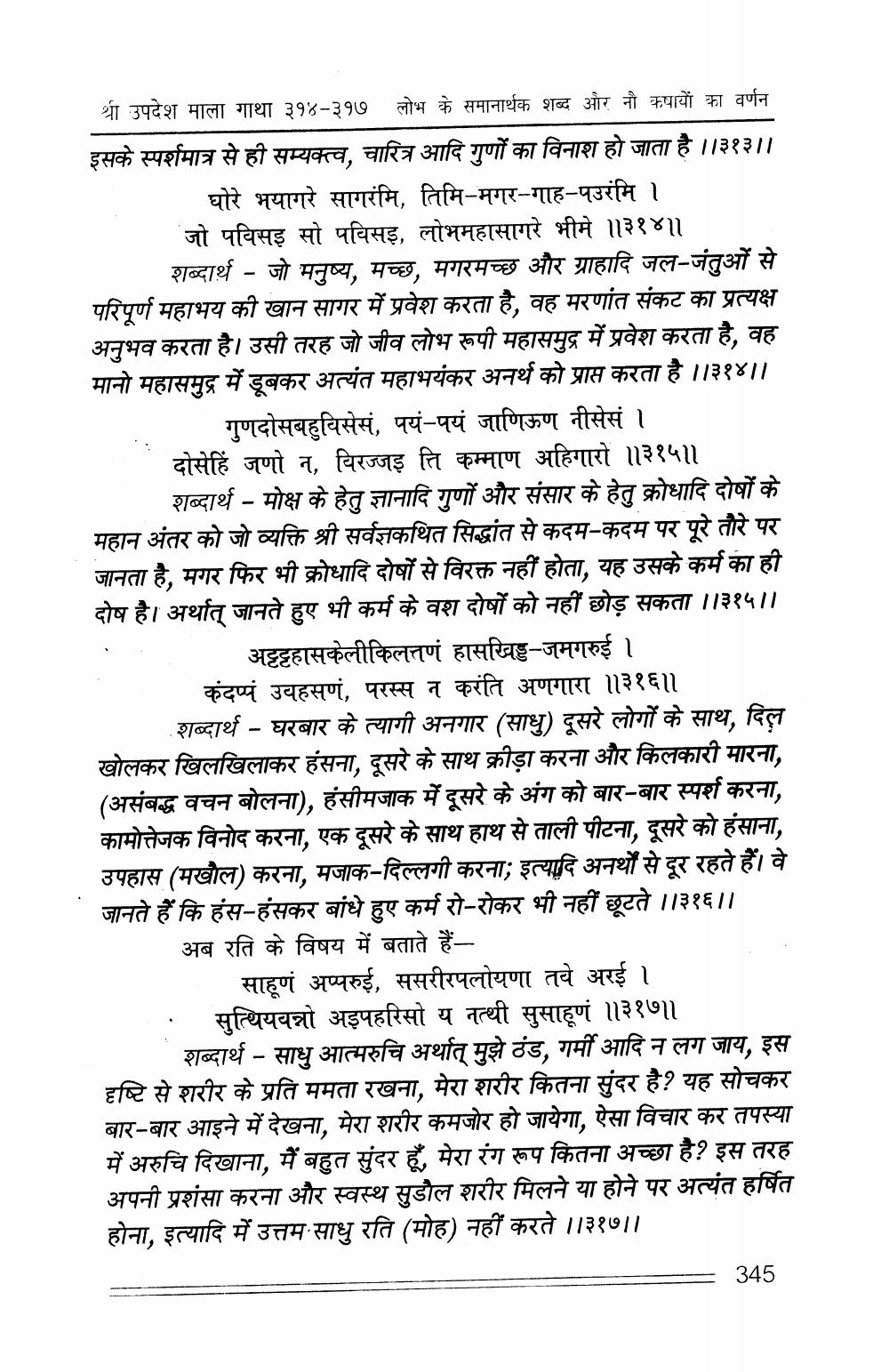________________
थी उपदेश माला गाथा ३१४-३१७ लोभ के समानार्थक शब्द और नौ कषायों का वर्णन इसके स्पर्शमात्र से ही सम्यक्त्व, चारित्र आदि गुणों का विनाश हो जाता है ।।३१३।।
घोरे भयागरे सागरंमि, तिमि-मगर-गाह-पउरंमि । जो पविसइ सो पविसइ, लोभमहासागरे भीमे ॥३१४॥
शब्दार्थ - जो मनुष्य, मच्छ, मगरमच्छ और ग्राहादि जल-जंतुओं से परिपूर्ण महाभय की खान सागर में प्रवेश करता है, वह मरणांत संकट का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। उसी तरह जो जीव लोभ रूपी महासमुद्र में प्रवेश करता है, वह मानो महासमुद्र में डूबकर अत्यंत महाभयंकर अनर्थ को प्रास करता है ।।३१४।। . गुणदोसबहुविसेस, पयं-पयं जाणिऊण नीसेसं ।
दोसेहिं जणो न, विरज्जइ त्ति कम्माण अहिगारो ॥३१५॥
शब्दार्थ - मोक्ष के हेतु ज्ञानादि गुणों और संसार के हेतु क्रोधादि दोषों के महान अंतर को जो व्यक्ति श्री सर्वज्ञकथित सिद्धांत से कदम-कदम पर पूरे तौरे पर जानता है, मगर फिर भी क्रोधादि दोषों से विरक्त नहीं होता, यह उसके कर्म का ही दोष है। अर्थात् जानते हुए भी कर्म के वश दोषों को नहीं छोड़ सकता ।।३१५।।
__ अट्टहासकेलीकिलतणं हासखिड्ड-जमगरुई । कंदप्पं उवहसणं, परस्स् न करंति अणगारा ॥३१६॥
शब्दार्थ - घरबार के त्यागी अनगार (साधु) दूसरे लोगों के साथ, दिल खोलकर खिलखिलाकर हंसना, दूसरे के साथ क्रीड़ा करना और किलकारी मारना, (असंबद्ध वचन बोलना), हंसीमजाक में दूसरे के अंग को बार-बार स्पर्श करना, कामोत्तेजक विनोद करना, एक दूसरे के साथ हाथ से ताली पीटना, दूसरे को हंसाना, उपहास (मखौल) करना, मजाक-दिल्लगी करना; इत्यादि अनर्थों से दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि हंस-हंसकर बांधे हुए कर्म रो-रोकर भी नहीं छूटते ।।३१६ ।।
अब रति के विषय में बताते हैं
साहूणं अप्परुई, ससरीरपलोयणा तवे अरई ।
सुत्थियवन्नो अइपहरिसो य नत्थी सुसाहूणं ॥३१७॥ __ शब्दार्थ - साधु आत्मरुचि अर्थात् मुझे ठंड, गर्मी आदि न लग जाय, इस दृष्टि से शरीर के प्रति ममता रखना, मेरा शरीर कितना सुंदर है? यह सोचकर बार-बार आइने में देखना, मेरा शरीर कमजोर हो जायेगा, ऐसा विचार कर तपस्या में अरुचि दिखाना, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा रंग रूप कितना अच्छा है? इस तरह अपनी प्रशंसा करना और स्वस्थ सुडौल शरीर मिलने या होने पर अत्यंत हर्षित होना, इत्यादि में उत्तम साधु रति (मोह) नहीं करते ।।३१७।।
- 345