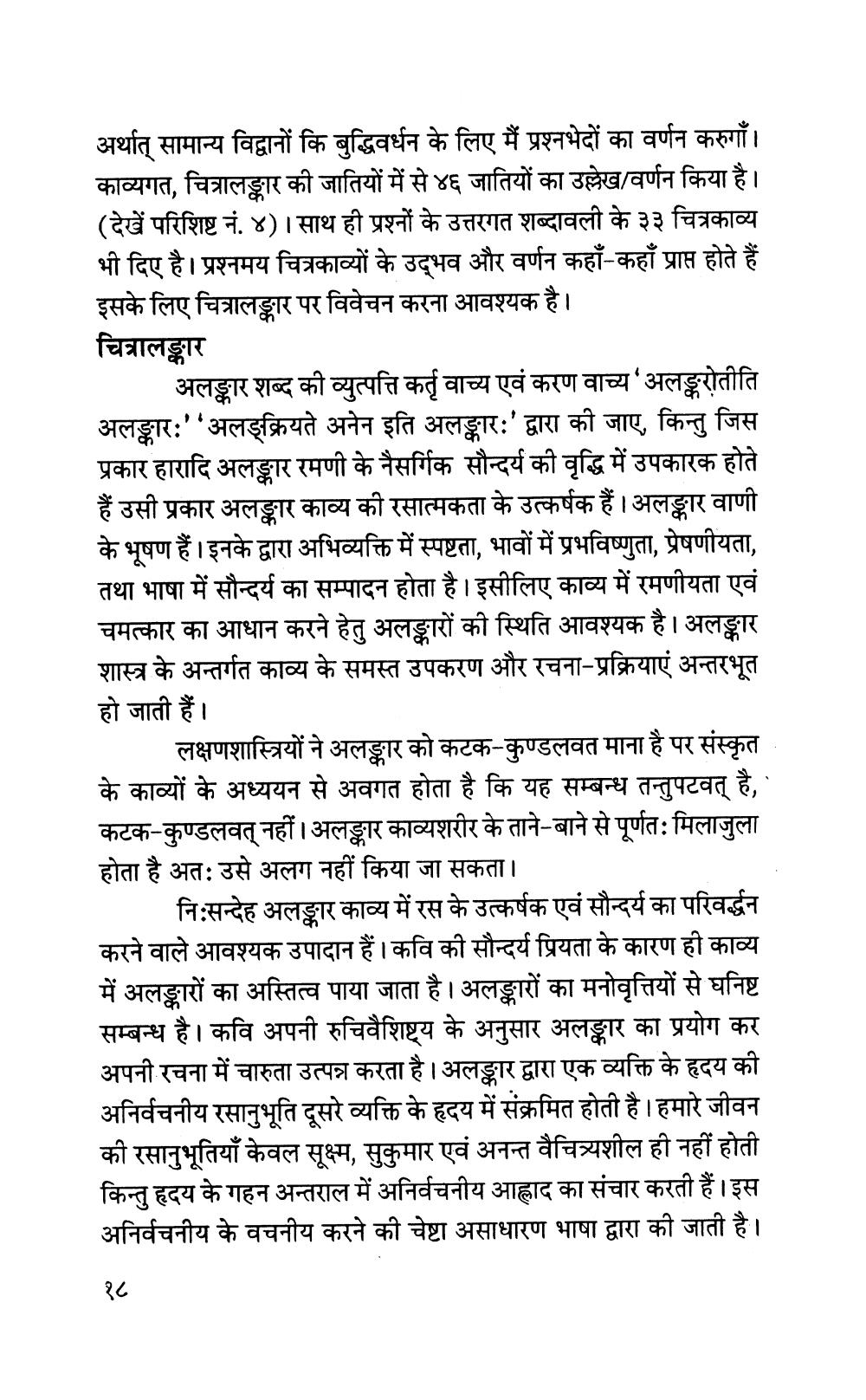________________
अर्थात् सामान्य विद्वानों कि बुद्धिवर्धन के लिए मैं प्रश्नभेदों का वर्णन करुगाँ। काव्यगत, चित्रालङ्कार की जातियों में से ४६ जातियों का उल्लेख/वर्णन किया है। (देखें परिशिष्ट नं. ४)। साथ ही प्रश्नों के उत्तरगत शब्दावली के ३३ चित्रकाव्य भी दिए है। प्रश्नमय चित्रकाव्यों के उद्भव और वर्णन कहाँ-कहाँ प्राप्त होते हैं इसके लिए चित्रालङ्कार पर विवेचन करना आवश्यक है। चित्रालङ्कार
अलङ्कार शब्द की व्युत्पत्ति कर्तृ वाच्य एवं करण वाच्य अलङ्करोतीति अलङ्कारः' 'अलङ्क्रियते अनेन इति अलङ्कारः' द्वारा की जाए, किन्तु जिस प्रकार हारादि अलङ्कार रमणी के नैसर्गिक सौन्दर्य की वृद्धि में उपकारक होते हैं उसी प्रकार अलङ्कार काव्य की रसात्मकता के उत्कर्षक हैं। अलङ्कार वाणी के भूषण हैं । इनके द्वारा अभिव्यक्ति में स्पष्टता, भावों में प्रभविष्णुता, प्रेषणीयता, तथा भाषा में सौन्दर्य का सम्पादन होता है। इसीलिए काव्य में रमणीयता एवं चमत्कार का आधान करने हेतु अलङ्कारों की स्थिति आवश्यक है। अलङ्कार शास्त्र के अन्तर्गत काव्य के समस्त उपकरण और रचना-प्रक्रियाएं अन्तरभूत हो जाती हैं।
लक्षणशास्त्रियों ने अलङ्कार को कटक-कुण्डलवत माना है पर संस्कृत के काव्यों के अध्ययन से अवगत होता है कि यह सम्बन्ध तन्तुपटवत् है, कटक-कुण्डलवत् नहीं। अलङ्कार काव्यशरीर के ताने-बाने से पूर्णतः मिलाजुला होता है अत: उसे अलग नहीं किया जा सकता।
निःसन्देह अलङ्कार काव्य में रस के उत्कर्षक एवं सौन्दर्य का परिवर्द्धन करने वाले आवश्यक उपादान हैं। कवि की सौन्दर्य प्रियता के कारण ही काव्य में अलङ्कारों का अस्तित्व पाया जाता है। अलङ्कारों का मनोवृत्तियों से घनिष्ट सम्बन्ध है। कवि अपनी रुचिवैशिष्ट्य के अनुसार अलङ्कार का प्रयोग कर अपनी रचना में चारुता उत्पन्न करता है। अलङ्कार द्वारा एक व्यक्ति के हृदय की अनिर्वचनीय रसानुभूति दूसरे व्यक्ति के हृदय में संक्रमित होती है। हमारे जीवन की रसानुभूतियाँ केवल सूक्ष्म, सुकुमार एवं अनन्त वैचित्र्यशील ही नहीं होती किन्तु हृदय के गहन अन्तराल में अनिर्वचनीय आह्लाद का संचार करती हैं। इस अनिर्वचनीय के वचनीय करने की चेष्टा असाधारण भाषा द्वारा की जाती है।