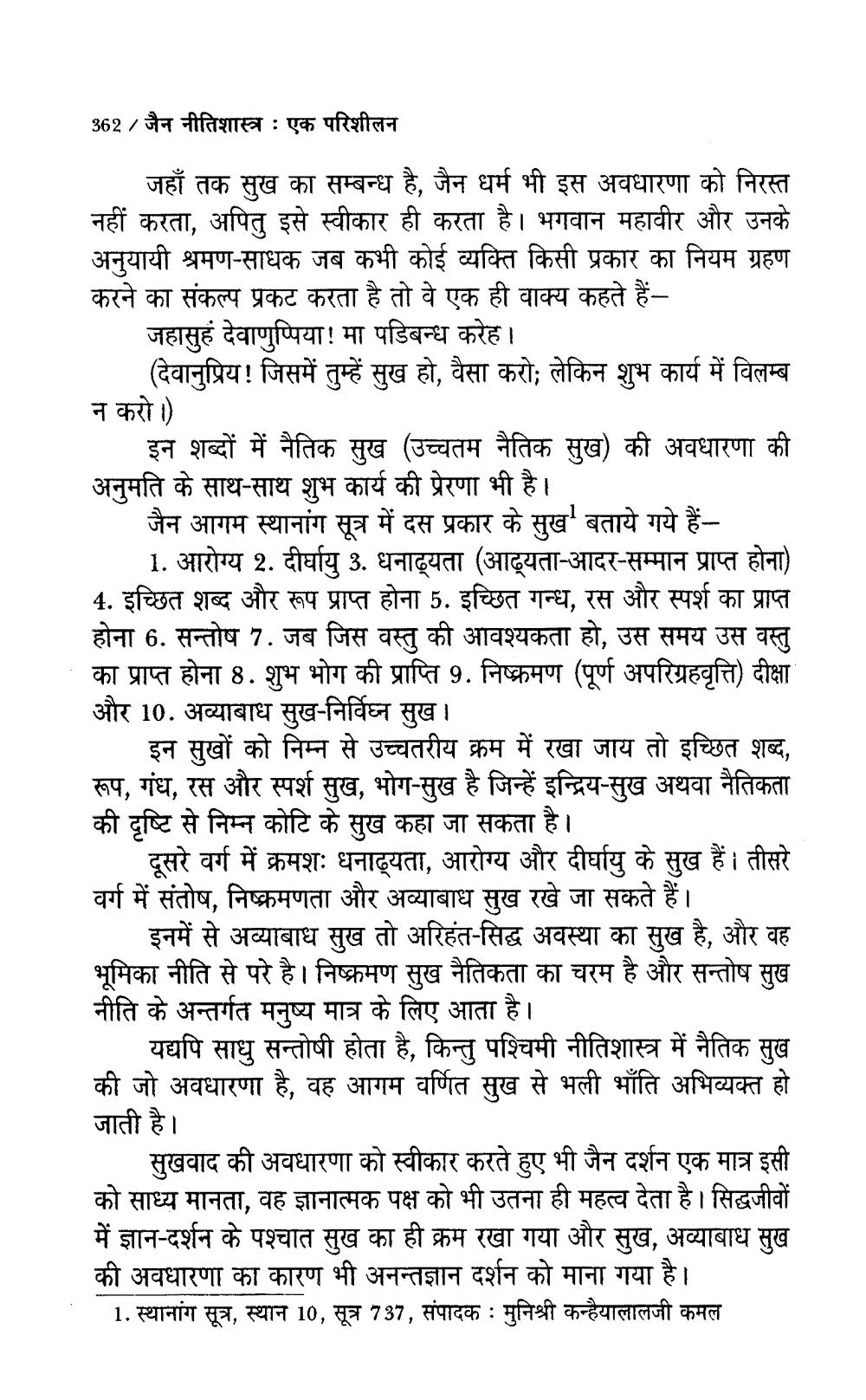________________
362 / जैन नीतिशास्त्र : एक परिशीलन
जहाँ तक सुख का सम्बन्ध है, जैन धर्म भी इस अवधारणा को निरस्त नहीं करता, अपितु इसे स्वीकार ही करता है। भगवान महावीर और उनके अनुयायी श्रमण-साधक जब कभी कोई व्यक्ति किसी प्रकार का नियम ग्रहण करने का संकल्प प्रकट करता है तो वे एक ही वाक्य कहते हैं
जहासुहं देवाणुप्पिया! मा पडिबन्ध करेह।
(देवानुप्रिय! जिसमें तुम्हें सुख हो, वैसा करो; लेकिन शुभ कार्य में विलम्ब न करो।)
इन शब्दों में नैतिक सुख (उच्चतम नैतिक सुख) की अवधारणा की अनुमति के साथ-साथ शुभ कार्य की प्रेरणा भी है। __ जैन आगम स्थानांग सूत्र में दस प्रकार के सुख बताये गये हैं__1. आरोग्य 2. दीर्घायु 3. धनाढ्यता (आढ्यता-आदर-सम्मान प्राप्त होना) 4. इच्छित शब्द और रूप प्राप्त होना 5. इच्छित गन्ध, रस और स्पर्श का प्राप्त होना 6. सन्तोष 7. जब जिस वस्तु की आवश्यकता हो, उस समय उस वस्तु का प्राप्त होना 8. शुभ भोग की प्राप्ति 9. निष्क्रमण (पूर्ण अपरिग्रहवृत्ति) दीक्षा और 10. अव्याबाध सुख-निर्विघ्न सुख।।
इन सुखों को निम्न से उच्चतरीय क्रम में रखा जाय तो इच्छित शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श सुख, भोग-सुख है जिन्हें इन्द्रिय-सुख अथवा नैतिकता की दृष्टि से निम्न कोटि के सुख कहा जा सकता है।
दूसरे वर्ग में क्रमशः धनाढ्यता, आरोग्य और दीर्घायु के सुख हैं। तीसरे वर्ग में संतोष, निष्क्रमणता और अव्याबाध सुख रखे जा सकते हैं।
इनमें से अव्याबाध सुख तो अरिहंत-सिद्ध अवस्था का सुख है, और वह भूमिका नीति से परे है। निष्क्रमण सुख नैतिकता का चरम है और सन्तोष सुख नीति के अन्तर्गत मनुष्य मात्र के लिए आता है।
यद्यपि साधु सन्तोषी होता है, किन्तु पश्चिमी नीतिशास्त्र में नैतिक सुख की जो अवधारणा है, वह आगम वर्णित सुख से भली भाँति अभिव्यक्त हो जाती है।
सुखवाद की अवधारणा को स्वीकार करते हुए भी जैन दर्शन एक मात्र इसी को साध्य मानता, वह ज्ञानात्मक पक्ष को भी उतना ही महत्व देता है। सिद्धजीवों में ज्ञान-दर्शन के पश्चात सुख का ही क्रम रखा गया और सुख, अव्याबाध सुख की अवधारणा का कारण भी अनन्तज्ञान दर्शन को माना गया है। 1. स्थानांग सूत्र, स्थान 10, सूत्र 737, संपादक : मुनिश्री कन्हैयालालजी कमल