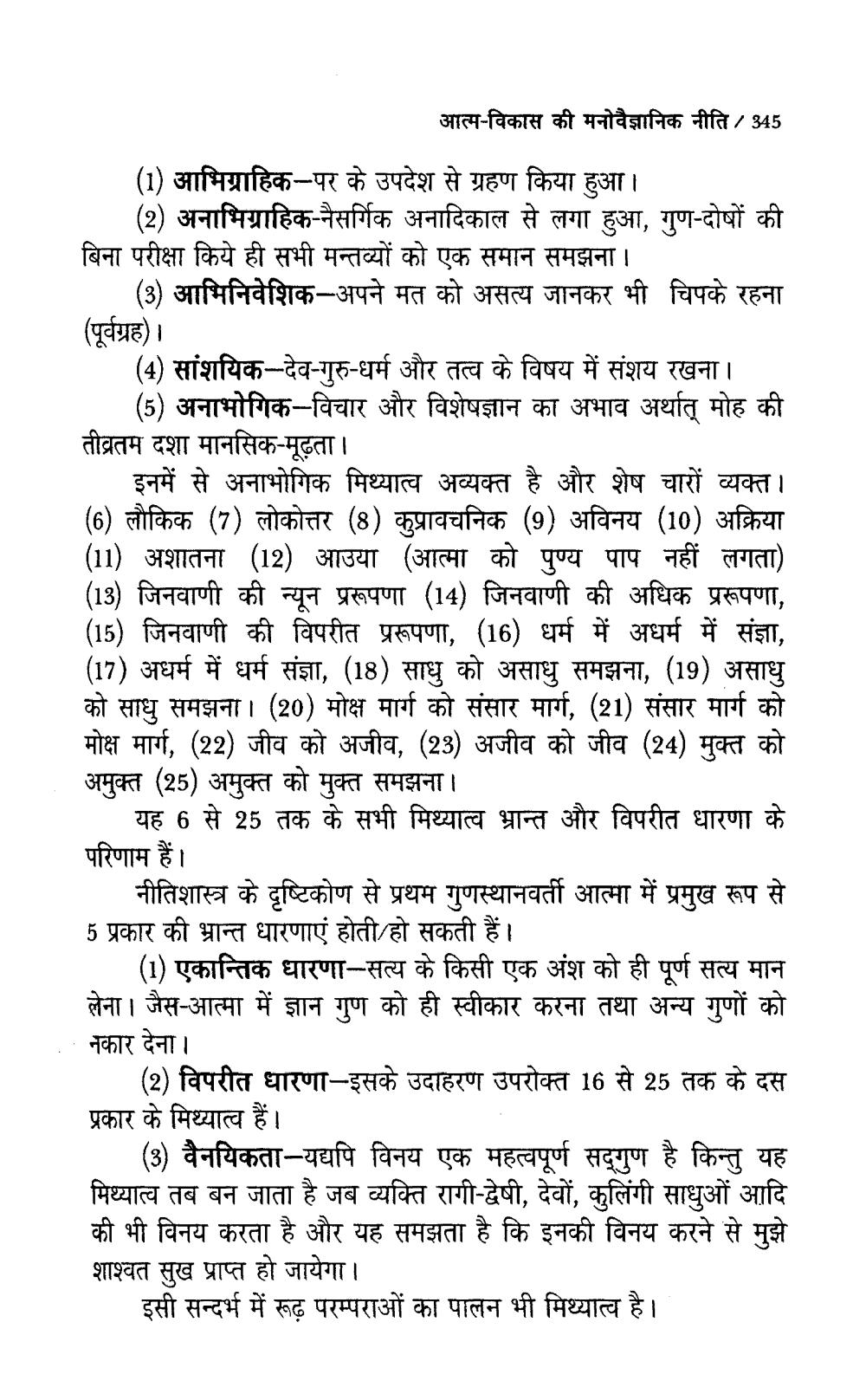________________
आत्म-विकास की मनोवैज्ञानिक नीति / 345
(1) आभिग्राहिक - पर के उपदेश से ग्रहण किया हुआ । (2) अनाभिग्राहिक - नैसर्गिक अनादिकाल से लगा हुआ, गुण-दोषों की बिना परीक्षा किये ही सभी मन्तव्यों को एक समान समझना ।
(3) आभिनिवेशिक - अपने मत को असत्य जानकर भी चिपके रहना (पूर्वग्रह ) ।
(4) सांशयिक - देव - गुरु- धर्म और तत्व के विषय में संशय रखना । ( 5 ) अनाभोगिक - विचार और विशेषज्ञान का अभाव अर्थात् मोह की तीव्रतम दशा मानसिक- मूढ़ता ।
(
इनमें से अनाभोगिक मिथ्यात्व अव्यक्त है और शेष चारों व्यक्त । ( 6 ) लौकिक ( 7 ) लोकोत्तर (8) कुप्रावचनिक ( 9 ) अविनय ( 10 ) अक्रिया ( 11 ) अशातना ( 12 ) आउया (आत्मा को पुण्य पाप नहीं लगता ) 13 ) जिनवाणी की न्यून प्ररूपणा ( 14 ) जिनवाणी की अधिक प्ररूपणा, ( 15 ) जिनवाणी की विपरीत प्ररूपणा, ( 16 ) धर्म में अधर्म में संज्ञा, ( 17 ) अधर्म में धर्म संज्ञा, ( 18 ) साधु को असाधु समझना, ( 19 ) असाधु को साधु समझना । ( 20 ) मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग, ( 21 ) संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग, (22) जीव को अजीव, ( 23 ) अजीव को जीव (24) मुक्त को अमुक्त ( 25 ) अमुक्त को मुक्त समझना ।
यह 6 से 25 तक के सभी मिथ्यात्व भ्रान्त और विपरीत धारणा के परिणाम हैं।
नीतिशास्त्र के दृष्टिकोण से प्रथम गुणस्थानवर्ती आत्मा में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की भ्रान्त धारणाएं होती / हो सकती हैं ।
(1) एकान्तिक धारणा - सत्य के किसी एक अंश को ही पूर्ण सत्य मान लेना । जैस - आत्मा में ज्ञान गुण को ही स्वीकार करना तथा अन्य गुणों को नकार देना ।
(2) विपरीत धारणा - इसके उदाहरण उपरोक्त 16 से 25 तक के दस प्रकार के मिथ्यात्व हैं 1
(3) वैनयिकता - यद्यपि विनय एक महत्वपूर्ण सद्गुण है किन्तु यह मिथ्यात्व तब बन जाता है जब व्यक्ति रागी -द्वेषी, देवों, कुलिंगी साधुओं आदि की भी विनय करता है और यह समझता है कि इनकी विनय करने से मुझे शाश्वत सुख प्राप्त हो जायेगा ।
इसी सन्दर्भ में रूढ़ परम्पराओं का पालन भी मिथ्यात्व है।