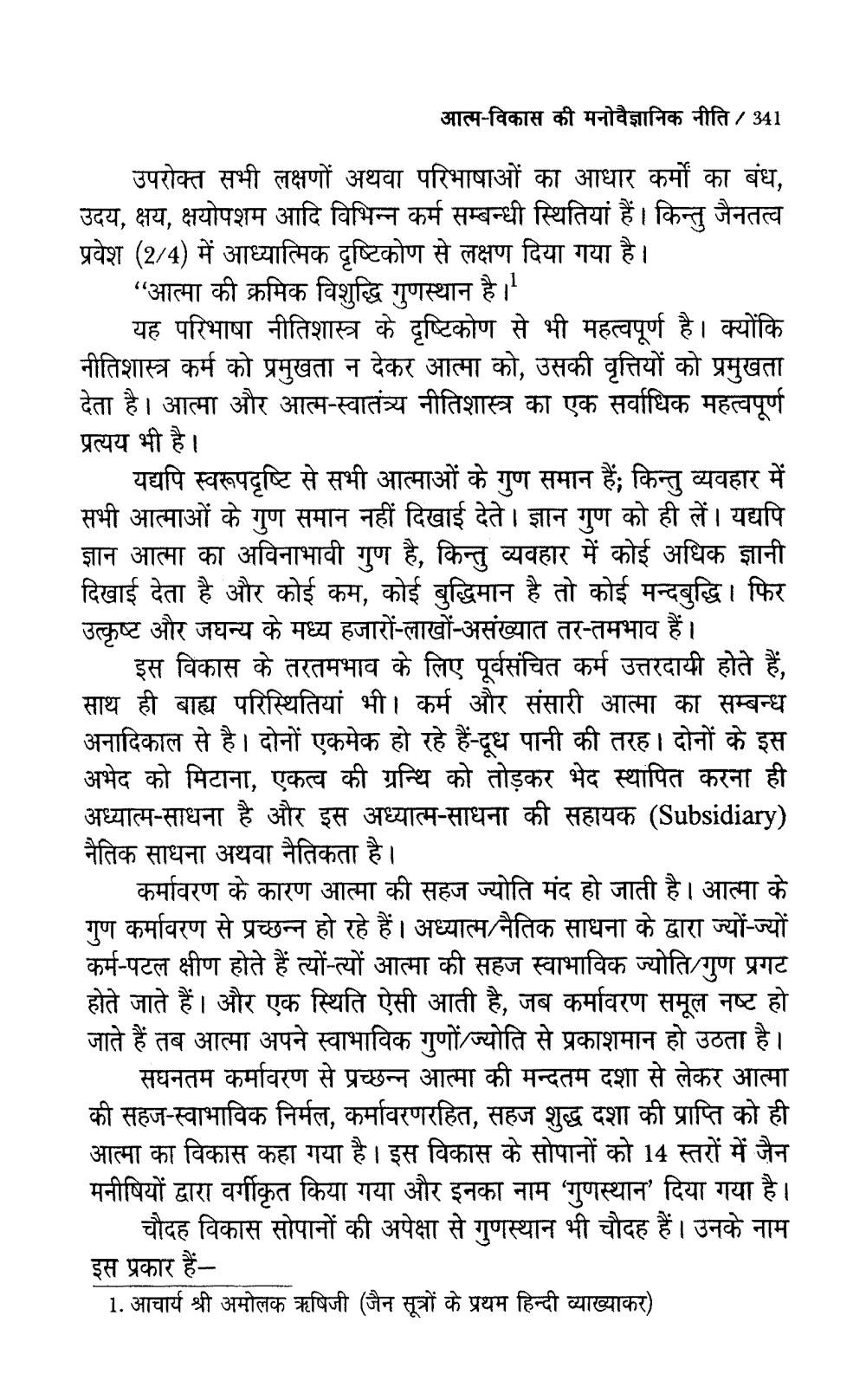________________
आत्म-विकास की मनोवैज्ञानिक नीति / 341
उपरोक्त सभी लक्षणों अथवा परिभाषाओं का आधार कर्मों का बंध, उदय, क्षय, क्षयोपशम आदि विभिन्न कर्म सम्बन्धी स्थितियां हैं । किन्तु जैनतत्व प्रवेश (2/4) में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लक्षण दिया गया है।
"आत्मा की क्रमिक विशुद्धि गुणस्थान 'है । '
यह परिभाषा नीतिशास्त्र के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि नीतिशास्त्र कर्म को प्रमुखता न देकर आत्मा को, उसकी वृत्तियों को प्रमुखता देता है। आत्मा और आत्म - स्वातंत्र्य नीतिशास्त्र का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रत्यय भी है।
I
यद्यपि स्वरूपदृष्टि से सभी आत्माओं के गुण समान हैं; किन्तु व्यवहार में सभी आत्माओं के गुण समान नहीं दिखाई देते । ज्ञान गुण को ही लें । यद्यपि ज्ञान आत्मा का अविनाभावी गुण है, किन्तु व्यवहार में कोई अधिक ज्ञानी दिखाई देता है और कोई कम, कोई बुद्धिमान है तो कोई मन्दबुद्धि । फिर उत्कृष्ट और जघन्य के मध्य हजारों-लाखों - असंख्यात तर - तमभाव हैं ।
इस विकास के तरतमभाव के लिए पूर्वसंचित कर्म उत्तरदायी होते हैं, साथ ही बाह्य परिस्थितियां भी । कर्म और संसारी आत्मा का सम्बन्ध अनादिकाल से है। दोनों एकमेक हो रहे हैं-दूध पानी की तरह। दोनों के इस अभेद को मिटाना, एकत्व की ग्रन्थि को तोड़कर भेद स्थापित करना ही अध्यात्म-साधना है और इस अध्यात्म-साधना की सहायक (Subsidiary) नैतिक साधना अथवा नैतिकता है ।
कर्मावरण के कारण आत्मा की सहज ज्योति मंद हो जाती है । आत्मा के गुणकर्मावरण से प्रच्छन्न हो रहे हैं । अध्यात्म / नैतिक साधना के द्वारा ज्यों-ज्यों कर्म-पटल क्षीण होते हैं त्यों-त्यों आत्मा की सहज स्वाभाविक ज्योति / गुण प्रगट होते जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है, जब कर्मावरण समूल नष्ट हो जाते हैं तब आत्मा अपने स्वाभाविक गुणों / ज्योति से प्रकाशमान हो उठता है ।
सघनतम कर्मावरण से प्रच्छन्न आत्मा की मन्दतम दशा से लेकर आत्मा की सहज-स्वाभाविक निर्मल, कर्मावरणरहित, सहज शुद्ध दशा की प्राप्ति को ही आत्मा का विकास कहा गया है। इस विकास के सोपानों को 14 स्तरों में जैन मनीषियों द्वारा वर्गीकृत किया गया और इनका नाम 'गुणस्थान' दिया गया है । चौदह विकास सोपानों की अपेक्षा से गुणस्थान भी चौदह हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं
1. आचार्य श्री अमोलक ऋषिजी (जैन सूत्रों के प्रथम हिन्दी व्याख्याकर)