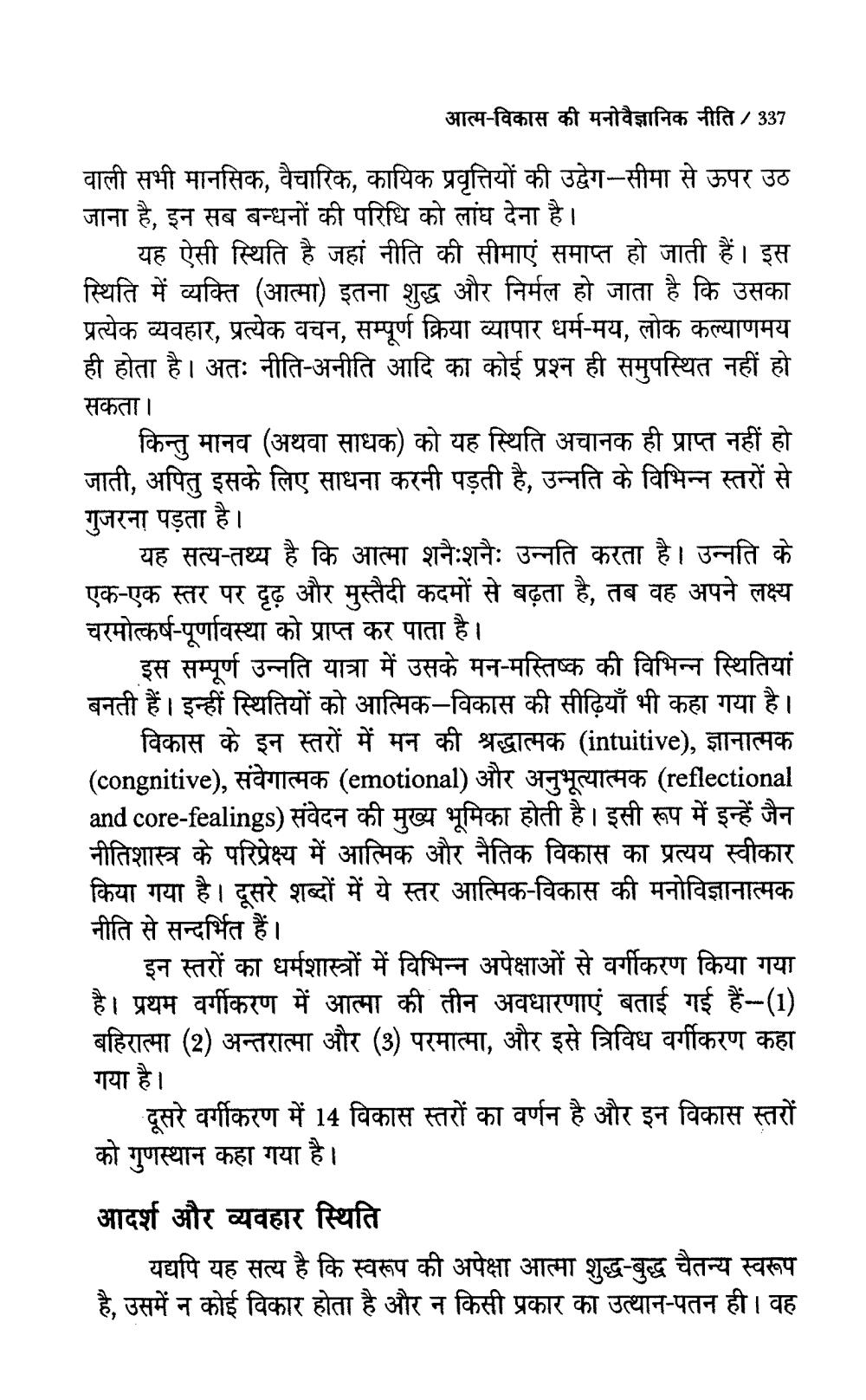________________
आत्म-विकास की मनोवैज्ञानिक नीति / 337
वाली सभी मानसिक, वैचारिक, कायिक प्रवृत्तियों की उद्वेग-सीमा से ऊपर उठ जाना है, इन सब बन्धनों की परिधि को लांघ देना है।
यह ऐसी स्थिति है जहां नीति की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति (आत्मा) इतना शुद्ध और निर्मल हो जाता है कि उसका प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक वचन, सम्पूर्ण क्रिया व्यापार धर्म-मय, लोक कल्याणमय ही होता है। अतः नीति-अनीति आदि का कोई प्रश्न ही समुपस्थित नहीं हो सकता।
किन्तु मानव (अथवा साधक) को यह स्थिति अचानक ही प्राप्त नहीं हो जाती, अपितु इसके लिए साधना करनी पड़ती है, उन्नति के विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है।
यह सत्य-तथ्य है कि आत्मा शनैःशनैः उन्नति करता है। उन्नति के एक-एक स्तर पर दृढ़ और मुस्तैदी कदमों से बढ़ता है, तब वह अपने लक्ष्य चरमोत्कर्ष-पूर्णावस्था को प्राप्त कर पाता है।
इस सम्पूर्ण उन्नति यात्रा में उसके मन-मस्तिष्क की विभिन्न स्थितियां बनती हैं। इन्हीं स्थितियों को आत्मिक-विकास की सीढ़ियाँ भी कहा गया है।
विकास के इन स्तरों में मन की श्रद्धात्मक (intuitive), ज्ञानात्मक (congnitive), संवेगात्मक (emotional) और अनुभूत्यात्मक (reflectional and core-fealings) संवेदन की मुख्य भूमिका होती है। इसी रूप में इन्हें जैन नीतिशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में आत्मिक और नैतिक विकास का प्रत्यय स्वीकार किया गया है। दूसरे शब्दों में ये स्तर आत्मिक-विकास की मनोविज्ञानात्मक नीति से सन्दर्भित हैं।
इन स्तरों का धर्मशास्त्रों में विभिन्न अपेक्षाओं से वर्गीकरण किया गया है। प्रथम वर्गीकरण में आत्मा की तीन अवधारणाएं बताई गई हैं-(1) बहिरात्मा (2) अन्तरात्मा और (3) परमात्मा, और इसे त्रिविध वर्गीकरण कहा गया है।
दूसरे वर्गीकरण में 14 विकास स्तरों का वर्णन है और इन विकास स्तरों को गुणस्थान कहा गया है। आदर्श और व्यवहार स्थिति
यद्यपि यह सत्य है कि स्वरूप की अपेक्षा आत्मा शुद्ध-बुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उसमें न कोई विकार होता है और न किसी प्रकार का उत्थान-पतन ही। वह