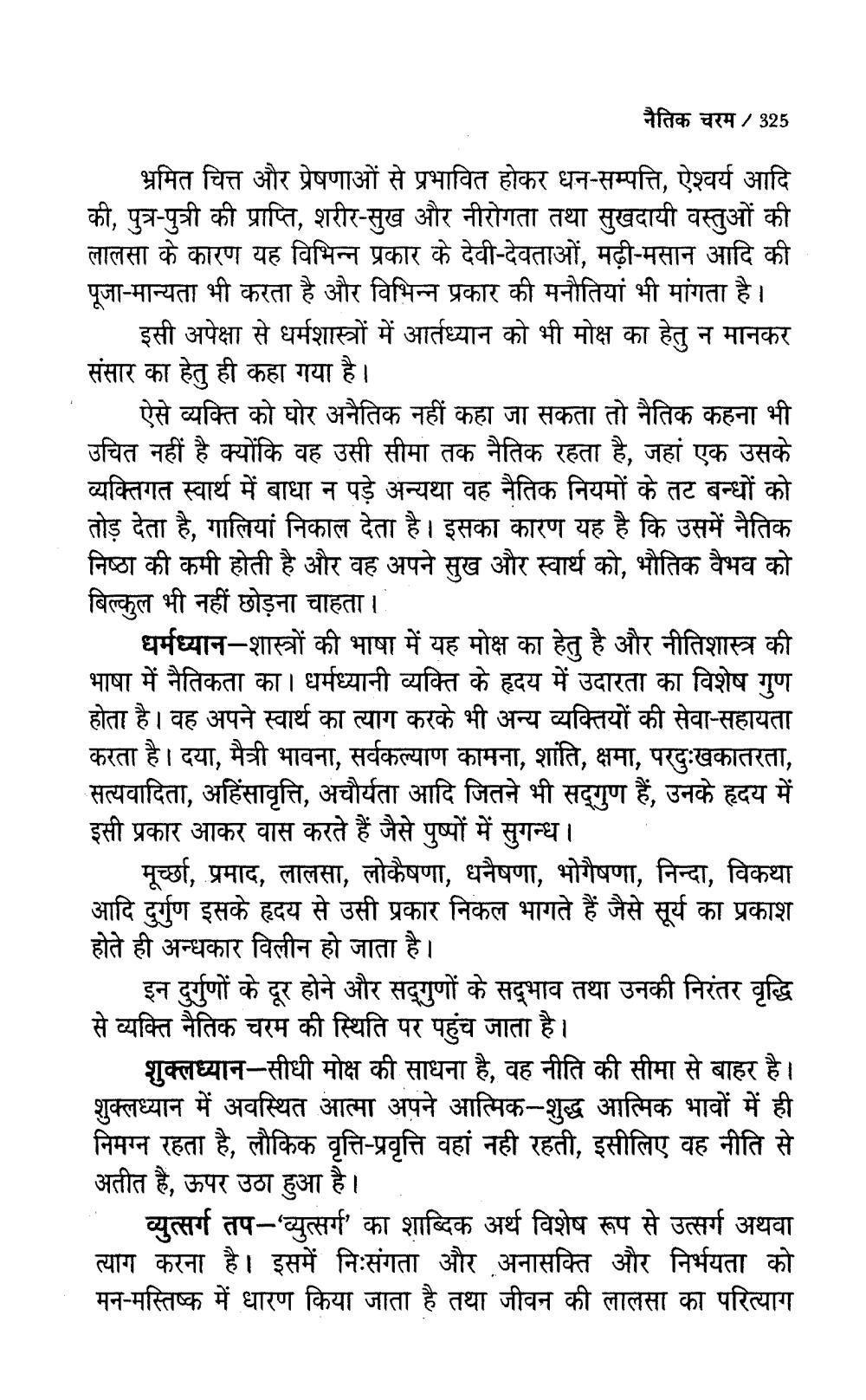________________
नैतिक चरम / 325
भ्रमित चित्त और प्रेषणाओं से प्रभावित होकर धन-सम्पत्ति, ऐश्वर्य आदि की, पुत्र-पुत्री की प्राप्ति, शरीर-सुख और नीरोगता तथा सुखदायी वस्तुओं की लालसा के कारण यह विभिन्न प्रकार के देवी-देवताओं, मढ़ी-मसान आदि की पूजा-मान्यता भी करता है और विभिन्न प्रकार की मनौतियां भी मांगता है।
इसी अपेक्षा से धर्मशास्त्रों में आर्तध्यान को भी मोक्ष का हेतु न मानकर संसार का हेतु ही कहा गया है।
ऐसे व्यक्ति को घोर अनैतिक नहीं कहा जा सकता तो नैतिक कहना भी उचित नहीं है क्योंकि वह उसी सीमा तक नैतिक रहता है, जहां एक उसके व्यक्तिगत स्वार्थ में बाधा न पड़े अन्यथा वह नैतिक नियमों के तट बन्धों को तोड़ देता है, गालियां निकाल देता है। इसका कारण यह है कि उसमें नैतिक निष्ठा की कमी होती है और वह अपने सुख और स्वार्थ को, भौतिक वैभव को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता।
धर्मध्यान-शास्त्रों की भाषा में यह मोक्ष का हेतु है और नीतिशास्त्र की भाषा में नैतिकता का। धर्मध्यानी व्यक्ति के हृदय में उदारता का विशेष गुण होता है। वह अपने स्वार्थ का त्याग करके भी अन्य व्यक्तियों की सेवा-सहायता करता है। दया, मैत्री भावना, सर्वकल्याण कामना, शांति, क्षमा, परदुःखकातरता, सत्यवादिता, अहिंसावृत्ति, अचौर्यता आदि जितने भी सद्गुण हैं, उनके हृदय में इसी प्रकार आकर वास करते हैं जैसे पुष्पों में सुगन्ध।।
मूर्छा, प्रमाद, लालसा, लोकेषणा, धनैषणा, भोगैषणा, निन्दा, विकथा आदि दुर्गुण इसके हृदय से उसी प्रकार निकल भागते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही अन्धकार विलीन हो जाता है।
इन दुर्गुणों के दूर होने और सद्गुणों के सद्भाव तथा उनकी निरंतर वृद्धि से व्यक्ति नैतिक चरम की स्थिति पर पहुंच जाता है।
शुक्लध्यान-सीधी मोक्ष की साधना है, वह नीति की सीमा से बाहर है। शुक्लध्यान में अवस्थित आत्मा अपने आत्मिक-शुद्ध आत्मिक भावों में ही निमग्न रहता है, लौकिक वृत्ति-प्रवृत्ति वहां नही रहती, इसीलिए वह नीति से अतीत है, ऊपर उठा हुआ है। - व्युत्सर्ग तप-'व्युत्सर्ग' का शाब्दिक अर्थ विशेष रूप से उत्सर्ग अथवा त्याग करना है। इसमें निःसंगता और अनासक्ति और निर्भयता को मन-मस्तिष्क में धारण किया जाता है तथा जीवन की लालसा का परित्याग