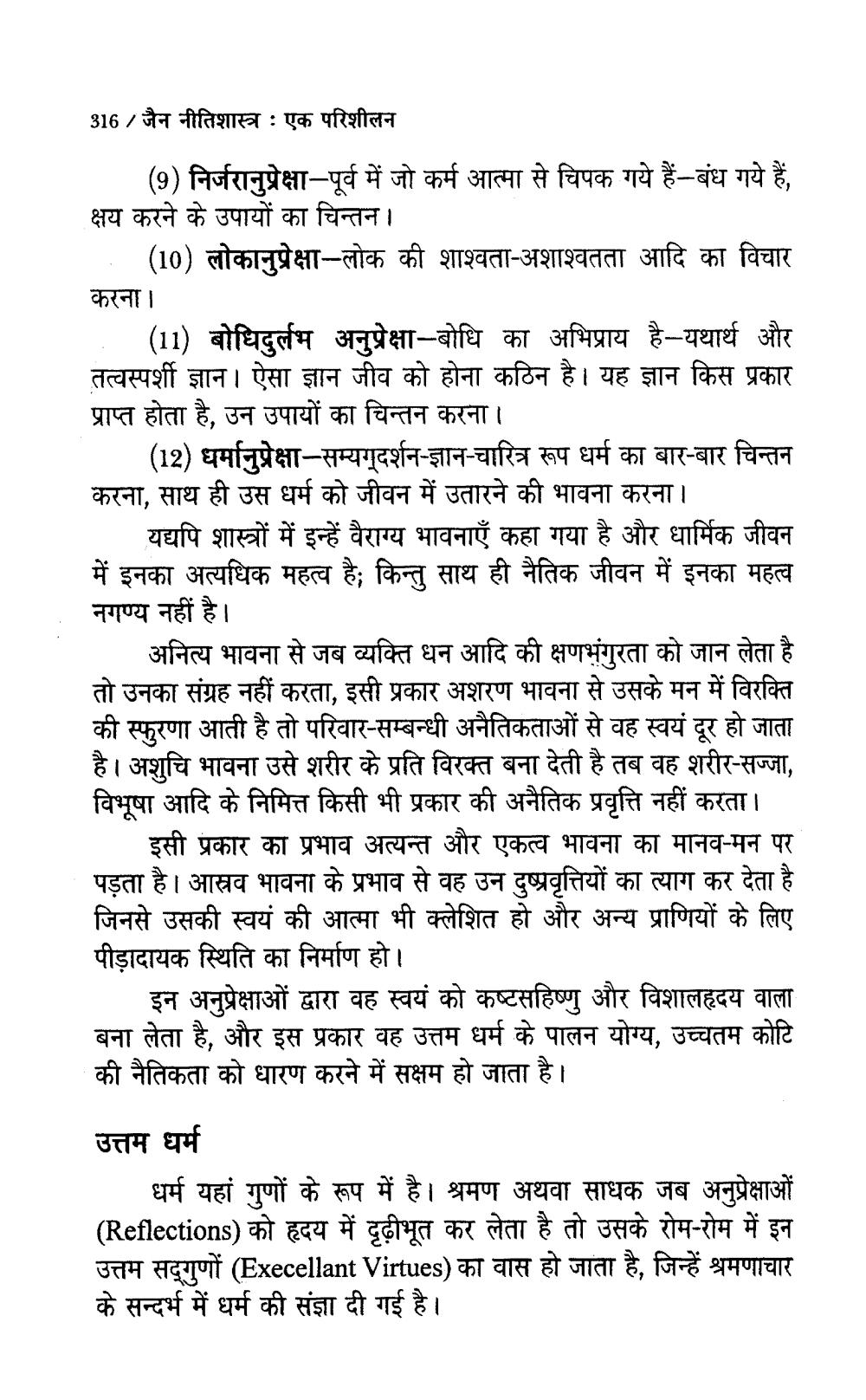________________
316 / जैन नीतिशास्त्र : एक परिशीलन
(9) निर्जरानुप्रेक्षा-पूर्व में जो कर्म आत्मा से चिपक गये हैं-बंध गये हैं, क्षय करने के उपायों का चिन्तन। .(10) लोकानुप्रेक्षा-लोक की शाश्वता-अशाश्वतता आदि का विचार करना। . (11) बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षा-बोधि का अभिप्राय है-यथार्थ और तत्वस्पर्शी ज्ञान। ऐसा ज्ञान जीव को होना कठिन है। यह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है, उन उपायों का चिन्तन करना।
(12) धर्मानुप्रेक्षा-सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप धर्म का बार-बार चिन्तन करना, साथ ही उस धर्म को जीवन में उतारने की भावना करना।
यद्यपि शास्त्रों में इन्हें वैराग्य भावनाएँ कहा गया है और धार्मिक जीवन में इनका अत्यधिक महत्व है; किन्तु साथ ही नैतिक जीवन में इनका महत्व नगण्य नहीं है।
अनित्य भावना से जब व्यक्ति धन आदि की क्षणभंगुरता को जान लेता है तो उनका संग्रह नहीं करता, इसी प्रकार अशरण भावना से उसके मन में विरक्ति की स्फुरणा आती है तो परिवार-सम्बन्धी अनैतिकताओं से वह स्वयं दूर हो जाता है। अशुचि भावना उसे शरीर के प्रति विरक्त बना देती है तब वह शरीर-सज्जा, विभूषा आदि के निमित्त किसी भी प्रकार की अनैतिक प्रवृत्ति नहीं करता।
इसी प्रकार का प्रभाव अत्यन्त और एकत्व भावना का मानव-मन पर पड़ता है। आस्रव भावना के प्रभाव से वह उन दुष्प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है जिनसे उसकी स्वयं की आत्मा भी क्लेशित हो और अन्य प्राणियों के लिए पीड़ादायक स्थिति का निर्माण हो।
इन अनुप्रेक्षाओं द्वारा वह स्वयं को कष्टसहिष्णु और विशालहृदय वाला बना लेता है, और इस प्रकार वह उत्तम धर्म के पालन योग्य, उच्चतम कोटि की नैतिकता को धारण करने में सक्षम हो जाता है।
उत्तम धर्म
धर्म यहां गुणों के रूप में है। श्रमण अथवा साधक जब अनुप्रेक्षाओं (Reflections) को हृदय में दृढ़ीभूत कर लेता है तो उसके रोम-रोम में इन उत्तम सद्गुणों (Execellant Virtues) का वास हो जाता है, जिन्हें श्रमणाचार के सन्दर्भ में धर्म की संज्ञा दी गई है।