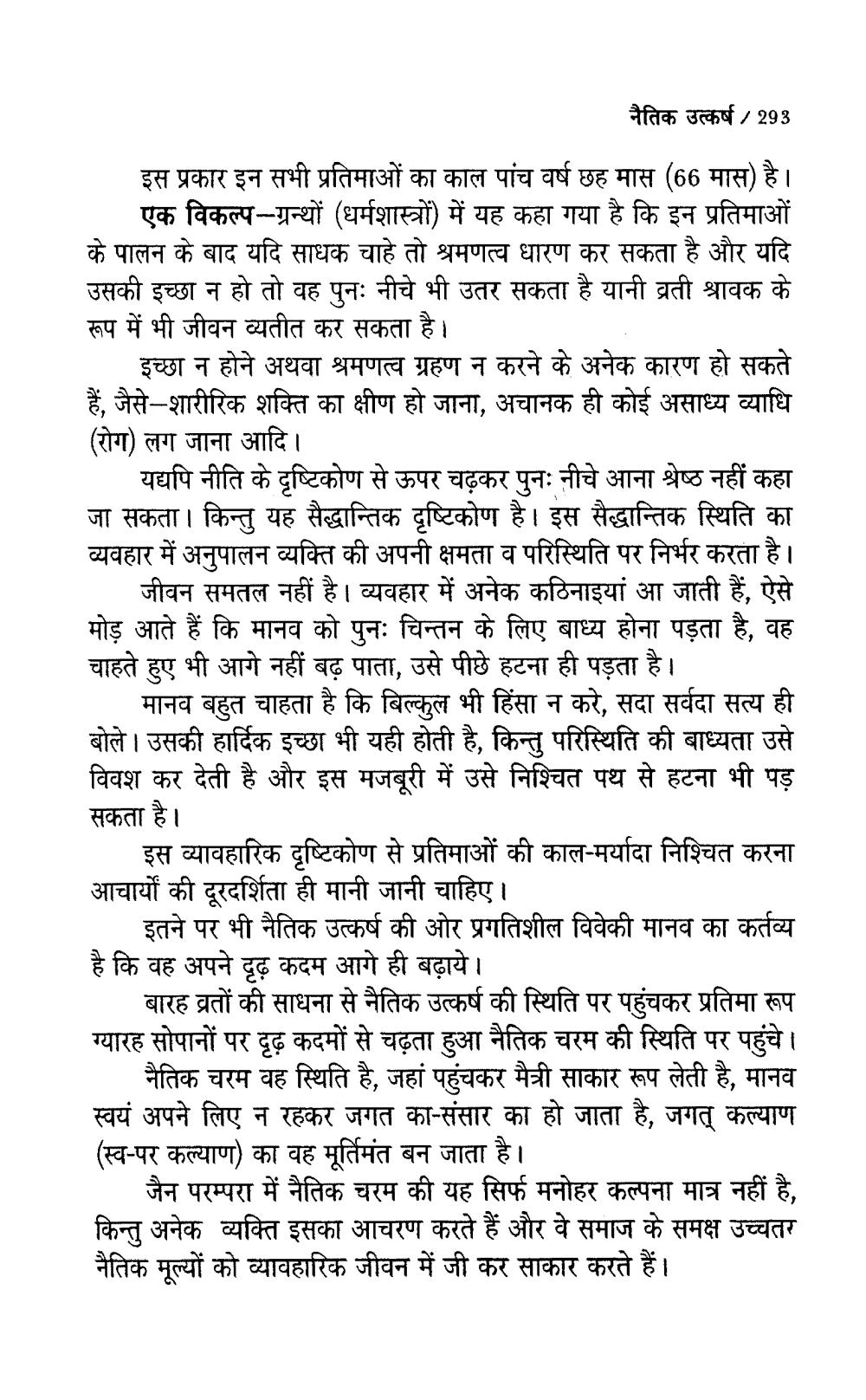________________
नैतिक उत्कर्ष / 293
इस प्रकार इन सभी प्रतिमाओं का काल पांच वर्ष छह मास (66 मास) है।
एक विकल्प-ग्रन्थों (धर्मशास्त्रों) में यह कहा गया है कि इन प्रतिमाओं के पालन के बाद यदि साधक चाहे तो श्रमणत्व धारण कर सकता है और यदि उसकी इच्छा न हो तो वह पुनः नीचे भी उतर सकता है यानी व्रती श्रावक के रूप में भी जीवन व्यतीत कर सकता है।
इच्छा न होने अथवा श्रमणत्व ग्रहण न करने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे-शारीरिक शक्ति का क्षीण हो जाना, अचानक ही कोई असाध्य व्याधि (रोग) लग जाना आदि।
यद्यपि नीति के दृष्टिकोण से ऊपर चढ़कर पुनः नीचे आना श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। किन्तु यह सैद्धान्तिक दृष्टिकोण है। इस सैद्धान्तिक स्थिति का व्यवहार में अनुपालन व्यक्ति की अपनी क्षमता व परिस्थिति पर निर्भर करता है।
जीवन समतल नहीं है। व्यवहार में अनेक कठिनाइयां आ जाती हैं, ऐसे मोड़ आते हैं कि मानव को पुनः चिन्तन के लिए बाध्य होना पड़ता है, वह चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाता, उसे पीछे हटना ही पड़ता है।
मानव बहुत चाहता है कि बिल्कुल भी हिंसा न करे, सदा सर्वदा सत्य ही बोले। उसकी हार्दिक इच्छा भी यही होती है, किन्तु परिस्थिति की बाध्यता उसे विवश कर देती है और इस मजबूरी में उसे निश्चित पथ से हटना भी पड़ सकता है।
इस व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रतिमाओं की काल-मर्यादा निश्चित करना आचार्यों की दूरदर्शिता ही मानी जानी चाहिए।
इतने पर भी नैतिक उत्कर्ष की ओर प्रगतिशील विवेकी मानव का कर्तव्य है कि वह अपने दृढ़ कदम आगे ही बढ़ाये।
बारह व्रतों की साधना से नैतिक उत्कर्ष की स्थिति पर पहुंचकर प्रतिमा रूप ग्यारह सोपानों पर दृढ़ कदमों से चढ़ता हुआ नैतिक चरम की स्थिति पर पहुंचे।
नैतिक चरम वह स्थिति है, जहां पहुंचकर मैत्री साकार रूप लेती है, मानव स्वयं अपने लिए न रहकर जगत का-संसार का हो जाता है, जगत् कल्याण (स्व-पर कल्याण) का वह मूर्तिमंत बन जाता है।
जैन परम्परा में नैतिक चरम की यह सिर्फ मनोहर कल्पना मात्र नहीं है, किन्तु अनेक व्यक्ति इसका आचरण करते हैं और वे समाज के समक्ष उच्चतर नैतिक मूल्यों को व्यावहारिक जीवन में जी कर साकार करते हैं।