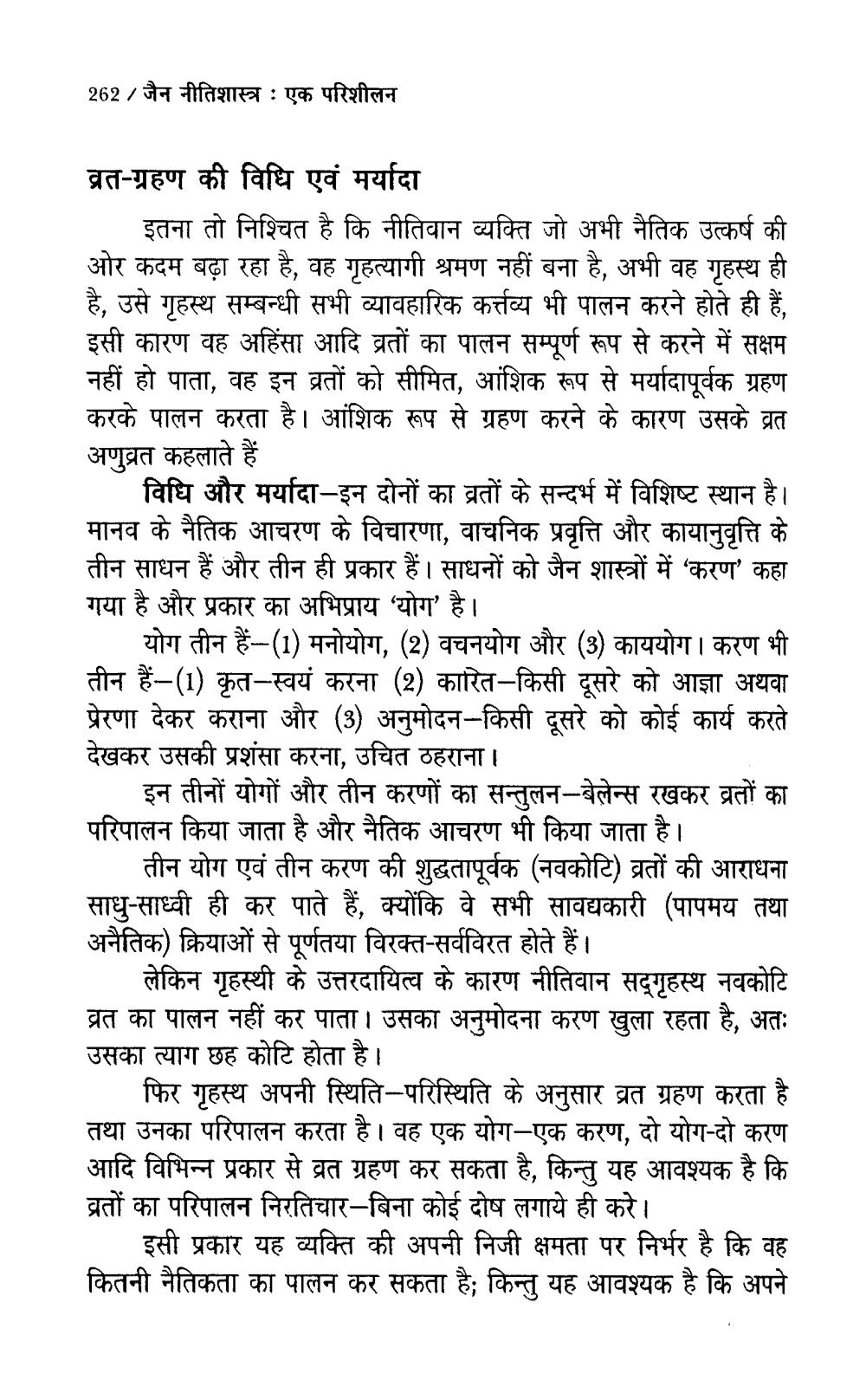________________
262 / जैन नीतिशास्त्र : एक परिशीलन
व्रत-ग्रहण की विधि एवं मर्यादा
इतना तो निश्चित है कि नीतिवान व्यक्ति जो अभी नैतिक उत्कर्ष की ओर कदम बढ़ा रहा है, वह गृहत्यागी श्रमण नहीं बना है, अभी वह गृहस्थ ही है, उसे गृहस्थ सम्बन्धी सभी व्यावहारिक कर्त्तव्य भी पालन करने होते ही हैं, इसी कारण वह अहिंसा आदि व्रतों का पालन सम्पूर्ण रूप से करने में सक्षम नहीं हो पाता, वह इन व्रतों को सीमित, आंशिक रूप से मर्यादापूर्वक ग्रहण करके पालन करता है। आंशिक रूप से ग्रहण करने के कारण उसके व्रत अणुव्रत कहलाते हैं
विधि और मर्यादा-इन दोनों का व्रतों के सन्दर्भ में विशिष्ट स्थान है। मानव के नैतिक आचरण के विचारणा, वाचनिक प्रवृत्ति और कायानुवृत्ति के तीन साधन हैं और तीन ही प्रकार हैं। साधनों को जैन शास्त्रों में 'करण' कहा गया है और प्रकार का अभिप्राय 'योग' है।
योग तीन हैं-(1) मनोयोग, (2) वचनयोग और (3) काययोग। करण भी तीन हैं-(1) कृत-स्वयं करना (2) कारित-किसी दूसरे को आज्ञा अथवा प्रेरणा देकर कराना और (3) अनुमोदन-किसी दूसरे को कोई कार्य करते देखकर उसकी प्रशंसा करना, उचित ठहराना।
इन तीनों योगों और तीन करणों का सन्तुलन–बेलेन्स रखकर व्रतों का परिपालन किया जाता है और नैतिक आचरण भी किया जाता है।
तीन योग एवं तीन करण की शुद्धतापूर्वक (नवकोटि) व्रतों की आराधना साधु-साध्वी ही कर पाते हैं, क्योंकि वे सभी सावधकारी (पापमय तथा अनैतिक) क्रियाओं से पूर्णतया विरक्त-सर्वविरत होते हैं।
लेकिन गृहस्थी के उत्तरदायित्व के कारण नीतिवान सद्गृहस्थ नवकोटि व्रत का पालन नहीं कर पाता। उसका अनुमोदना करण खुला रहता है, अतः उसका त्याग छह कोटि होता है।
फिर गृहस्थ अपनी स्थिति-परिस्थिति के अनुसार व्रत ग्रहण करता है तथा उनका परिपालन करता है। वह एक योग-एक करण, दो योग-दो करण आदि विभिन्न प्रकार से व्रत ग्रहण कर सकता है, किन्तु यह आवश्यक है कि व्रतों का परिपालन निरतिचार-बिना कोई दोष लगाये ही करे।
इसी प्रकार यह व्यक्ति की अपनी निजी क्षमता पर निर्भर है कि वह कितनी नैतिकता का पालन कर सकता है; किन्तु यह आवश्यक है कि अपने