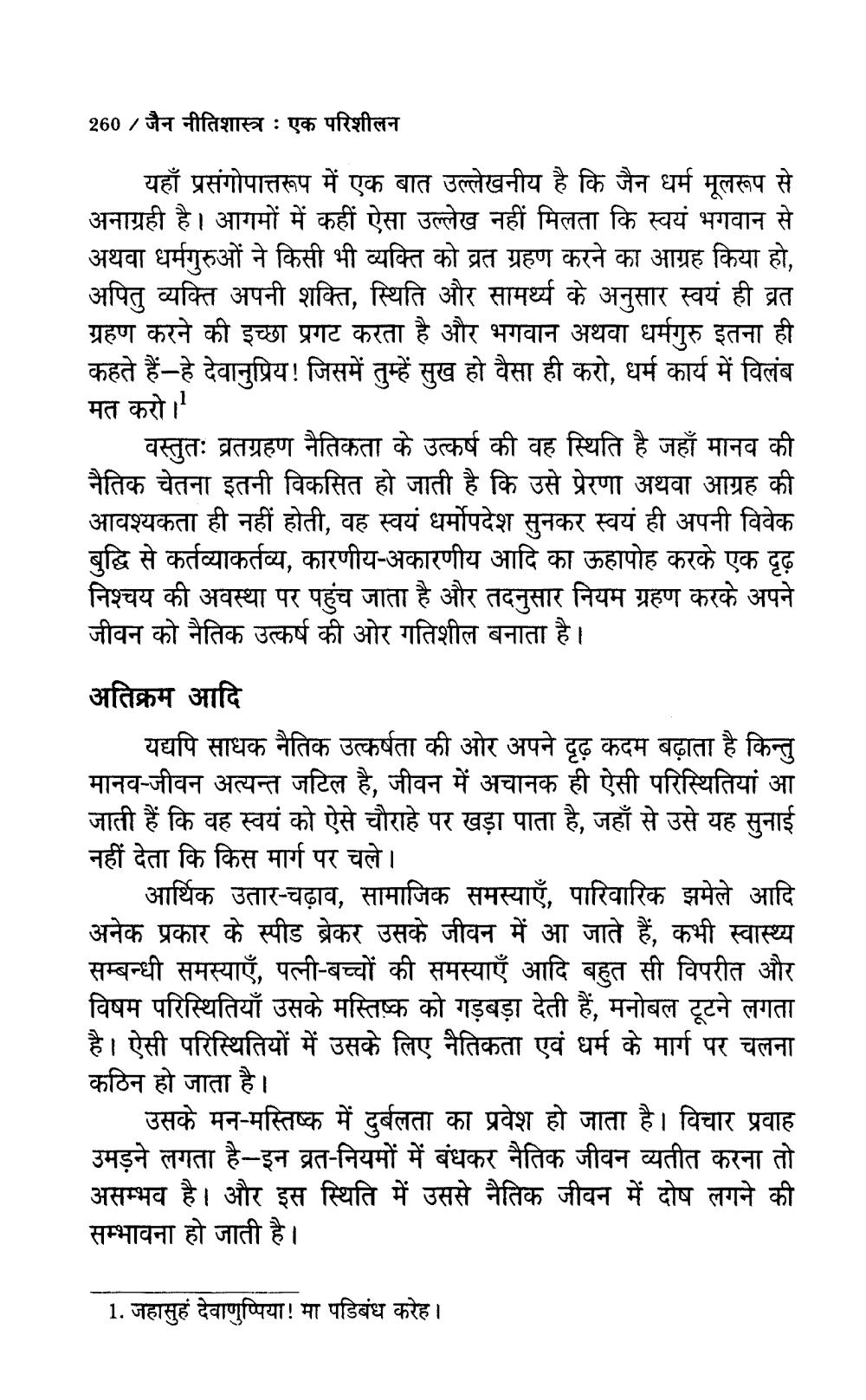________________
260 / जैन नीतिशास्त्र : एक परिशीलन
यहाँ प्रसंगोपात्तरूप में एक बात उल्लेखनीय है कि जैन धर्म मूलरूप से अनाग्रही है। आगमों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि स्वयं भगवान से अथवा धर्मगुरुओं ने किसी भी व्यक्ति को व्रत ग्रहण करने का आग्रह किया हो, अपितु व्यक्ति अपनी शक्ति, स्थिति और सामर्थ्य के अनुसार स्वयं ही व्रत ग्रहण करने की इच्छा प्रगट करता है और भगवान अथवा धर्मगुरु इतना ही कहते हैं-हे देवानुप्रिय! जिसमें तुम्हें सुख हो वैसा ही करो, धर्म कार्य में विलंब मत करो।
वस्तुतः व्रतग्रहण नैतिकता के उत्कर्ष की वह स्थिति है जहाँ मानव की नैतिक चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि उसे प्रेरणा अथवा आग्रह की आवश्यकता ही नहीं होती, वह स्वयं धर्मोपदेश सुनकर स्वयं ही अपनी विवेक बुद्धि से कर्तव्याकर्तव्य, कारणीय-अकारणीय आदि का ऊहापोह करके एक दृढ़ निश्चय की अवस्था पर पहुंच जाता है और तदनुसार नियम ग्रहण करके अपने जीवन को नैतिक उत्कर्ष की ओर गतिशील बनाता है।
अतिक्रम आदि
यद्यपि साधक नैतिक उत्कर्षता की ओर अपने दृढ़ कदम बढ़ाता है किन्तु मानव-जीवन अत्यन्त जटिल है, जीवन में अचानक ही ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वह स्वयं को ऐसे चौराहे पर खड़ा पाता है, जहाँ से उसे यह सुनाई नहीं देता कि किस मार्ग पर चले।
आर्थिक उतार-चढ़ाव, सामाजिक समस्याएँ, पारिवारिक झमेले आदि अनेक प्रकार के स्पीड ब्रेकर उसके जीवन में आ जाते हैं, कभी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ, पत्नी-बच्चों की समस्याएँ आदि बहुत सी विपरीत और विषम परिस्थितियाँ उसके मस्तिष्क को गड़बड़ा देती हैं, मनोबल टूटने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में उसके लिए नैतिकता एवं धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो जाता है।
उसके मन-मस्तिष्क में दुर्बलता का प्रवेश हो जाता है। विचार प्रवाह उमड़ने लगता है-इन व्रत-नियमों में बंधकर नैतिक जीवन व्यतीत करना तो असम्भव है। और इस स्थिति में उससे नैतिक जीवन में दोष लगने की सम्भावना हो जाती है।
1. जहासुहं देवाणुप्पिया! मा पडिबंध करेह।