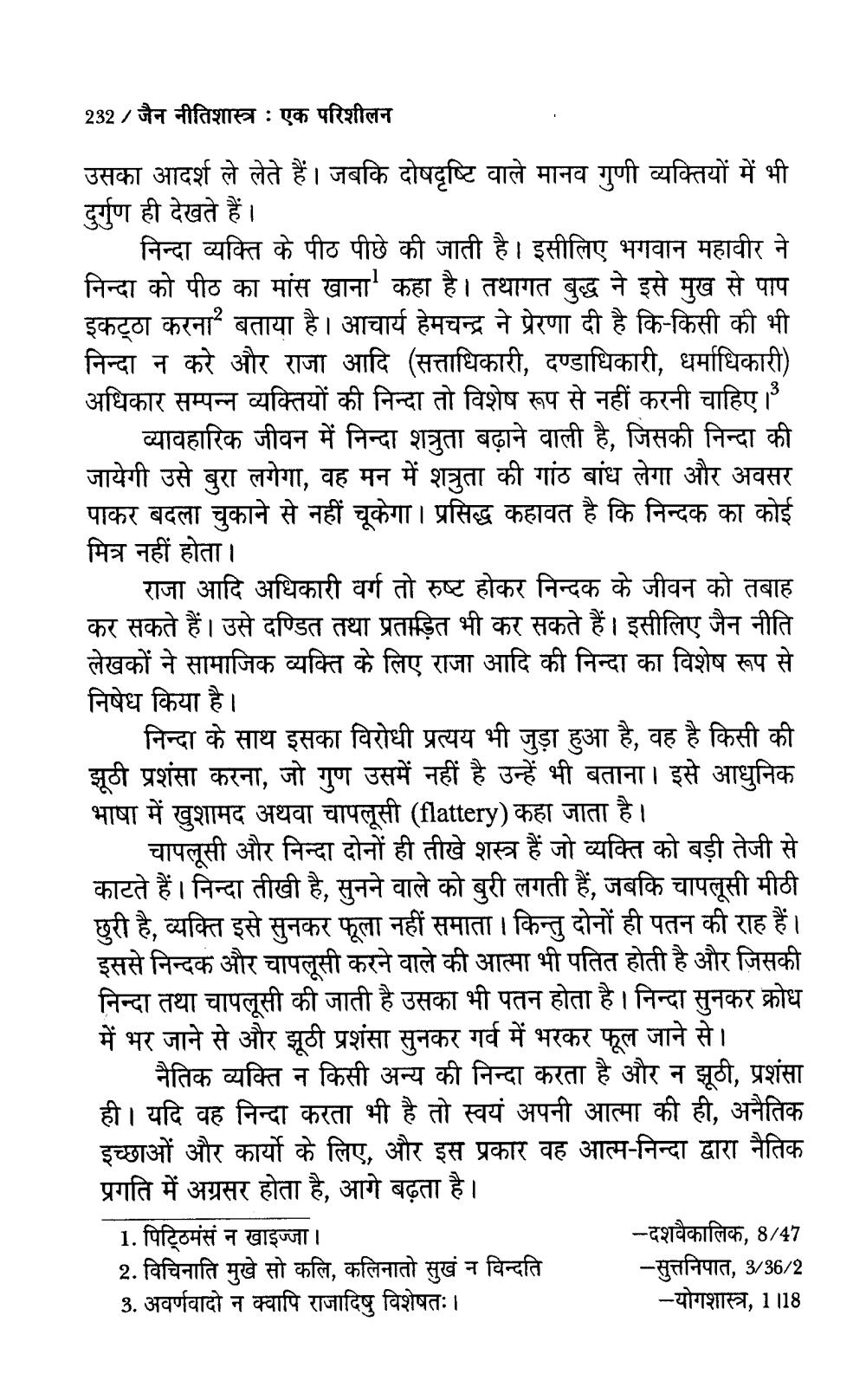________________
232 / जैन नीतिशास्त्र : एक परिशीलन
उसका आदर्श ले लेते हैं। जबकि दोषदृष्टि वाले मानव गुणी व्यक्तियों में भी दुर्गुण ही देखते हैं।
निन्दा व्यक्ति के पीठ पीछे की जाती है। इसीलिए भगवान महावीर ने निन्दा को पीठ का मांस खाना' कहा है। तथागत बुद्ध ने इसे मुख से पाप इकट्ठा करना बताया है। आचार्य हेमचन्द्र ने प्रेरणा दी है कि किसी की भी निन्दा न करे और राजा आदि (सत्ताधिकारी, दण्डाधिकारी, धर्माधिकारी) अधिकार सम्पन्न व्यक्तियों की निन्दा तो विशेष रूप से नहीं करनी चाहिए।
व्यावहारिक जीवन में निन्दा शत्रुता बढ़ाने वाली है, जिसकी निन्दा की जायेगी उसे बुरा लगेगा, वह मन में शत्रुता की गांठ बांध लेगा और अवसर पाकर बदला चुकाने से नहीं चूकेगा। प्रसिद्ध कहावत है कि निन्दक का कोई मित्र नहीं होता।
राजा आदि अधिकारी वर्ग तो रुष्ट होकर निन्दक के जीवन को तबाह कर सकते हैं। उसे दण्डित तथा प्रताड़ित भी कर सकते हैं। इसीलिए जैन नीति लेखकों ने सामाजिक व्यक्ति के लिए राजा आदि की निन्दा का विशेष रूप से निषेध किया है।
निन्दा के साथ इसका विरोधी प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है, वह है किसी की झूठी प्रशंसा करना, जो गुण उसमें नहीं है उन्हें भी बताना। इसे आधुनिक भाषा में खुशामद अथवा चापलूसी (flattery) कहा जाता है।
चापलूसी और निन्दा दोनों ही तीखे शस्त्र हैं जो व्यक्ति को बड़ी तेजी से काटते हैं। निन्दा तीखी है, सुनने वाले को बुरी लगती हैं, जबकि चापलूसी मीठी छुरी है, व्यक्ति इसे सुनकर फूला नहीं समाता। किन्तु दोनों ही पतन की राह हैं। इससे निन्दक और चापलूसी करने वाले की आत्मा भी पतित होती है और जिसकी निन्दा तथा चापलूसी की जाती है उसका भी पतन होता है। निन्दा सुनकर क्रोध में भर जाने से और झूठी प्रशंसा सुनकर गर्व में भरकर फूल जाने से।
नैतिक व्यक्ति न किसी अन्य की निन्दा करता है और न झूठी, प्रशंसा ही। यदि वह निन्दा करता भी है तो स्वयं अपनी आत्मा की ही, अनैतिक इच्छाओं और कार्यो के लिए, और इस प्रकार वह आत्म-निन्दा द्वारा नैतिक प्रगति में अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। 1. पिट्ठिमंसं न खाइज्जा।
-दशवैकालिक, 8/47 2. विचिनाति मुखे सो कलि, कलिनातो सुखं न विन्दति -सुत्तनिपात, 3/36/2 3. अवर्णवादो न क्वापि राजादिषु विशेषतः।
-योगशास्त्र, 118