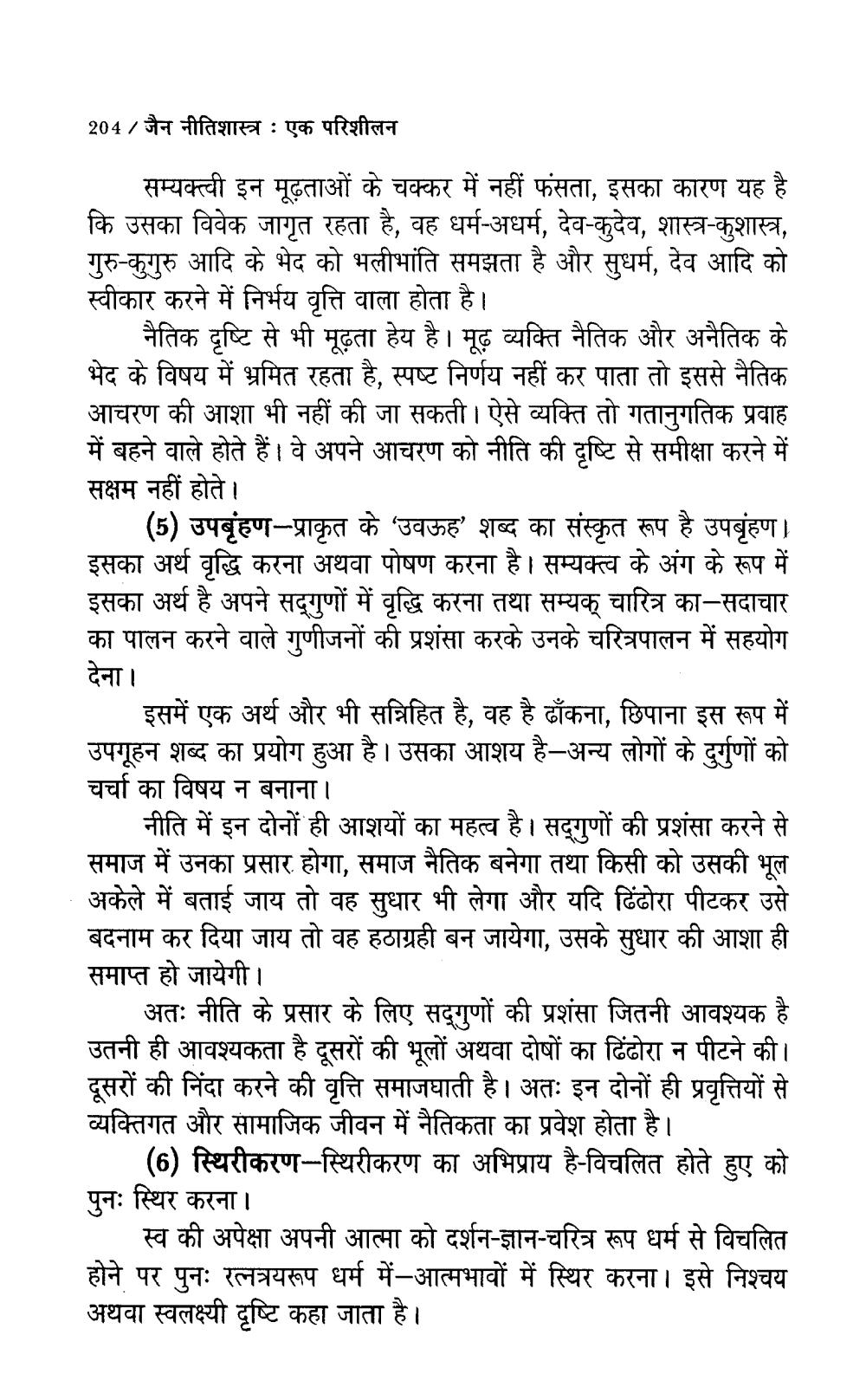________________
204 / जैन नीतिशास्त्र : एक परिशीलन
सम्यक्त्वी इन मूढ़ताओं के चक्कर में नहीं फंसता, इसका कारण यह है कि उसका विवेक जागृत रहता है, वह धर्म-अधर्म, देव-कुदेव, शास्त्र-कुशास्त्र, गुरु-कुगुरु आदि के भेद को भलीभांति समझता है और सुधर्म, देव आदि को स्वीकार करने में निर्भय वृत्ति वाला होता है।
नैतिक दृष्टि से भी मूढ़ता हेय है। मूढ़ व्यक्ति नैतिक और अनैतिक के भेद के विषय में भ्रमित रहता है, स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता तो इससे नैतिक आचरण की आशा भी नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्ति तो गतानुगतिक प्रवाह में बहने वाले होते हैं। वे अपने आचरण को नीति की दृष्टि से समीक्षा करने में सक्षम नहीं होते।
(5) उपबृंहण-प्राकृत के 'उवऊह' शब्द का संस्कृत रूप है उपबृंहण। इसका अर्थ वृद्धि करना अथवा पोषण करना है। सम्यक्त्व के अंग के रूप में इसका अर्थ है अपने सद्गुणों में वृद्धि करना तथा सम्यक् चारित्र का-सदाचार का पालन करने वाले गुणीजनों की प्रशंसा करके उनके चरित्रपालन में सहयोग देना।
इसमें एक अर्थ और भी सन्निहित है, वह है ढाँकना, छिपाना इस रूप में उपगूहन शब्द का प्रयोग हुआ है। उसका आशय है-अन्य लोगों के दुर्गुणों को चर्चा का विषय न बनाना।
नीति में इन दोनों ही आशयों का महत्व है। सदगणों की प्रशंसा करने से समाज में उनका प्रसार होगा, समाज नैतिक बनेगा तथा किसी को उसकी भूल अकेले में बताई जाय तो वह सुधार भी लेगा और यदि ढिंढोरा पीटकर उसे बदनाम कर दिया जाय तो वह हठाग्रही बन जायेगा, उसके सुधार की आशा ही समाप्त हो जायेगी।
अतः नीति के प्रसार के लिए सद्गुणों की प्रशंसा जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यकता है दूसरों की भूलों अथवा दोषों का ढिंढोरा न पीटने की। दूसरों की निंदा करने की वृत्ति समाजघाती है। अतः इन दोनों ही प्रवृत्तियों से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में नैतिकता का प्रवेश होता है।
(6) स्थिरीकरण-स्थिरीकरण का अभिप्राय है-विचलित होते हुए को पुनः स्थिर करना।
स्व की अपेक्षा अपनी आत्मा को दर्शन-ज्ञान-चरित्र रूप धर्म से विचलित होने पर पुनः रत्नत्रयरूप धर्म में-आत्मभावों में स्थिर करना। इसे निश्चय अथवा स्वलक्ष्यी दृष्टि कहा जाता है।