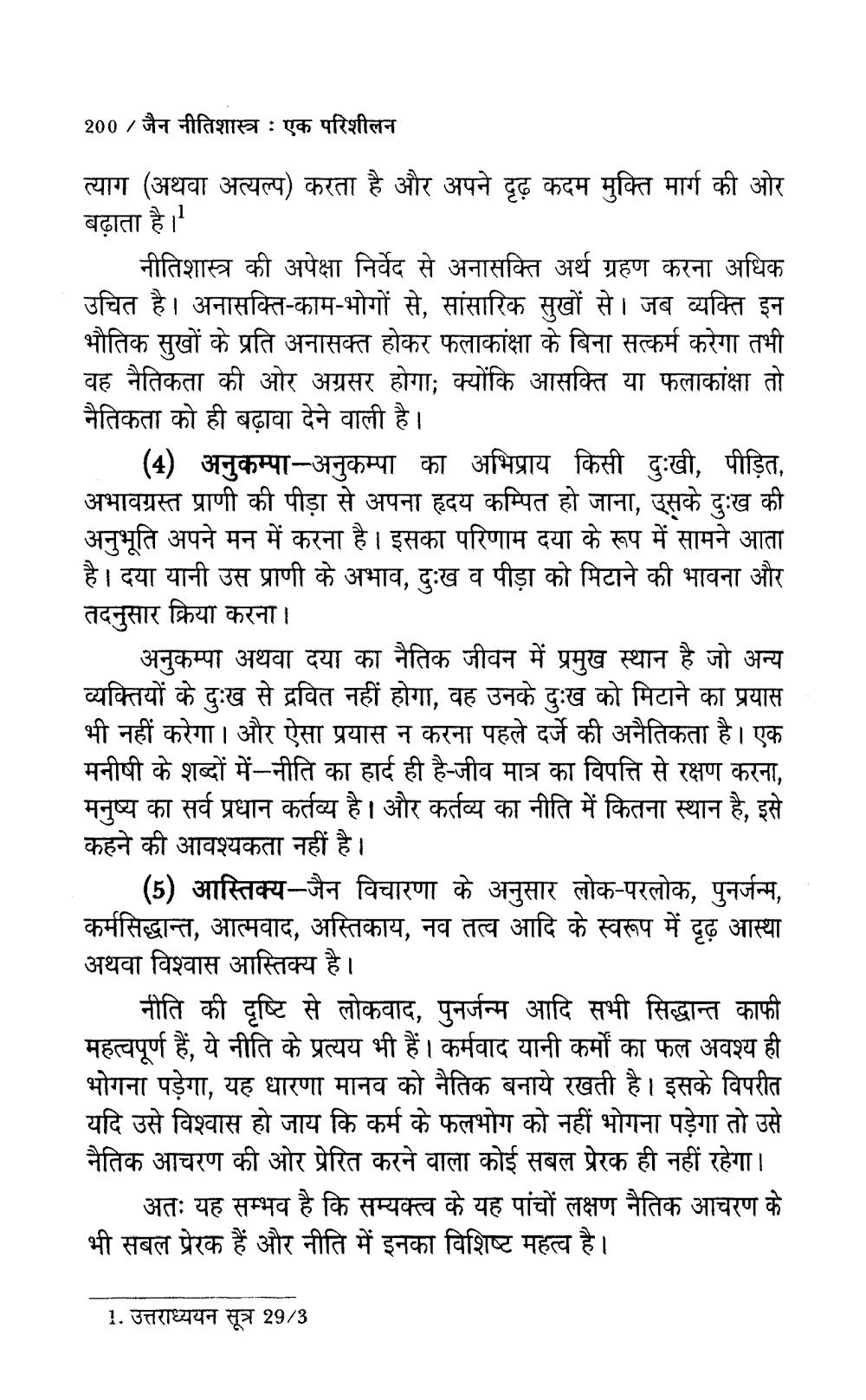________________
200 / जैन नीतिशास्त्र : एक परिशीलन
त्याग (अथवा अत्यल्प) करता है और अपने दृढ़ कदम मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ाता है । '
नीतिशास्त्र की अपेक्षा निर्वेद से अनासक्ति अर्थ ग्रहण करना अधिक उचित है । अनासक्ति-काम- म-भोगों से, सांसारिक सुखों से। जब व्यक्ति इन भौतिक सुखों के प्रति अनासक्त होकर फलाकांक्षा के बिना सत्कर्म करेगा तभी वह नैतिकता की ओर अग्रसर होगा; क्योंकि आसक्ति या फलाकांक्षा तो नैतिकता को ही बढ़ावा देने वाली है ।
(4) अनुकम्पा - अनुकम्पा का अभिप्राय किसी दुःखी, पीड़ित, अभावग्रस्त प्राणी की पीड़ा से अपना हृदय कम्पित हो जाना, उसके दुःख की अनुभूति अपने मन में करना है । इसका परिणाम दया के रूप में सामने आता है । दया यानी उस प्राणी के अभाव, दुःख व पीड़ा को मिटाने की भावना और तदनुसार क्रिया करना ।
अनुकम्पा अथवा दया का नैतिक जीवन में प्रमुख स्थान है जो अन्य व्यक्तियों के दुःख से द्रवित नहीं होगा, वह उनके दुःख को मिटाने का प्रयास भी नहीं करेगा । और ऐसा प्रयास न करना पहले दर्जे की अनैतिकता है । एक मनीषी के शब्दों में- नीति का हार्द ही है - जीव मात्र का विपत्ति से रक्षण करना, मनुष्य का सर्व प्रधान कर्तव्य है । और कर्तव्य का नीति में कितना स्थान है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है
1
( 5 ) आस्तिक्य - जैन विचारणा के अनुसार लोक-परलोक, पुनर्जन्म, कर्मसिद्धान्त, आत्मवाद, अस्तिकाय, नव तत्व आदि के स्वरूप में दृढ़ आस्था अथवा विश्वास आस्तिक्य है ।
नीति की दृष्टि से लोकवाद, पुनर्जन्म आदि सभी सिद्धान्त काफी महत्वपूर्ण हैं, ये नीति के प्रत्यय भी हैं । कर्मवाद यानी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा, यह धारणा मानव को नैतिक बनाये रखती है । इसके विपरीत यदि उसे विश्वास हो जाय कि कर्म के फलभोग को नहीं भोगना पड़ेगा तो उसे नैतिक आचरण की ओर प्रेरित करने वाला कोई सबल प्रेरक ही नहीं रहेगा ।
अतः यह सम्भव है कि सम्यक्त्व के यह पांचों लक्षण नैतिक आचरण के भी सबल प्रेरक हैं और नीति में इनका विशिष्ट महत्व है ।
1. उत्तराध्ययन सूत्र 29 / 3