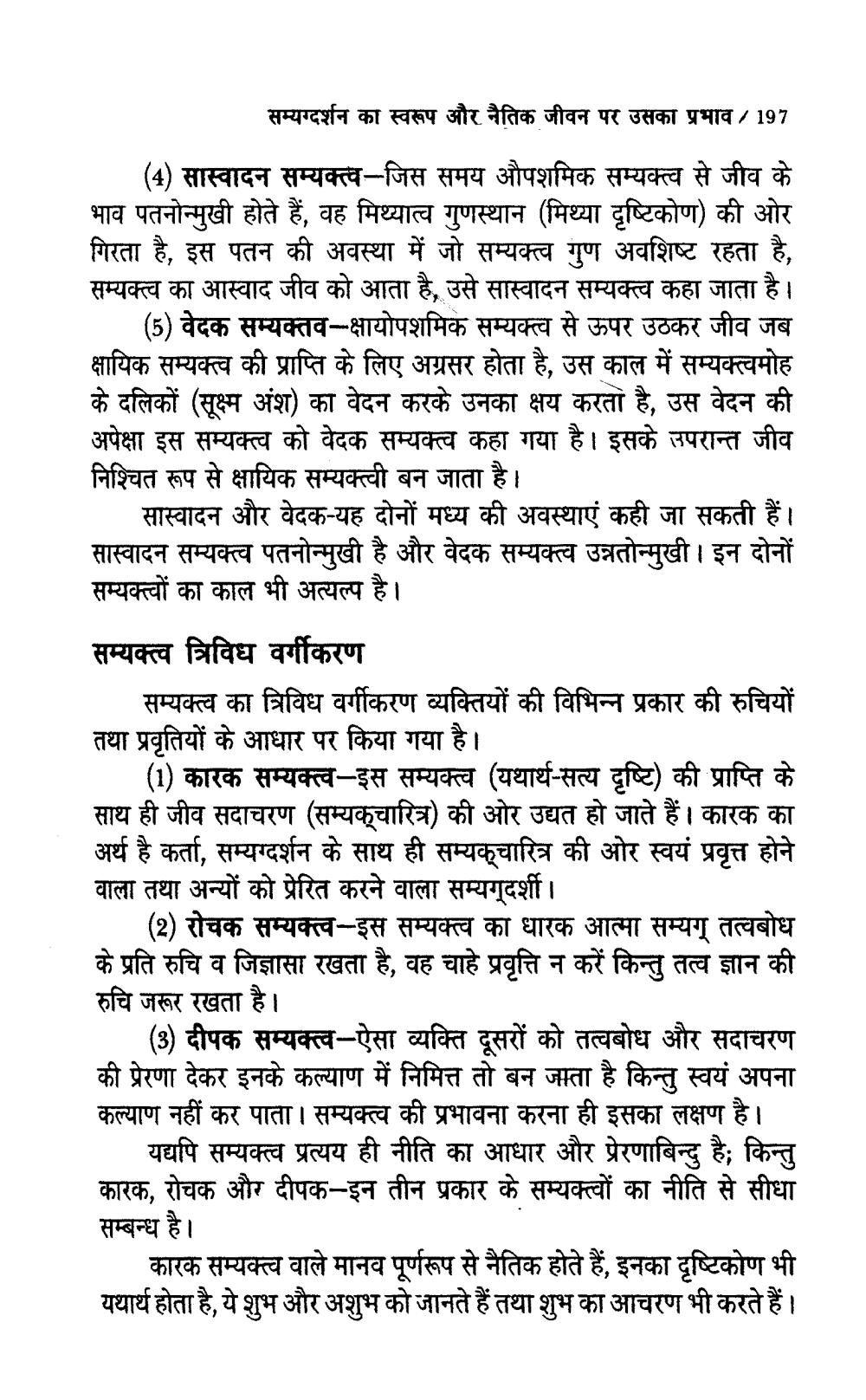________________
सम्यग्दर्शन का स्वरूप और नैतिक जीवन पर उसका प्रभाव / 197
(4) सास्वादन सम्यक्त्व-जिस समय औपशमिक सम्यक्त्व से जीव के भाव पतनोन्मुखी होते हैं, वह मिथ्यात्व गुणस्थान (मिथ्या दृष्टिकोण) की ओर गिरता है, इस पतन की अवस्था में जो सम्यक्त्व गुण अवशिष्ट रहता है, सम्यक्त्व का आस्वाद जीव को आता है, उसे सास्वादन सम्यक्त्व कहा जाता है।
(5) वेदक सम्यक्तव-क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से ऊपर उठकर जीव जब क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है, उस काल में सम्यक्त्वमोह के दलिकों (सूक्ष्म अंश) का वेदन करके उनका क्षय करता है, उस वेदन की अपेक्षा इस सम्यक्त्व को वेदक सम्यक्त्व कहा गया है। इसके उपरान्त जीव निश्चित रूप से क्षायिक सम्यक्त्वी बन जाता है।
सास्वादन और वेदक-यह दोनों मध्य की अवस्थाएं कही जा सकती हैं। सास्वादन सम्यक्त्व पतनोन्मुखी है और वेदक सम्यक्त्व उन्नतोन्मुखी। इन दोनों सम्यक्त्वों का काल भी अत्यल्प है।
सम्यक्त्व त्रिविध वर्गीकरण
सम्यक्त्व का त्रिविध वर्गीकरण व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की रुचियों तथा प्रवृतियों के आधार पर किया गया है।
(1) कारक सम्यक्त्व-इस सम्यक्त्व (यथार्थ-सत्य दृष्टि) की प्राप्ति के साथ ही जीव सदाचरण (सम्यक्चारित्र) की ओर उद्यत हो जाते हैं। कारक का अर्थ है कर्ता, सम्यग्दर्शन के साथ ही सम्यक्चारित्र की ओर स्वयं प्रवृत्त होने वाला तथा अन्यों को प्रेरित करने वाला सम्यग्दर्शी।
(2) रोचक सम्यक्त्व-इस सम्यक्त्व का धारक आत्मा सम्यग् तत्वबोध के प्रति रुचि व जिज्ञासा रखता है, वह चाहे प्रवृत्ति न करें किन्तु तत्व ज्ञान की रुचि जरूर रखता है।
(3) दीपक सम्यक्त्व-ऐसा व्यक्ति दूसरों को तत्वबोध और सदाचरण की प्रेरणा देकर इनके कल्याण में निमित्त तो बन जाता है किन्तु स्वयं अपना कल्याण नहीं कर पाता। सम्यक्त्व की प्रभावना करना ही इसका लक्षण है।
यद्यपि सम्यक्त्व प्रत्यय ही नीति का आधार और प्रेरणाबिन्दु है; किन्तु कारक, रोचक और दीपक-इन तीन प्रकार के सम्यक्त्वों का नीति से सीधा सम्बन्ध है।
कारक सम्यक्त्व वाले मानव पूर्णरूप से नैतिक होते हैं, इनका दृष्टिकोण भी यथार्थ होता है, ये शुभ और अशुभ को जानते हैं तथा शुभ का आचरण भी करते हैं।