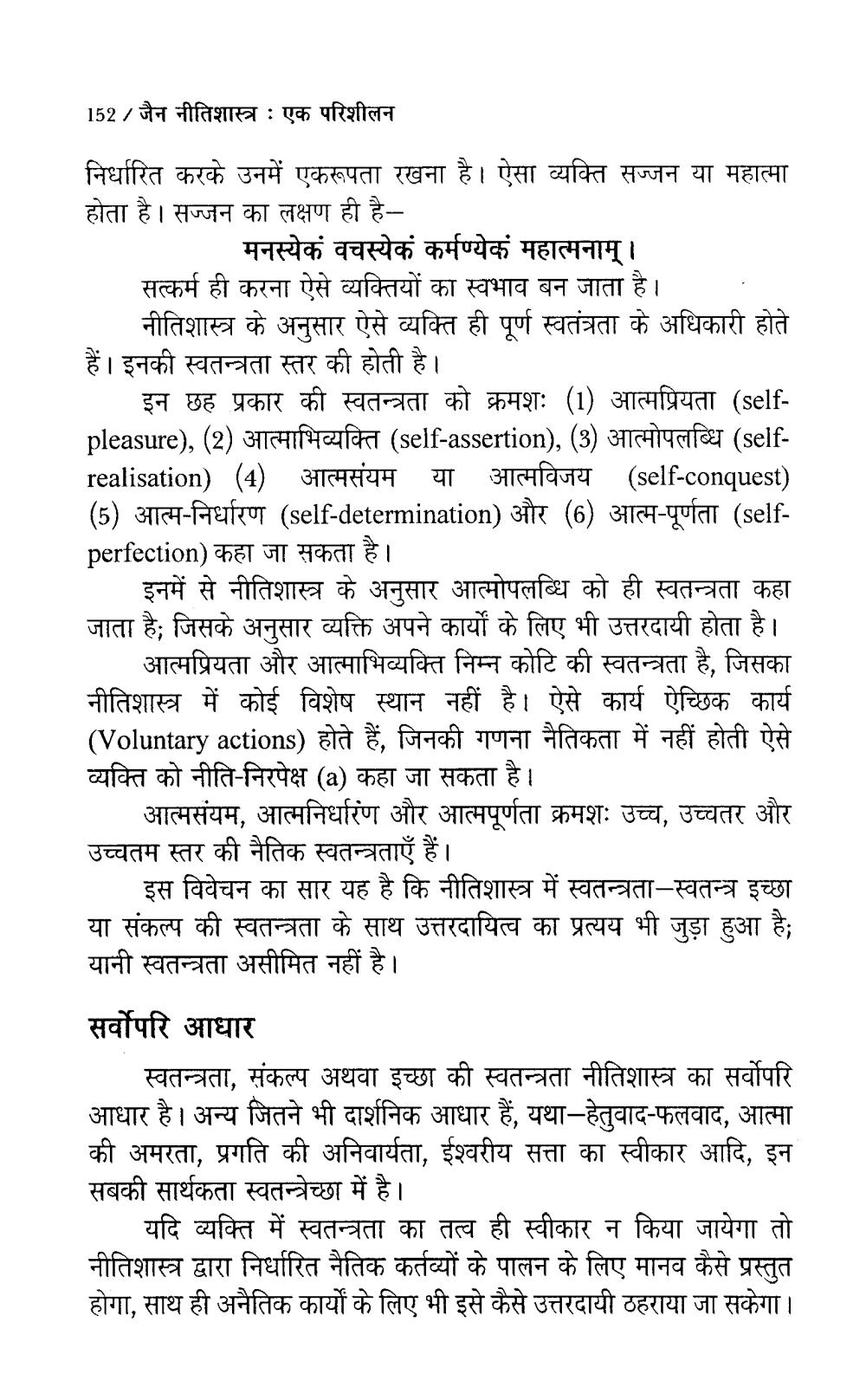________________
152 / जैन नीतिशास्त्र : एक परिशीलन
निर्धारित करके उनमें एकरूपता रखना है। ऐसा व्यक्ति सज्जन या महात्मा होता है। सज्जन का लक्षण ही है
मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्।। सत्कर्म ही करना ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव बन जाता है।
नीतिशास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति ही पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकारी होते हैं। इनकी स्वतन्त्रता स्तर की होती है।
इन छह प्रकार की स्वतन्त्रता को क्रमशः (1) आत्मप्रियता (selfpleasure), (2) आत्माभिव्यक्ति (self-assertion), (3) आत्मोपलब्धि (selfrealisation) (4) आत्मसंयम या आत्मविजय (self-conquest) (5) आत्म-निर्धारण (self-determination) और (6) आत्म-पूर्णता (selfperfection) कहा जा सकता है।
इनमें से नीतिशास्त्र के अनुसार आत्मोपलब्धि को ही स्वतन्त्रता कहा जाता है; जिसके अनुसार व्यक्ति अपने कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होता है।
आत्मप्रियता और आत्माभिव्यक्ति निम्न कोटि की स्वतन्त्रता है, जिसका नीतिशास्त्र में कोई विशेष स्थान नहीं है। ऐसे कार्य ऐच्छिक कार्य (Voluntary actions) होते हैं, जिनकी गणना नैतिकता में नहीं होती ऐसे व्यक्ति को नीति-निरपेक्ष (a) कहा जा सकता है।
आत्मसंयम, आत्मनिर्धारण और आत्मपूर्णता क्रमशः उच्च, उच्चतर और उच्चतम स्तर की नैतिक स्वतन्त्रताएँ हैं।
इस विवेचन का सार यह है कि नीतिशास्त्र में स्वतन्त्रता-स्वतन्त्र इच्छा या संकल्प की स्वतन्त्रता के साथ उत्तरदायित्व का प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है; यानी स्वतन्त्रता असीमित नहीं है।
सर्वोपरि आधार
स्वतन्त्रता, संकल्प अथवा इच्छा की स्वतन्त्रता नीतिशास्त्र का सर्वोपरि आधार है। अन्य जितने भी दार्शनिक आधार हैं, यथा-हेतुवाद-फलवाद, आत्मा की अमरता, प्रगति की अनिवार्यता, ईश्वरीय सत्ता का स्वीकार आदि, इन सबकी सार्थकता स्वतन्त्रेच्छा में है।
यदि व्यक्ति में स्वतन्त्रता का तत्व ही स्वीकार न किया जायेगा तो नीतिशास्त्र द्वारा निर्धारित नैतिक कर्तव्यों के पालन के लिए मानव कैसे प्रस्तुत होगा, साथ ही अनैतिक कार्यों के लिए भी इसे कैसे उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा।