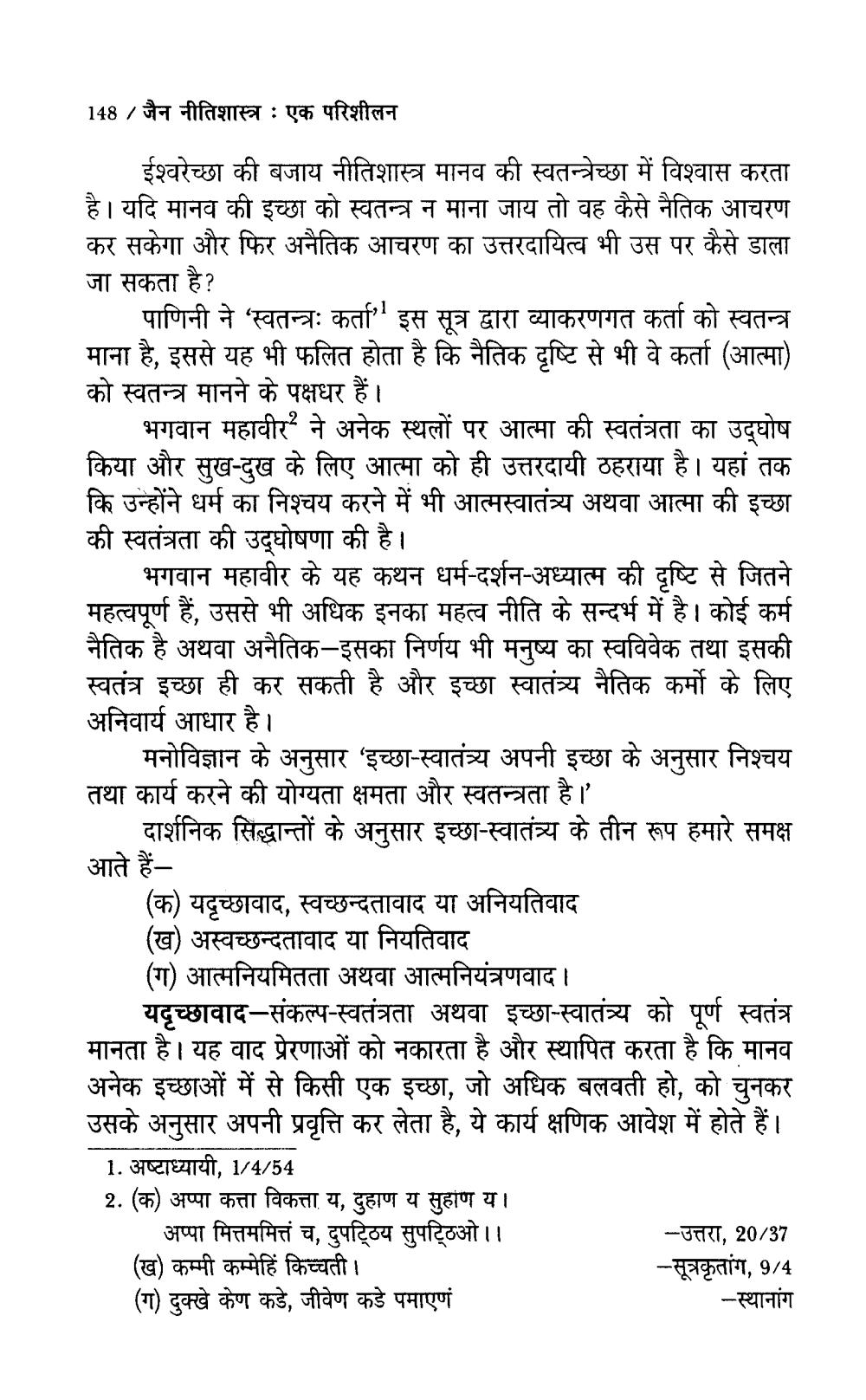________________
148 / जैन नीतिशास्त्र : एक परिशीलन
ईश्वरेच्छा की बजाय नीतिशास्त्र मानव की स्वतन्त्रेच्छा में विश्वास करता है । यदि मानव की इच्छा को स्वतन्त्र न माना जाय तो वह कैसे नैतिक आचरण कर सकेगा और फिर अनैतिक आचरण का उत्तरदायित्व भी उस पर कैसे डाला जा सकता है?
पाणिनी ने ‘स्वतन्त्रः कर्ता"" इस सूत्र द्वारा व्याकरणगत कर्ता को स्वतन्त्र माना है, इससे यह भी फलित होता है कि नैतिक दृष्टि से भी वे कर्ता (आत्मा) को स्वतन्त्र मानने के पक्षधर हैं ।
भगवान महावीर' ने अनेक स्थलों पर आत्मा की स्वतंत्रता का उद्घोष किया और सुख-दुख के लिए आत्मा को ही उत्तरदायी ठहराया है। यहां तक कि उन्होंने धर्म का निश्चय करने में भी आत्मस्वातंत्र्य अथवा आत्मा की इच्छा की स्वतंत्रता की उद्घोषणा की है।
भगवान महावीर के यह कथन धर्म-दर्शन - अध्यात्म की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण हैं, उससे भी अधिक इनका महत्व नीति के सन्दर्भ में है । कोई कर्म नैतिक है अथवा अनैतिक - इसका निर्णय भी मनुष्य का स्वविवेक तथा इसकी स्वतंत्र इच्छा ही कर सकती है और इच्छा स्वातंत्र्य नैतिक कर्मो के लिए अनिवार्य आधार है 1
मनोविज्ञान के अनुसार 'इच्छा - स्वातंत्र्य अपनी इच्छा के अनुसार निश्चय तथा कार्य करने की योग्यता क्षमता और स्वतन्त्रता है ।'
दार्शनिक सिद्धान्तों के अनुसार इच्छा स्वातंत्र्य के तीन रूप हमारे समक्ष आते हैं
(क) यदृच्छावाद, स्वच्छन्दतावाद या अनियतिवाद (ख) अस्वच्छन्दतावाद या नियतिवाद
(ग) आत्मनियमितता अथवा आत्मनियंत्रणवाद ।
यदृच्छावाद - संकल्प - स्वतंत्रता अथवा इच्छा - स्वातंत्र्य को पूर्ण स्वतंत्र माता है | यह वाद प्रेरणाओं को नकारता है और स्थापित करता है कि मानव अनेक इच्छाओं में से किसी एक इच्छा, जो अधिक बलवती हो, को चुनकर उसके अनुसार अपनी प्रवृत्ति कर लेता है, ये कार्य क्षणिक आवेश में होते हैं ।
1. अष्टाध्यायी, 1/4/54
2. (क) अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।
अप्पा मित्तममित्तं च, दुपट्ठिय सुपट्ठिओ ।।
(ख) कम्मी कम्मेहिं किच्चती ।
(ग) दुक्खे केण कडे, जीवेण कडे पमाएणं
-उत्तरा, 20/37
-सूत्रकृतांग, 9/4 - स्थानांग