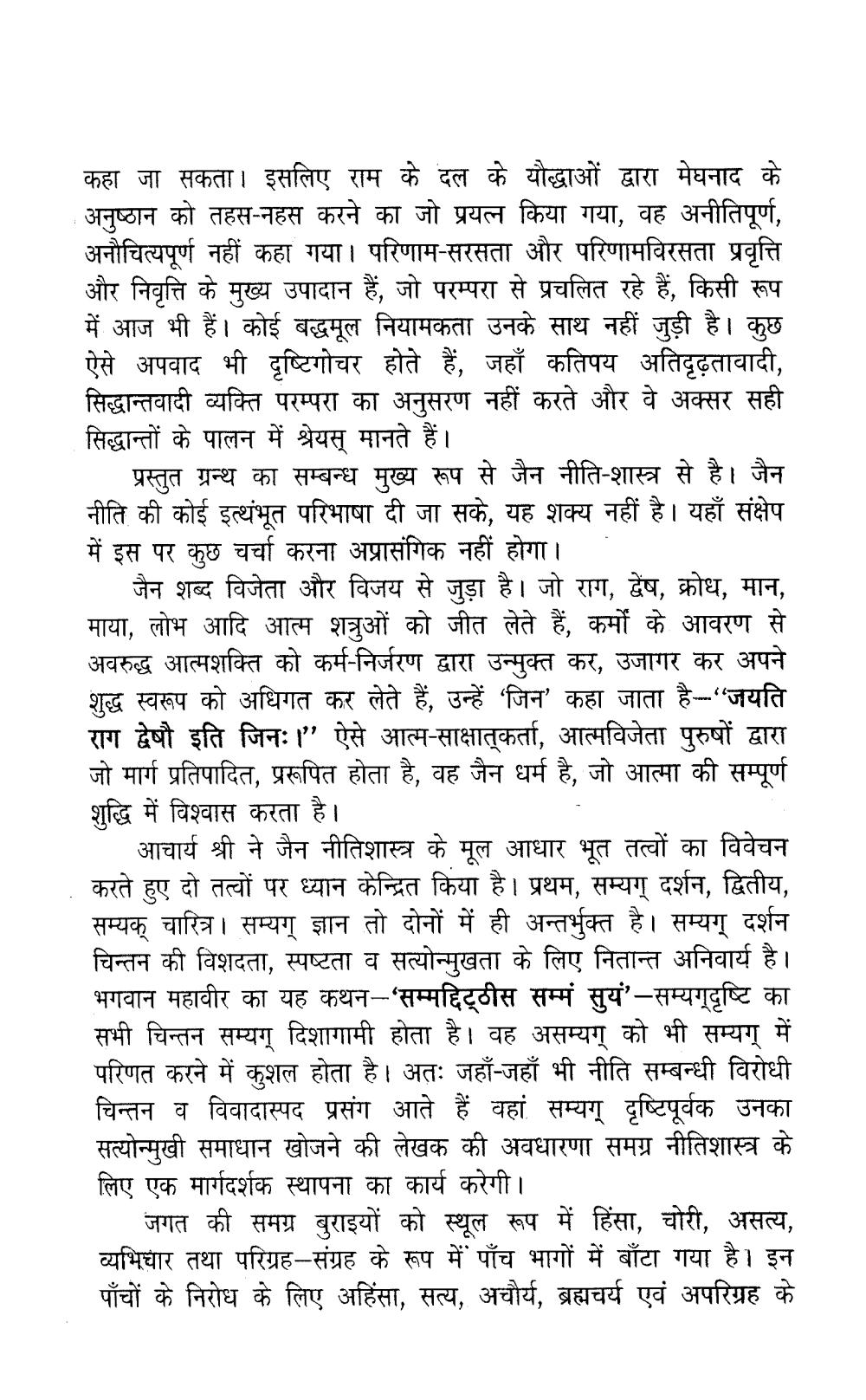________________
कहा जा सकता। इसलिए राम के दल के यौद्धाओं द्वारा मेघनाद के अनुष्ठान को तहस-नहस करने का जो प्रयत्न किया गया, वह अनीतिपूर्ण, अनौचित्यपूर्ण नहीं कहा गया। परिणाम-सरसता और परिणामविरसता प्रवृत्ति और निवृत्ति के मुख्य उपादान हैं, जो परम्परा से प्रचलित रहे हैं, किसी रूप में आज भी हैं। कोई बद्धमूल नियामकता उनके साथ नहीं जड़ी है। कुछ ऐसे अपवाद भी दृष्टिगोचर होते हैं, जहाँ कतिपय अतिदृढ़तावादी, सिद्धान्तवादी व्यक्ति परम्परा का अनुसरण नहीं करते और वे अक्सर सही सिद्धान्तों के पालन में श्रेयस् मानते हैं।
प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्बन्ध मुख्य रूप से जैन नीति-शास्त्र से है। जैन नीति की कोई इत्थंभूत परिभाषा दी जा सके, यह शक्य नहीं है। यहाँ संक्षेप में इस पर कुछ चर्चा करना अप्रासंगिक नहीं होगा।
जैन शब्द विजेता और विजय से जुड़ा है। जो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आत्म शत्रुओं को जीत लेते हैं, कर्मों के आवरण से अवरुद्ध आत्मशक्ति को कर्म-निर्जरण द्वारा उन्मुक्त कर, उजागर कर अपने शुद्ध स्वरूप को अधिगत कर लेते हैं, उन्हें 'जिन' कहा जाता है-“जयति राग द्वेषौ इति जिनः।" ऐसे आत्म-साक्षात्कर्ता, आत्मविजेता पुरुषों द्वारा जो मार्ग प्रतिपादित, प्ररूपित होता है, वह जैन धर्म है, जो आत्मा की सम्पूर्ण शुद्धि में विश्वास करता है। __आचार्य श्री ने जैन नीतिशास्त्र के मूल आधार भूत तत्वों का विवेचन करते हुए दो तत्वों पर ध्यान केन्द्रित किया है। प्रथम, सम्यग् दर्शन, द्वितीय, सम्यक् चारित्र। सम्यग् ज्ञान तो दोनों में ही अन्तर्भुक्त है। सम्यग् दर्शन चिन्तन की विशदता, स्पष्टता व सत्योन्मुखता के लिए नितान्त अनिवार्य है। भगवान महावीर का यह कथन-'सम्मद्दिट्ठीस सम्मं सुयं'-सम्यग्दृष्टि का सभी चिन्तन सम्यग् दिशागामी होता है। वह असम्यग् को भी सम्यग् में परिणत करने में कुशल होता है। अतः जहाँ-जहाँ भी नीति सम्बन्धी विरोधी चिन्तन व विवादास्पद प्रसंग आते हैं वहां सम्यग् दृष्टिपूर्वक उनका सत्योन्मुखी समाधान खोजने की लेखक की अवधारणा समग्र नीतिशास्त्र के लिए एक मार्गदर्शक स्थापना का कार्य करेगी। ___ जगत की समग्र बुराइयों को स्थूल रूप में हिंसा, चोरी, असत्य, व्यभिचार तथा परिग्रह-संग्रह के रूप में पाँच भागों में बाँटा गया है। इन पाँचों के निरोध के लिए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह के