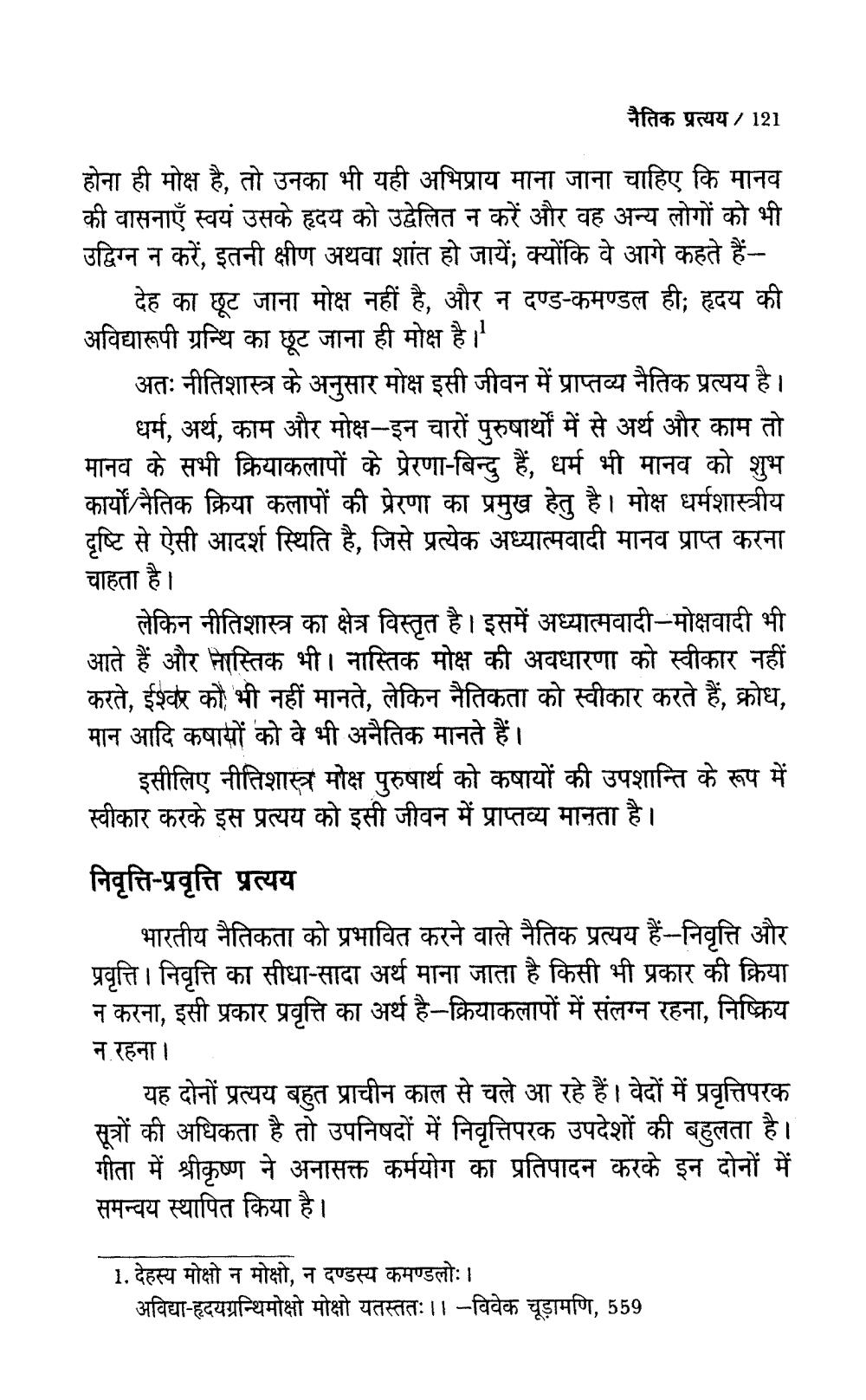________________
नैतिक प्रत्यय / 121
होना ही मोक्ष है, तो उनका भी यही अभिप्राय माना जाना चाहिए कि मानव की वासनाएँ स्वयं उसके हृदय को उद्वेलित न करें और वह अन्य लोगों को भी उद्विग्न न करें, इतनी क्षीण अथवा शांत हो जायें; क्योंकि वे आगे कहते हैं
देह का छूट जाना मोक्ष नहीं है, और न दण्ड-कमण्डल ही; हृदय की अविद्यारूपी ग्रन्थि का छूट जाना ही मोक्ष है।'
अतः नीतिशास्त्र के अनुसार मोक्ष इसी जीवन में प्राप्तव्य नैतिक प्रत्यय है।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थों में से अर्थ और काम तो मानव के सभी क्रियाकलापों के प्रेरणा-बिन्दु हैं, धर्म भी मानव को शुभ कार्यों/नैतिक क्रिया कलापों की प्रेरणा का प्रमुख हेतु है। मोक्ष धर्मशास्त्रीय दृष्टि से ऐसी आदर्श स्थिति है, जिसे प्रत्येक अध्यात्मवादी मानव प्राप्त करना चाहता है।
लेकिन नीतिशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत है। इसमें अध्यात्मवादी-मोक्षवादी भी आते हैं और नास्तिक भी। नास्तिक मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर को भी नहीं मानते, लेकिन नैतिकता को स्वीकार करते हैं, क्रोध, मान आदि कषायों को वे भी अनैतिक मानते हैं। ___ इसीलिए नीतिशास्त्र मोक्ष पुरुषार्थ को कषायों की उपशान्ति के रूप में स्वीकार करके इस प्रत्यय को इसी जीवन में प्राप्तव्य मानता है।
निवृत्ति-प्रवृत्ति प्रत्यय ___ भारतीय नैतिकता को प्रभावित करने वाले नैतिक प्रत्यय हैं-निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति का सीधा-सादा अर्थ माना जाता है किसी भी प्रकार की क्रिया न करना, इसी प्रकार प्रवृत्ति का अर्थ है-क्रियाकलापों में संलग्न रहना, निष्क्रिय न रहना।
यह दोनों प्रत्यय बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। वेदों में प्रवृत्तिपरक सूत्रों की अधिकता है तो उपनिषदों में निवृत्तिपरक उपदेशों की बहुलता है। गीता में श्रीकृष्ण ने अनासक्त कर्मयोग का प्रतिपादन करके इन दोनों में समन्वय स्थापित किया है।
1. देहस्य मोक्षो न मोक्षो, न दण्डस्य कमण्डलोः ।
अविद्या-हृदयग्रन्थिमोक्षो मोक्षो यतस्ततः ।। -विवेक चूड़ामणि, 559