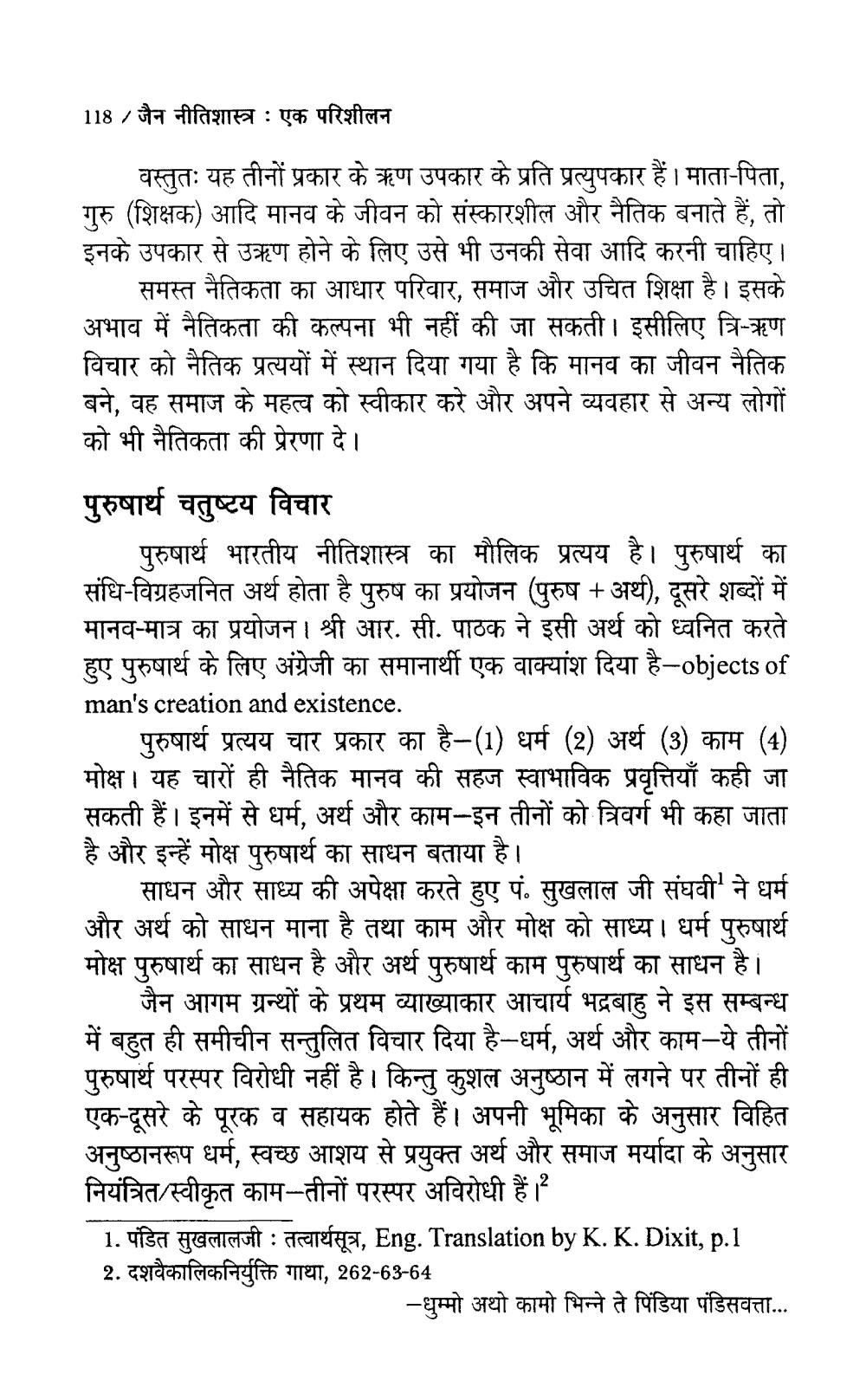________________
118 / जैन नीतिशास्त्र : एक परिशीलन
वस्तुतः यह तीनों प्रकार के ऋण उपकार के प्रति प्रत्युपकार हैं। माता-पिता, गुरु (शिक्षक) आदि मानव के जीवन को संस्कारशील और नैतिक बनाते हैं, तो इनके उपकार से उऋण होने के लिए उसे भी उनकी सेवा आदि करनी चाहिए।
समस्त नैतिकता का आधार परिवार, समाज और उचित शिक्षा है। इसके अभाव में नैतिकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए त्रि-ऋण विचार को नैतिक प्रत्ययों में स्थान दिया गया है कि मानव का जीवन नैतिक बने, वह समाज के महत्व को स्वीकार करे और अपने व्यवहार से अन्य लोगों को भी नैतिकता की प्रेरणा दे।
पुरुषार्थ चतुष्टय विचार
पुरुषार्थ भारतीय नीतिशास्त्र का मौलिक प्रत्यय है। पुरुषार्थ का संधि-विग्रहजनित अर्थ होता है पुरुष का प्रयोजन (पुरुष + अथ), दूसरे शब्दों में मानव-मात्र का प्रयोजन। श्री आर. सी. पाठक ने इसी अर्थ को ध्वनित करते हुए पुरुषार्थ के लिए अंग्रेजी का समानार्थी एक वाक्यांश दिया है-objects of man's creation and existence.
पुरुषार्थ प्रत्यय चार प्रकार का है-(1) धर्म (2) अर्थ (3) काम (4) मोक्ष। यह चारों ही नैतिक मानव की सहज स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ कही जा सकती हैं। इनमें से धर्म, अर्थ और काम-इन तीनों को त्रिवर्ग भी कहा जाता है और इन्हें मोक्ष पुरुषार्थ का साधन बताया है।
साधन और साध्य की अपेक्षा करते हुए पं. सुखलाल जी संघवी ने धर्म और अर्थ को साधन माना है तथा काम और मोक्ष को साध्य। धर्म पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ का साधन है और अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ का साधन है।
जैन आगम ग्रन्थों के प्रथम व्याख्याकार आचार्य भद्रबाहु ने इस सम्बन्ध में बहुत ही समीचीन सन्तुलित विचार दिया है-धर्म, अर्थ और काम-ये तीनों पुरुषार्थ परस्पर विरोधी नहीं है। किन्तु कुशल अनुष्ठान में लगने पर तीनों ही एक-दूसरे के पूरक व सहायक होते हैं। अपनी भूमिका के अनुसार विहित अनुष्ठानरूप धर्म, स्वच्छ आशय से प्रयुक्त अर्थ और समाज मर्यादा के अनुसार नियंत्रित/स्वीकृत काम-तीनों परस्पर अविरोधी हैं।' 1. पंडित सुखलालजी : तत्वार्थसूत्र, Eng. Translation by K. K. Dixit, p.1 2. दशवैकालिकनियुक्ति गाथा, 262-63-64
-धुम्मो अथो कामो भिन्ने ते पिंडिया पंडिसवत्ता...