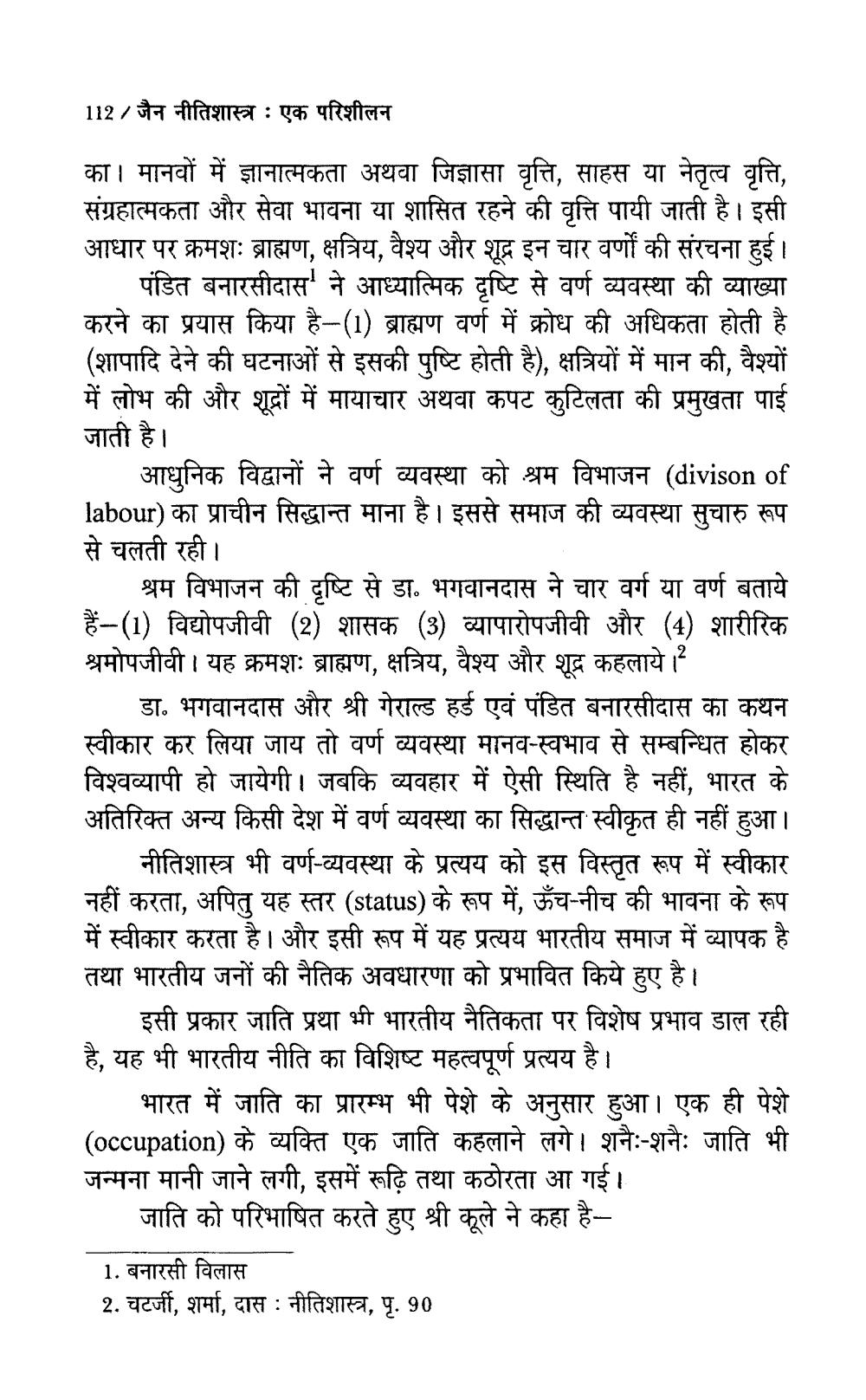________________
112 / जैन नीतिशास्त्र : एक परिशीलन
का। मानवों में ज्ञानात्मकता अथवा जिज्ञासा वृत्ति, साहस या नेतृत्व वृत्ति, संग्रहात्मकता और सेवा भावना या शासित रहने की वृत्ति पायी जाती है । इसी आधार पर क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों की संरचना हुई ।
पंडित बनारसीदास' ने आध्यात्मिक दृष्टि से वर्ण व्यवस्था की व्याख्या करने का प्रयास किया है - (1) ब्राह्मण वर्ण में क्रोध की अधिकता होती है (शापादि देने की घटनाओं से इसकी पुष्टि होती है), क्षत्रियों में मान की, वैश्यों में लोभ की और शूद्रों में मायाचार अथवा कपट कुटिलता की प्रमुखता पाई जाती है। आधुनिक विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था को श्रम विभाजन (divison of labour) का प्राचीन सिद्धान्त माना है । इससे समाज की व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रही ।
श्रम विभाजन की दृष्टि से डा. भगवानदास ने चार वर्ग या वर्ण बताये हैं- (1) विद्योपजीवी (2) शासक ( 3 ) व्यापारोपजीवी और (1) शारीरिक श्रमोपजीवी । यह क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाये ।
1
डा. भगवानदास और श्री गेराल्ड हर्ड एवं पंडित बनारसीदास का कथन स्वीकार कर लिया जाय तो वर्ण व्यवस्था मानव स्वभाव से सम्बन्धित होकर विश्वव्यापी हो जायेगी। जबकि व्यवहार में ऐसी स्थिति है नहीं, भारत के अतिरिक्त अन्य किसी देश में वर्ण व्यवस्था का सिद्धान्त स्वीकृत ही नहीं हुआ ।
नीतिशास्त्र भी वर्ण-व्यवस्था के प्रत्यय को इस विस्तृत रूप में स्वीकार नहीं करता, अपितु यह स्तर (status) के रूप में, ऊँच-नीच की भावना के रूप में स्वीकार करता है । और इसी रूप में यह प्रत्यय भारतीय समाज में व्यापक है तथा भारतीय जनों की नैतिक अवधारणा को प्रभावित किये हुए है ।
इसी प्रकार जाति प्रथा भी भारतीय नैतिकता पर विशेष प्रभाव डाल रही है, यह भी भारतीय नीति का विशिष्ट महत्वपूर्ण प्रत्यय है ।
भारत में जाति का प्रारम्भ भी पेशे के अनुसार हुआ। एक ही पेशे ( occupation) के व्यक्ति एक जाति कहलाने लगे । शनैः-शनैः जाति भी जन्मना मानी जाने लगी, इसमें रूढ़ि तथा कठोरता आ गई ।
जाति को परिभाषित करते हुए श्री कूले ने कहा है
-
1. बनारसी विलास
2. चटर्जी, शर्मा, दास : नीतिशास्त्र, पृ. 90