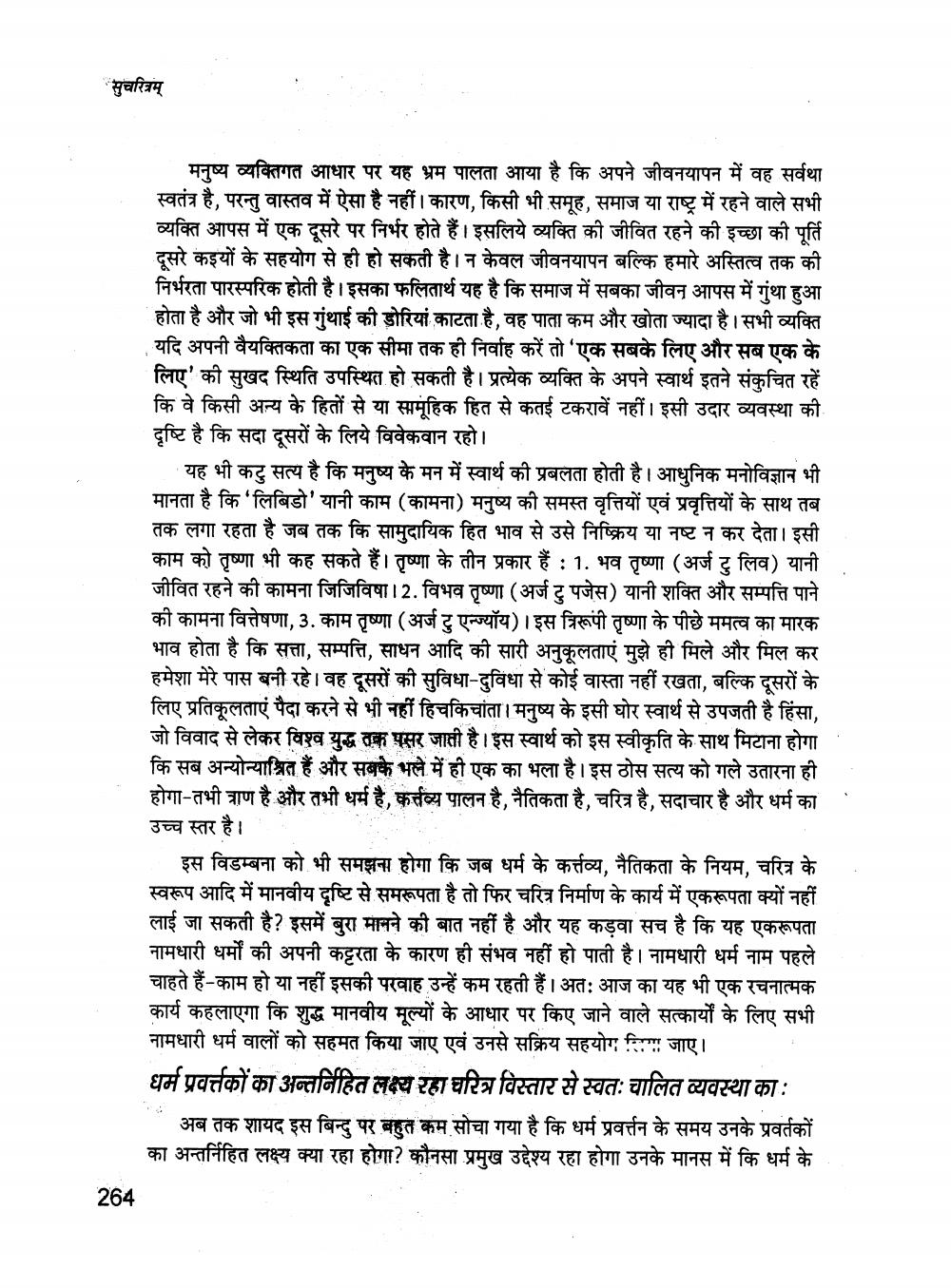________________
सुचरित्रम्
264
मनुष्य व्यक्तिगत आधार पर यह भ्रम पालता आया है कि अपने जीवनयापन में वह सर्वथा स्वतंत्र है, परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं । कारण, किसी भी समूह, समाज या राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसलिये व्यक्ति की जीवित रहने की इच्छा की पूर्ति दूसरे कइयों के सहयोग से ही हो सकती है। न केवल जीवनयापन बल्कि हमारे अस्तित्व तक की निर्भरता पारस्परिक होती है। इसका फलितार्थ यह है कि समाज में सबका जीवन आपस में गुंथा हुआ होता है और जो भी इस गुंथाई की डोरियां काटता है, वह पाता कम और खोता ज्यादा है। सभी व्यक्ति यदि अपनी वैयक्तिकता का एक सीमा तक ही निर्वाह करें तो 'एक सबके लिए और सब एक के लिए' की सुखद स्थिति उपस्थित हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वार्थ इतने संकुचित रहें कि वे किसी अन्य के हितों से या सामूहिक हित से कतई टकरावें नहीं । इसी उदार व्यवस्था की दृष्टि है कि सदा दूसरों के लिये विवेकवान रहो ।
यह भी कटु सत्य है कि मनुष्य के मन में स्वार्थ की प्रबलता होती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि 'लिबिडो' यानी काम (कामना) मनुष्य की समस्त वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों के साथ तब तक लगा रहता है जब तक कि सामुदायिक हित भाव से उसे निष्क्रिय या नष्ट न कर देता। इसी काम को तृष्णा भी कह सकते हैं। तृष्णा के तीन प्रकार हैं: 1. भव तृष्णा ( अर्ज टु लिव) यानी जीवित रहने की कामना जिजिविषा । 2. विभव तृष्णा (अर्ज टु पजेस) यानी शक्ति और सम्पत्ति पाने की कामना वित्तेषणा, 3. काम तृष्णा ( अर्ज टु एन्ज्यॉय) । इस त्रिरूपी तृष्णा के पीछे ममत्व का मारक भाव होता है कि सत्ता, सम्पत्ति, साधन आदि की सारी अनुकूलताएं मुझे ही मिले और मिल कर हमेशा मेरे पास बनी रहे। वह दूसरों की सुविधा दुविधा से कोई वास्ता नहीं रखता, बल्कि दूसरों के लिए प्रतिकूलताएं पैदा करने से भी नहीं हिचकिचांता । मनुष्य के इसी घोर स्वार्थ से उपजती है हिंसा, जो विवाद से लेकर विश्व युद्ध तक पसर जाती है। इस स्वार्थ को इस स्वीकृति के साथ मिटाना होगा कि सब अन्योन्याश्रित हैं और सबके भले में ही एक का भला है। इस ठोस सत्य को गले उतारना ही होगा तभी त्राण है और तभी धर्म है, कर्तव्य पालन है, नैतिकता है, चरित्र है, सदाचार है और धर्म का उच्च स्तर है।
इस विडम्बना को भी समझना होगा कि जब धर्म के कर्त्तव्य, नैतिकता के नियम, चरित्र के स्वरूप आदि में मानवीय दृष्टि से समरूपता है तो फिर चरित्र निर्माण के कार्य में एकरूपता क्यों नहीं लाई जा सकती है? इसमें बुरा मानने की बात नहीं है और यह कड़वा सच है कि यह एकरूपता नामधारी धर्मों की अपनी कट्टरता के कारण ही संभव नहीं हो पाती है। नामधारी धर्म नाम पहले चाहते हैं-काम हो या नहीं इसकी परवाह उन्हें कम रहती हैं। अतः आज का यह भी एक रचनात्मक कार्य कहलाएगा कि शुद्ध मानवीय मूल्यों के आधार पर किए जाने वाले सत्कार्यों के लिए सभी नामधारी धर्म वालों को सहमत किया जाए एवं उनसे सक्रिय सहयोग लिया जाए।
धर्म प्रवर्त्तकों का अन्तर्निहित लक्ष्य रहा चरित्र विस्तार से स्वतः चालित व्यवस्था का :
अब तक शायद इस बिन्दु पर बहुत कम सोचा गया है कि धर्म प्रवर्तन के समय उनके प्रवर्तकों का अन्तर्निहित लक्ष्य क्या रहा होगा? कौनसा प्रमुख उद्देश्य रहा होगा उनके मानस में कि धर्म के