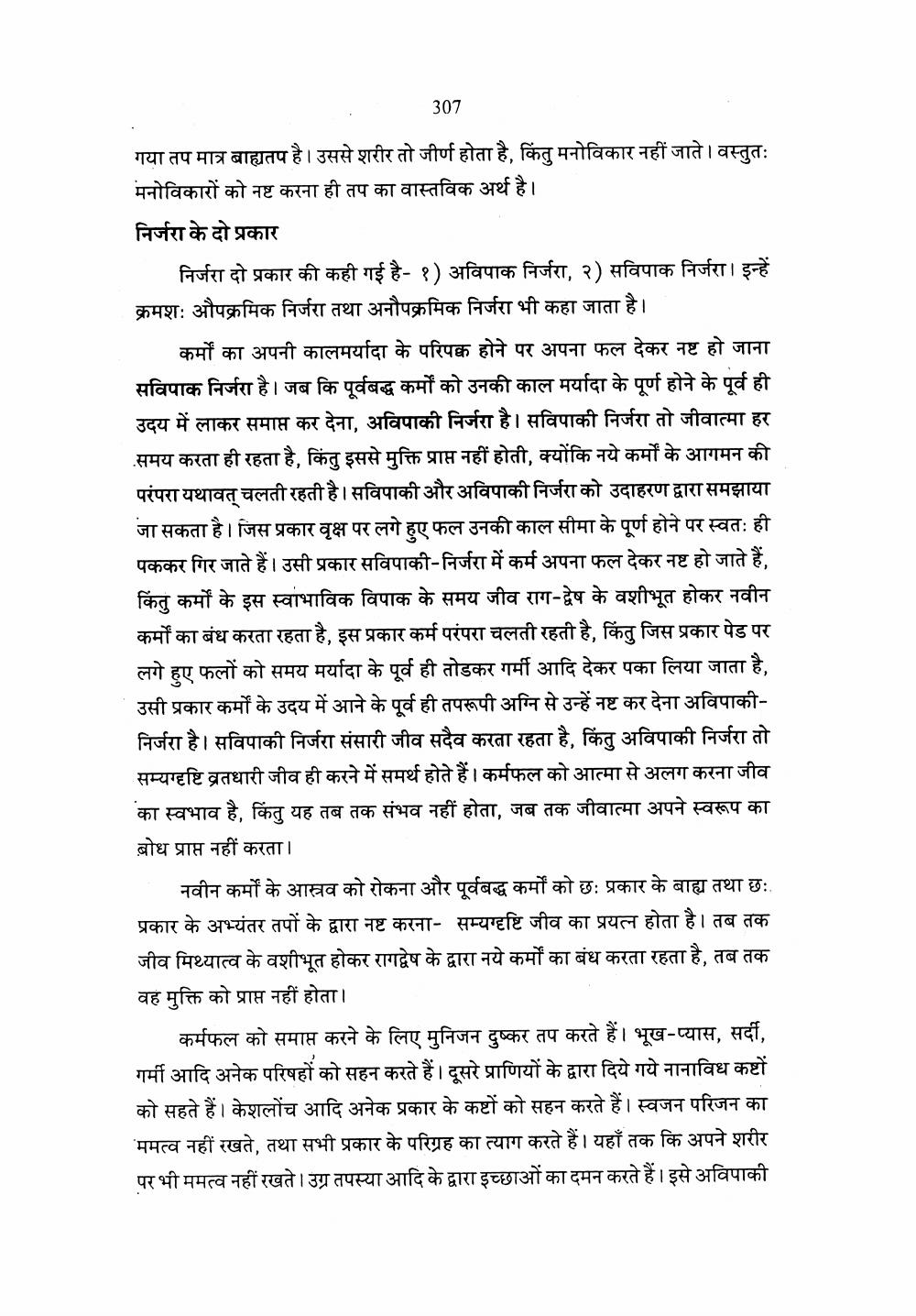________________
307
गया तप मात्र बाह्यतप है। उससे शरीर तो जीर्ण होता है, किंतु मनोविकार नहीं जाते। वस्तुत: मनोविकारों को नष्ट करना ही तप का वास्तविक अर्थ है। निर्जरा के दो प्रकार
निर्जरा दो प्रकार की कही गई है- १) अविपाक निर्जरा, २) सविपाक निर्जरा। इन्हें क्रमश: औपक्रमिक निर्जरा तथा अनौपक्रमिक निर्जरा भी कहा जाता है।
कर्मों का अपनी कालमर्यादा के परिपक्व होने पर अपना फल देकर नष्ट हो जाना सविपाक निर्जरा है। जब कि पूर्वबद्ध कर्मों को उनकी काल मर्यादा के पूर्ण होने के पूर्व ही उदय में लाकर समाप्त कर देना, अविपाकी निर्जरा है। सविपाकी निर्जरा तो जीवात्मा हर समय करता ही रहता है, किंतु इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि नये कर्मों के आगमन की परंपरा यथावत् चलती रहती है। सविपाकी और अविपाकी निर्जरा को उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। जिस प्रकार वृक्ष पर लगे हुए फल उनकी काल सीमा के पूर्ण होने पर स्वत: ही पककर गिर जाते हैं। उसी प्रकार सविपाकी-निर्जरा में कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं, किंतु कर्मों के इस स्वाभाविक विपाक के समय जीव राग-द्वेष के वशीभूत होकर नवीन कर्मों का बंध करता रहता है, इस प्रकार कर्म परंपरा चलती रहती है, किंतु जिस प्रकार पेड पर लगे हुए फलों को समय मर्यादा के पूर्व ही तोडकर गर्मी आदि देकर पका लिया जाता है, उसी प्रकार कर्मों के उदय में आने के पूर्व ही तपरूपी अग्नि से उन्हें नष्ट कर देना अविपाकीनिर्जरा है। सविपाकी निर्जरा संसारी जीव सदैव करता रहता है, किंतु अविपाकी निर्जरा तो सम्यग्दृष्टि व्रतधारी जीव ही करने में समर्थ होते हैं। कर्मफल को आत्मा से अलग करना जीव का स्वभाव है, किंतु यह तब तक संभव नहीं होता, जब तक जीवात्मा अपने स्वरूप का ब्रोध प्राप्त नहीं करता।
नवीन कर्मों के आस्रव को रोकना और पूर्वबद्ध कर्मों को छः प्रकार के बाह्य तथा छ: प्रकार के अभ्यंतर तपों के द्वारा नष्ट करना- सम्यग्दृष्टि जीव का प्रयत्न होता है। तब तक जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर रागद्वेष के द्वारा नये कर्मों का बंध करता रहता है, तब तक वह मुक्ति को प्राप्त नहीं होता।
कर्मफल को समाप्त करने के लिए मुनिजन दुष्कर तप करते हैं। भूख-प्यास, सर्दी, गर्मी आदि अनेक परिषहों को सहन करते हैं। दूसरे प्राणियों के द्वारा दिये गये नानाविध कष्टों को सहते हैं। केशलोंच आदि अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हैं। स्वजन परिजन का ममत्व नहीं रखते, तथा सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। यहाँ तक कि अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखते। उग्र तपस्या आदि के द्वारा इच्छाओं का दमन करते हैं। इसे अविपाकी