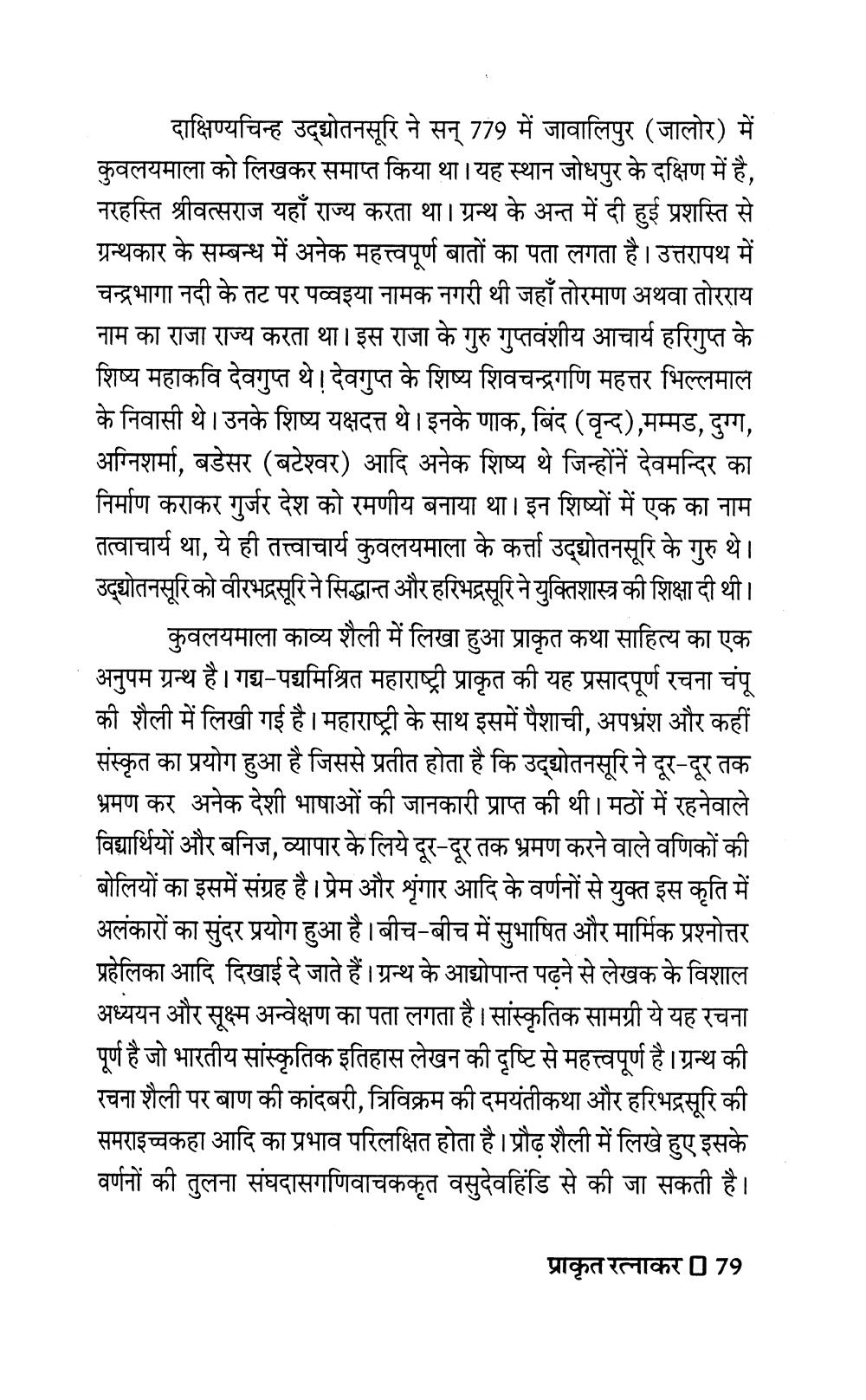________________
दाक्षिण्यचिन्ह उद्द्योतनसूरि ने सन् 779 में जावालिपुर (जालोर) में कुवलयमाला को लिखकर समाप्त किया था। यह स्थान जोधपुर के दक्षिण में है, नरहस्ति श्रीवत्सराज यहाँ राज्य करता था। ग्रन्थ के अन्त में दी हुई प्रशस्ति से ग्रन्थकार के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बातों का पता लगता है। उत्तरापथ में चन्द्रभागा नदी के तट पर पव्वइया नामक नगरी थी जहाँ तोरमाण अथवा तोरराय नाम का राजा राज्य करता था। इस राजा के गुरु गुप्तवंशीय आचार्य हरिगुप्त के शिष्य महाकवि देवगुप्त थे। देवगुप्त के शिष्य शिवचन्द्रगणि महत्तर भिल्लमाल के निवासी थे। उनके शिष्य यक्षदत्त थे। इनके णाक, बिंद (वृन्द),मम्मड, दुग्ग, अग्निशर्मा, बडेसर (बटेश्वर) आदि अनेक शिष्य थे जिन्होंने देवमन्दिर का निर्माण कराकर गुर्जर देश को रमणीय बनाया था। इन शिष्यों में एक का नाम तत्वाचार्य था, ये ही तत्त्वाचार्य कुवलयमाला के कर्ता उद्योतनसूरि के गुरु थे। उद्द्योतनसूरि को वीरभद्रसूरिने सिद्धान्त और हरिभद्रसूरि ने युक्तिशास्त्र की शिक्षा दी थी।
कुवलयमाला काव्य शैली में लिखा हुआ प्राकृत कथा साहित्य का एक अनुपम ग्रन्थ है। गद्य-पद्यमिश्रित महाराष्ट्री प्राकृत की यह प्रसादपूर्ण रचना चंपू की शैली में लिखी गई है। महाराष्ट्री के साथ इसमें पैशाची, अपभ्रंश और कहीं संस्कृत का प्रयोग हुआ है जिससे प्रतीत होता है कि उद्द्योतनसूरि ने दूर-दूर तक भ्रमण कर अनेक देशी भाषाओं की जानकारी प्राप्त की थी। मठों में रहनेवाले विद्यार्थियों और बनिज, व्यापार के लिये दूर-दूर तक भ्रमण करने वाले वणिकों की बोलियों का इसमें संग्रह है। प्रेम और शृंगार आदि के वर्णनों से युक्त इस कृति में अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। बीच-बीच में सुभाषित और मार्मिक प्रश्नोत्तर प्रहेलिका आदि दिखाई दे जाते हैं। ग्रन्थ के आद्योपान्त पढ़ने से लेखक के विशाल अध्ययन और सूक्ष्म अन्वेक्षण का पता लगता है। सांस्कृतिक सामग्री ये यह रचना पूर्ण है जो भारतीय सांस्कृतिक इतिहास लेखन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। ग्रन्थ की रचना शैली पर बाण की कांदबरी, त्रिविक्रम की दमयंतीकथा और हरिभद्रसूरि की समराइच्चकहा आदि का प्रभाव परिलक्षित होता है। प्रौढ़ शैली में लिखे हुए इसके वर्णनों की तुलना संघदासगणिवाचककृत वसुदेवहिडि से की जा सकती है।
प्राकृत रत्नाकर 079