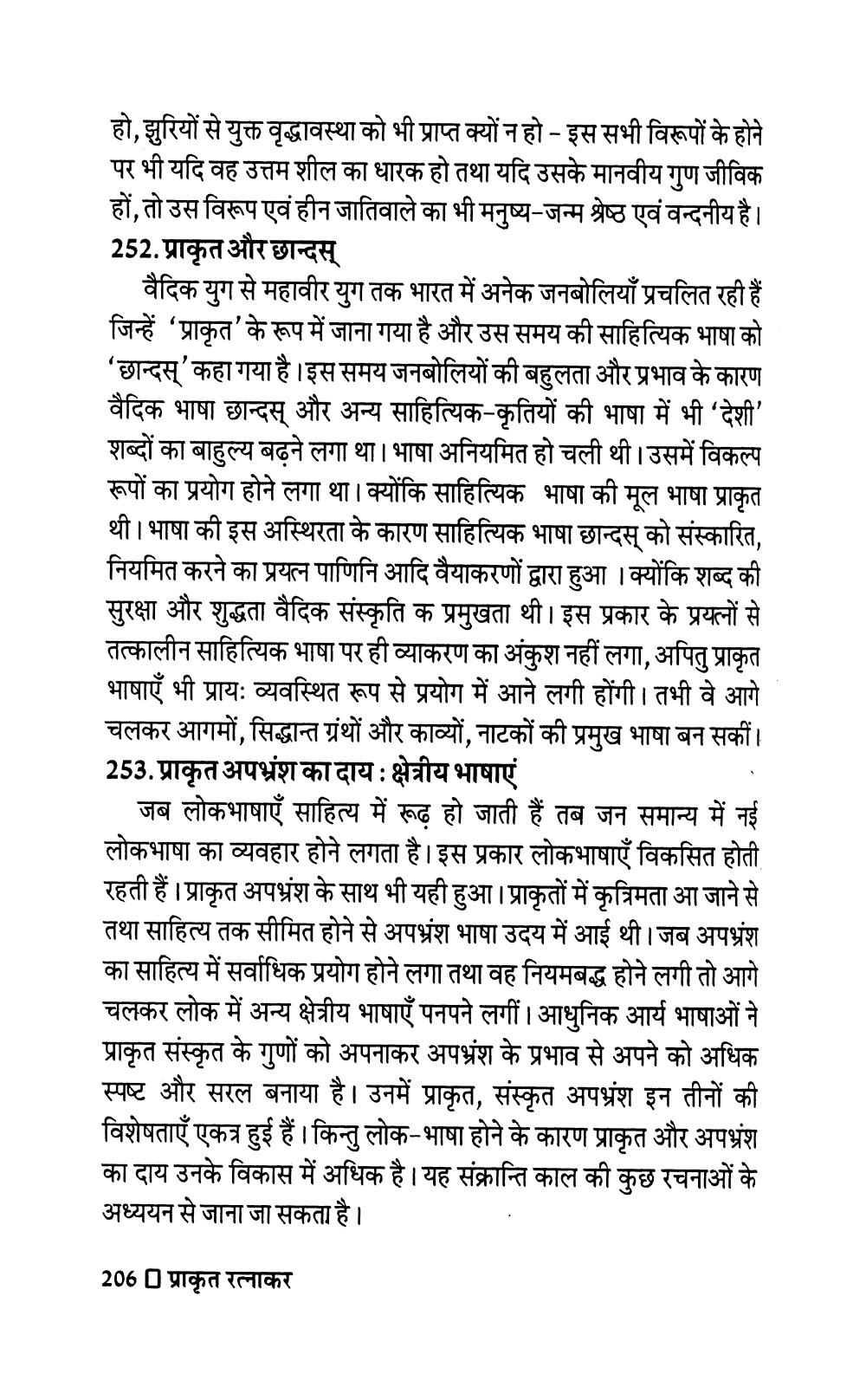________________
हो, झुरियों से युक्त वृद्धावस्था को भी प्राप्त क्यों न हो - इस सभी विरूपों के होने पर भी यदि वह उत्तम शील का धारक हो तथा यदि उसके मानवीय गुण जीविक हों, तो उस विरूप एवं हीन जातिवाले का भी मनुष्य-जन्म श्रेष्ठ एवं वन्दनीय है। 252. प्राकृत और छान्दस् __ वैदिक युग से महावीर युग तक भारत में अनेक जनबोलियाँ प्रचलित रही हैं जिन्हें 'प्राकृत' के रूप में जाना गया है और उस समय की साहित्यिक भाषा को 'छान्दस्' कहा गया है। इस समय जनबोलियों की बहुलता और प्रभाव के कारण वैदिक भाषा छान्दस् और अन्य साहित्यिक-कृतियों की भाषा में भी 'देशी' शब्दों का बाहुल्य बढ़ने लगा था। भाषा अनियमित हो चली थी। उसमें विकल्प रूपों का प्रयोग होने लगा था। क्योंकि साहित्यिक भाषा की मूल भाषा प्राकृत थी। भाषा की इस अस्थिरता के कारण साहित्यिक भाषा छान्दस् को संस्कारित, नियमित करने का प्रयत्न पाणिनि आदि वैयाकरणों द्वारा हुआ । क्योंकि शब्द की सुरक्षा और शुद्धता वैदिक संस्कृति क प्रमुखता थी। इस प्रकार के प्रयत्नों से तत्कालीन साहित्यिक भाषा पर ही व्याकरण का अंकुश नहीं लगा, अपितु प्राकृत भाषाएँ भी प्रायः व्यवस्थित रूप से प्रयोग में आने लगी होंगी। तभी वे आगे चलकर आगमों, सिद्धान्त ग्रंथों और काव्यों, नाटकों की प्रमुख भाषा बन सकीं। 253. प्राकृत अपभ्रंशकादाय: क्षेत्रीय भाषाएं
जब लोकभाषाएँ साहित्य में रूढ़ हो जाती हैं तब जन समान्य में नई लोकभाषा का व्यवहार होने लगता है। इस प्रकार लोकभाषाएँ विकसित होती रहती हैं। प्राकृत अपभ्रंश के साथ भी यही हुआ। प्राकृतों में कृत्रिमता आ जाने से तथा साहित्य तक सीमित होने से अपभ्रंश भाषा उदय में आई थी। जब अपभ्रंश का साहित्य में सर्वाधिक प्रयोग होने लगा तथा वह नियमबद्ध होने लगी तो आगे चलकर लोक में अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ पनपने लगीं। आधुनिक आर्य भाषाओं ने प्राकृत संस्कृत के गुणों को अपनाकर अपभ्रंश के प्रभाव से अपने को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया है। उनमें प्राकृत, संस्कृत अपभ्रंश इन तीनों की विशेषताएँ एकत्र हुई हैं। किन्तु लोक-भाषा होने के कारण प्राकृत और अपभ्रंश का दाय उनके विकास में अधिक है। यह संक्रान्ति काल की कुछ रचनाओं के अध्ययन से जाना जा सकता है।
206 0 प्राकृत रत्नाकर