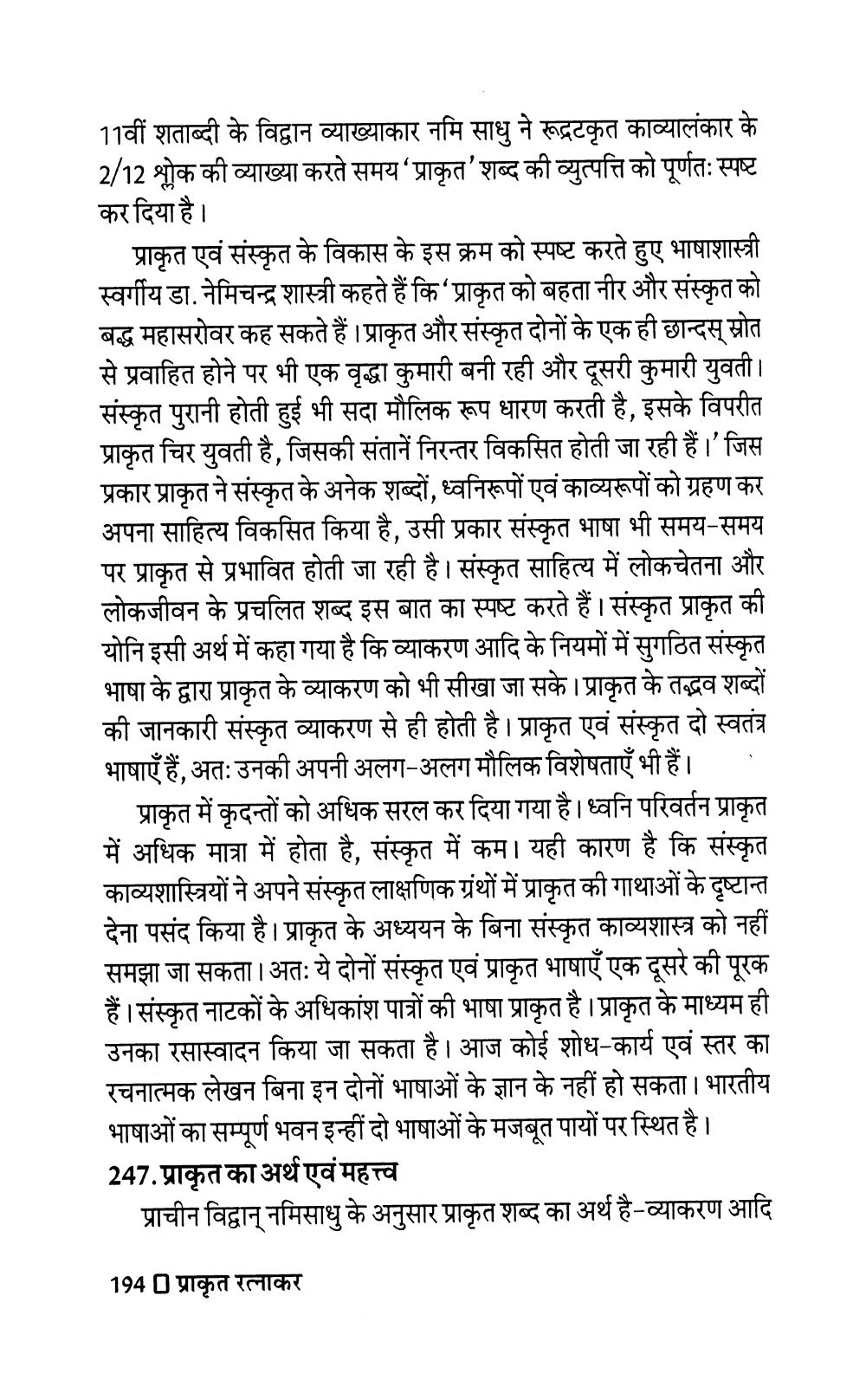________________
11वीं शताब्दी के विद्वान व्याख्याकार नमि साधु ने रूद्रटकृत काव्यालंकार के 2/12 शोक की व्याख्या करते समय ‘प्राकृत' शब्द की व्युत्पत्ति को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है।
प्राकृत एवं संस्कृत के विकास के इस क्रम को स्पष्ट करते हुए भाषाशास्त्री स्वर्गीय डा. नेमिचन्द्र शास्त्री कहते हैं कि प्राकृत को बहता नीर और संस्कृत को बद्ध महासरोवर कह सकते हैं। प्राकृत और संस्कृत दोनों के एक ही छान्दस् स्रोत से प्रवाहित होने पर भी एक वृद्धा कुमारी बनी रही और दूसरी कुमारी युवती। संस्कृत पुरानी होती हुई भी सदा मौलिक रूप धारण करती है, इसके विपरीत प्राकृत चिर युवती है, जिसकी संतानें निरन्तर विकसित होती जा रही हैं। जिस प्रकार प्राकृत ने संस्कृत के अनेक शब्दों, ध्वनिरूपों एवं काव्यरूपों को ग्रहण कर अपना साहित्य विकसित किया है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा भी समय-समय पर प्राकृत से प्रभावित होती जा रही है। संस्कृत साहित्य में लोकचेतना और लोकजीवन के प्रचलित शब्द इस बात का स्पष्ट करते हैं। संस्कृत प्राकृत की योनि इसी अर्थ में कहा गया है कि व्याकरण आदि के नियमों में सुगठित संस्कृत भाषा के द्वारा प्राकृत के व्याकरण को भी सीखा जा सके। प्राकृत के तद्भव शब्दों की जानकारी संस्कृत व्याकरण से ही होती है। प्राकृत एवं संस्कृत दो स्वतंत्र भाषाएँ हैं, अतः उनकी अपनी अलग-अलग मौलिक विशेषताएँ भी हैं। __ प्राकृत में कृदन्तों को अधिक सरल कर दिया गया है। ध्वनि परिवर्तन प्राकृत में अधिक मात्रा में होता है, संस्कृत में कम। यही कारण है कि संस्कृत काव्यशास्त्रियों ने अपने संस्कृत लाक्षणिक ग्रंथों में प्राकृत की गाथाओं के दृष्टान्त देना पसंद किया है। प्राकृत के अध्ययन के बिना संस्कृत काव्यशास्त्र को नहीं समझा जा सकता। अतः ये दोनों संस्कृत एवं प्राकृत भाषाएँ एक दूसरे की पूरक हैं। संस्कृत नाटकों के अधिकांश पात्रों की भाषा प्राकृत है। प्राकृत के माध्यम ही उनका रसास्वादन किया जा सकता है। आज कोई शोध-कार्य एवं स्तर का रचनात्मक लेखन बिना इन दोनों भाषाओं के ज्ञान के नहीं हो सकता। भारतीय भाषाओं का सम्पूर्ण भवन इन्हीं दो भाषाओं के मजबूत पायों पर स्थित है। 247. प्राकृत काअर्थ एवं महत्त्व
प्राचीन विद्वान् नमिसाधु के अनुसार प्राकृत शब्द का अर्थ है-व्याकरण आदि
1940 प्राकृत रत्नाकर