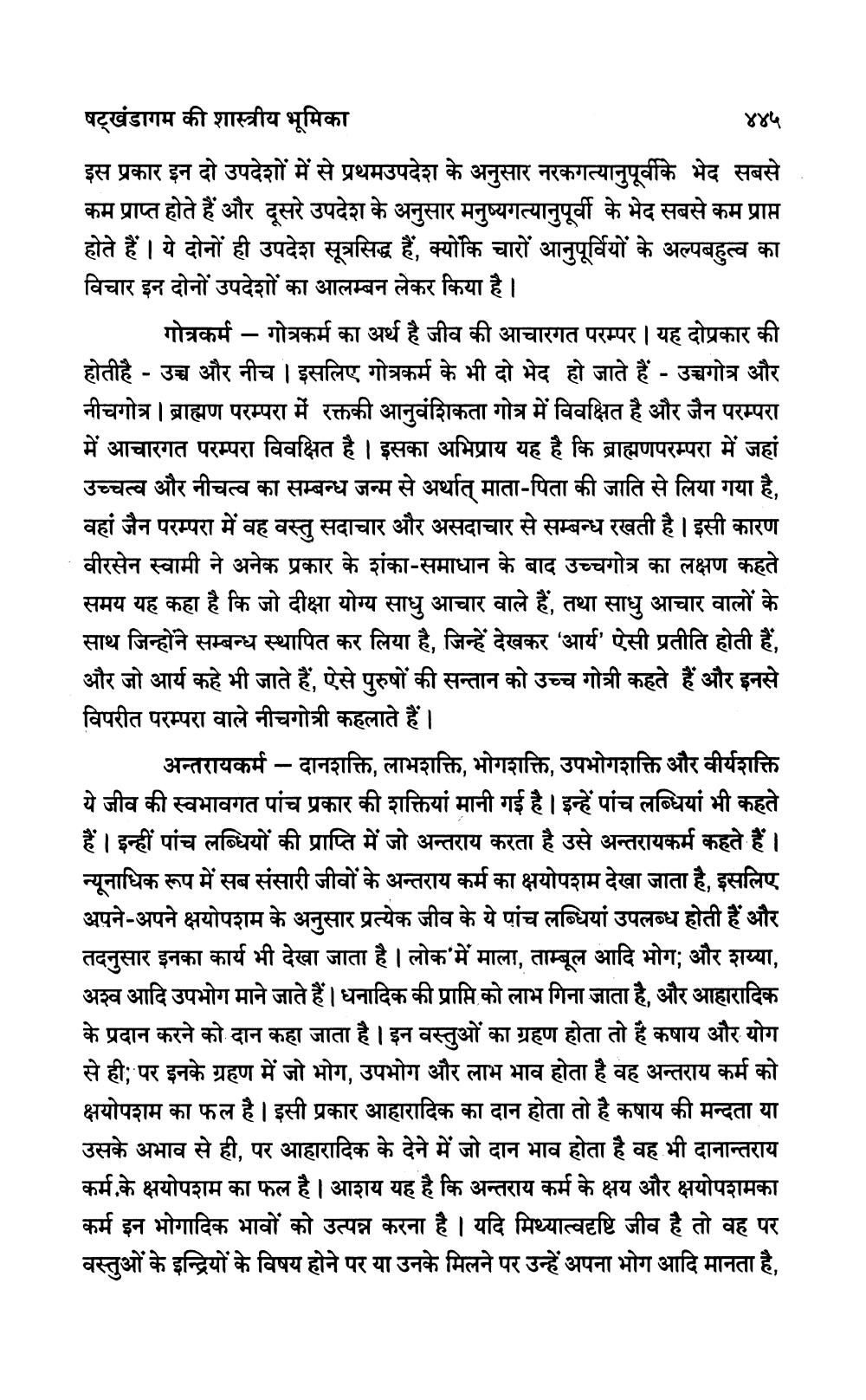________________
षट्खंडागम की शास्त्रीय भूमिका
४४५ इस प्रकार इन दो उपदेशों में से प्रथमउपदेश के अनुसार नरकगत्यानुपूर्वीके भेद सबसे कम प्राप्त होते हैं और दूसरे उपदेश के अनुसार मनुष्यगत्यानुपूर्वी के भेद सबसे कम प्राप्त होते हैं । ये दोनों ही उपदेश सूत्रसिद्ध हैं, क्योंकि चारों आनुपूर्वियों के अल्पबहुत्व का विचार इन दोनों उपदेशों का आलम्बन लेकर किया है।
गोत्रकर्म – गोत्रकर्म का अर्थ है जीव की आचारगत परम्पर । यह दोप्रकार की होतीहै - उच्च और नीच । इसलिए गोत्रकर्म के भी दो भेद हो जाते हैं - उच्चगोत्र और नीचगोत्र । ब्राह्मण परम्परा में रक्तकी आनुवंशिकता गोत्र में विवक्षित है और जैन परम्परा में आचारगत परम्परा विवक्षित है । इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणपरम्परा में जहां उच्चत्व और नीचत्व का सम्बन्ध जन्म से अर्थात् माता-पिता की जाति से लिया गया है, वहां जैन परम्परा में वह वस्तु सदाचार और असदाचार से सम्बन्ध रखती है । इसी कारण वीरसेन स्वामी ने अनेक प्रकार के शंका-समाधान के बाद उच्चगोत्र का लक्षण कहते समय यह कहा है कि जो दीक्षा योग्य साधु आचार वाले हैं, तथा साधु आचार वालों के साथ जिन्होंने सम्बन्ध स्थापित कर लिया है, जिन्हें देखकर 'आर्य' ऐसी प्रतीति होती हैं,
और जो आर्य कहे भी जाते हैं, ऐसे पुरुषों की सन्तान को उच्च गोत्री कहते हैं और इनसे विपरीत परम्परा वाले नीचगोत्री कहलाते हैं।
अन्तरायकर्म – दानशक्ति, लाभशक्ति, भोगशक्ति, उपभोगशक्ति और वीर्यशक्ति ये जीव की स्वभावगत पांच प्रकार की शक्तियां मानी गई है। इन्हें पांच लब्धियां भी कहते हैं । इन्हीं पांच लब्धियों की प्राप्ति में जो अन्तराय करता है उसे अन्तरायकर्म कहते हैं। न्यूनाधिक रूप में सब संसारी जीवों के अन्तराय कर्म का क्षयोपशम देखा जाता है, इसलिए अपने-अपने क्षयोपशम के अनुसार प्रत्येक जीव के ये पांच लब्धियां उपलब्ध होती हैं और तदनुसार इनका कार्य भी देखा जाता है । लोक में माला, ताम्बूल आदि भोग; और शय्या, अश्व आदि उपभोग माने जाते हैं। धनादिक की प्राप्ति को लाभ गिना जाता है, और आहारादिक के प्रदान करने को दान कहा जाता है । इन वस्तुओं का ग्रहण होता तो है कषाय और योग से ही; पर इनके ग्रहण में जो भोग, उपभोग और लाभ भाव होता है वह अन्तराय कर्म को क्षयोपशम का फल है । इसी प्रकार आहारादिक का दान होता तो है कषाय की मन्दता या उसके अभाव से ही, पर आहारादिक के देने में जो दान भाव होता है वह भी दानान्तराय कर्म के क्षयोपशम का फल है। आशय यह है कि अन्तराय कर्म के क्षय और क्षयोपशमका कर्म इन भोगादिक भावों को उत्पन्न करना है । यदि मिथ्यात्वदृष्टि जीव है तो वह पर वस्तुओं के इन्द्रियों के विषय होने पर या उनके मिलने पर उन्हें अपना भोग आदि मानता है,