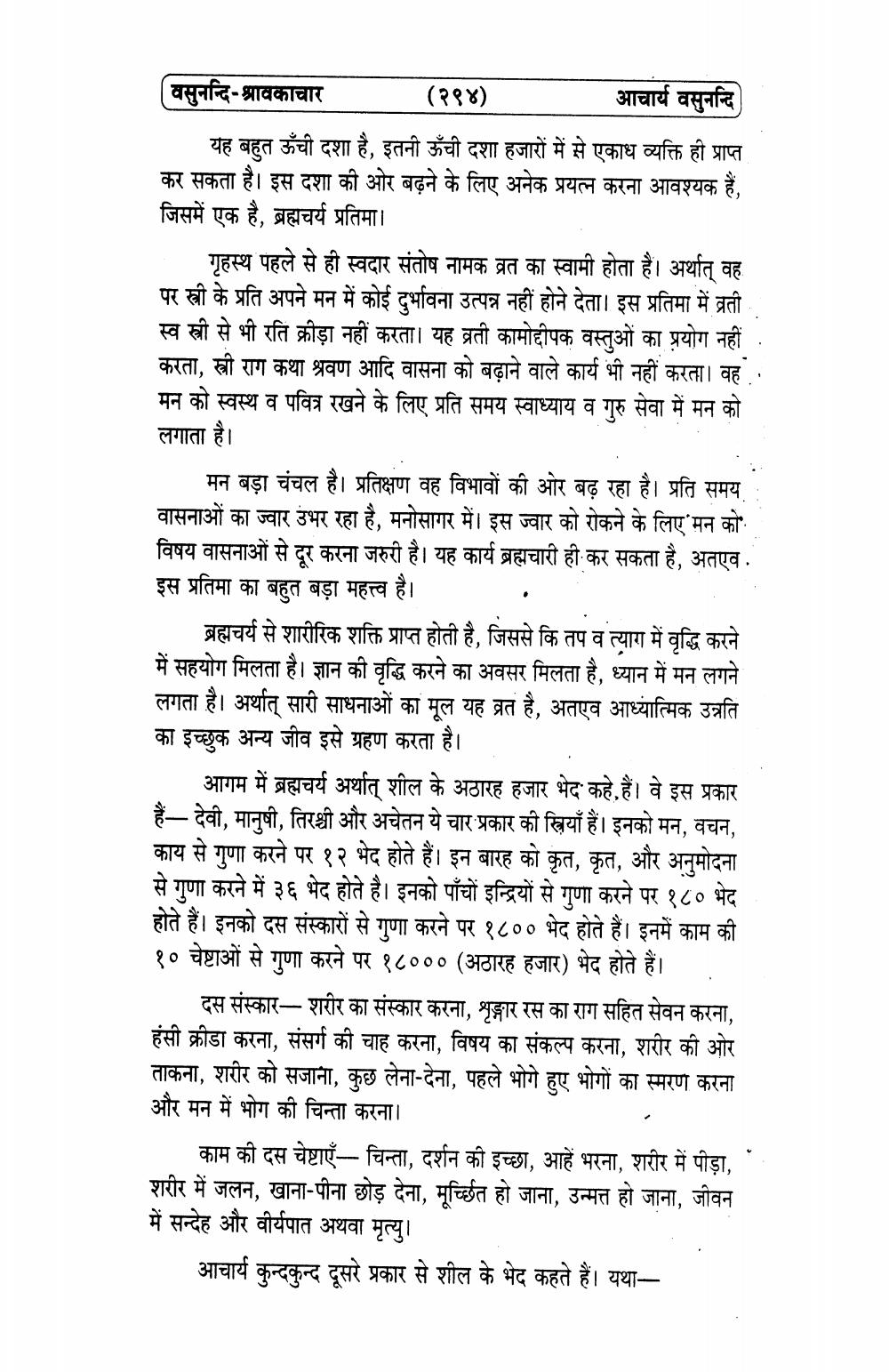________________
(वसुनन्दि-श्रावकाचार (२९४)
आचार्य वसुनन्दि यह बहुत ऊँची दशा है, इतनी ऊँची दशा हजारों में से एकाध व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। इस दशा की ओर बढ़ने के लिए अनेक प्रयत्न करना आवश्यक हैं, जिसमें एक है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा।
गृहस्थ पहले से ही स्वदार संतोष नामक व्रत का स्वामी होता है। अर्थात् वह पर स्त्री के प्रति अपने मन में कोई दुर्भावना उत्पन्न नहीं होने देता। इस प्रतिमा में व्रती . स्व स्त्री से भी रति क्रीड़ा नहीं करता। यह व्रती कामोद्दीपक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करता, स्त्री राग कथा श्रवण आदि वासना को बढ़ाने वाले कार्य भी नहीं करता। वह .. मन को स्वस्थ व पवित्र रखने के लिए प्रति समय स्वाध्याय व गुरु सेवा में मन को लगाता है।
मन बड़ा चंचल है। प्रतिक्षण वह विभावों की ओर बढ़ रहा है। प्रति समय : वासनाओं का ज्वार उभर रहा है, मनोसागर में। इस ज्वार को रोकने के लिए मन को विषय वासनाओं से दूर करना जरुरी है। यह कार्य ब्रह्मचारी ही कर सकता है, अतएव . इस प्रतिमा का बहुत बड़ा महत्त्व है।
ब्रह्मचर्य से शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कि तप व त्याग में वृद्धि करने में सहयोग मिलता है। ज्ञान की वृद्धि करने का अवसर मिलता है, ध्यान में मन लगने लगता है। अर्थात् सारी साधनाओं का मूल यह व्रत है, अतएव आध्यात्मिक उन्नति का इच्छुक अन्य जीव इसे ग्रहण करता है।
आगम में ब्रह्मचर्य अर्थात् शील के अठारह हजार भेद कहे, हैं। वे इस प्रकार हैं- देवी, मानुषी, तिरश्ची और अचेतन ये चार प्रकार की स्त्रियाँ हैं। इनको मन, वचन, काय से गुणा करने पर १२ भेद होते हैं। इन बारह को कृत, कृत, और अनुमोदना से गुणा करने में ३६ भेद होते है। इनको पाँचों इन्द्रियों से गुणा करने पर १८० भेद होते हैं। इनको दस संस्कारों से गुणा करने पर १८०० भेद होते हैं। इनमें काम की १० चेष्टाओं से गुणा करने पर १८००० (अठारह हजार) भेद होते हैं।
दस संस्कार- शरीर का संस्कार करना, शृङ्गार रस का राग सहित सेवन करना, हंसी क्रीडा करना, संसर्ग की चाह करना, विषय का संकल्प करना, शरीर की ओर ताकना, शरीर को सजाना, कुछ लेना-देना, पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण करना और मन में भोग की चिन्ता करना।
काम की दस चेष्टाएँ- चिन्ता, दर्शन की इच्छा, आहें भरना. शरीर में पीडा.. शरीर में जलन, खाना-पीना छोड़ देना, मूर्छित हो जाना, उन्मत्त हो जाना, जीवन में सन्देह और वीर्यपात अथवा मृत्यु।
आचार्य कुन्दकुन्द दूसरे प्रकार से शील के भेद कहते हैं। यथा