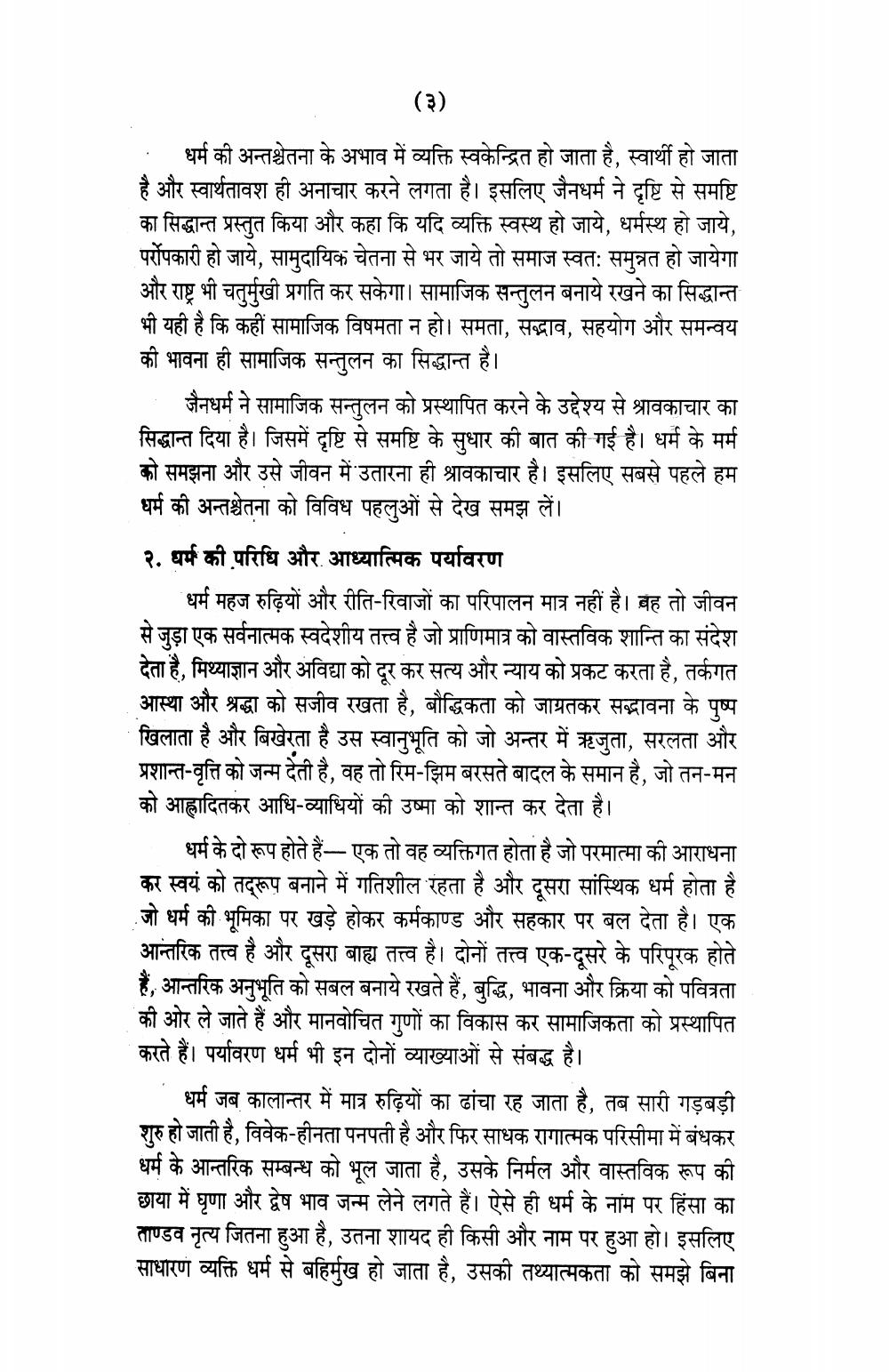________________
(३)
धर्म की अन्तश्चेतना के अभाव में व्यक्ति स्वकेन्द्रित हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है और स्वार्थतावश ही अनाचार करने लगता है। इसलिए जैनधर्म ने दृष्टि से समष्टि का सिद्धान्त प्रस्तुत किया और कहा कि यदि व्यक्ति स्वस्थ हो जाये, धर्मस्थ हो जाये, पर्रोपकारी हो जाये, सामुदायिक चेतना से भर जाये तो समाज स्वतः समुन्नत हो जायेगा और राष्ट्र भी चतुर्मुखी प्रगति कर सकेगा। सामाजिक सन्तुलन बनाये रखने का सिद्धान्त भी यही है कि कहीं सामाजिक विषमता न हो । समता, सद्भाव, सहयोग और समन्वय की भावना ही सामाजिक सन्तुलन का सिद्धान्त है ।
जैनधर्म ने सामाजिक सन्तुलन को प्रस्थापित करने के उद्देश्य से श्रावकाचार का सिद्धान्त दिया है। जिसमें दृष्टि से समष्टि के सुधार की बात की गई है। धर्म के मर्म को समझना और उसे जीवन में उतारना ही श्रावकाचार है। इसलिए सबसे पहले हम धर्म की अन्तश्चेतना को विविध पहलुओं से देख समझ लें ।
२. धर्म की परिधि और आध्यात्मिक पर्यावरण
धर्म मह रुढ़ियों और रीति-रिवाजों का परिपालन मात्र नहीं है। वह तो जीवन से जुड़ा एक सर्वनात्मक स्वदेशीय तत्त्व है जो प्राणिमात्र को वास्तविक शान्ति का संदेश देता है, मिथ्याज्ञान और अविद्या को दूर कर सत्य और न्याय को प्रकट करता है, तर्कगत आस्था और श्रद्धा को सजीव रखता है, बौद्धिकता को जाग्रतकर सद्भावना के पुष्प खिलाता है और बिखेरता है उस स्वानुभूति को जो अन्तर में ऋजुता, सरलता और प्रशान्त-वृत्ति को जन्म देती है, वह तो रिम झिम बरसते बादल के समान है, जो तन-मन को आह्लादितकर आधि-व्याधियों की उष्मा को शान्त कर देता है ।
धर्म के दो रूप होते हैं - एक तो वह व्यक्तिगत होता है जो परमात्मा की आराधना कर स्वयं को तद्रूप बनाने में गतिशील रहता है और दूसरा सांस्थिक धर्म होता है जो धर्म की भूमिका पर खड़े होकर कर्मकाण्ड और सहकार पर बल देता है। एक आन्तरिक तत्त्व है और दूसरा बाह्य तत्त्व है। दोनों तत्त्व एक-दूसरे के परिपूरक होते हैं, आन्तरिक अनुभूति को सबल बनाये रखते हैं, बुद्धि, भावना और क्रिया को पवित्रता की ओर ले जाते हैं और मानवोचित गुणों का विकास कर सामाजिकता को प्रस्थापित करते हैं। पर्यावरण धर्म भी इन दोनों व्याख्याओं से संबद्ध है।
धर्म जब कालान्तर में मात्र रुढ़ियों का ढांचा रह जाता है, तब सारी गड़बड़ी शुरु हो जाती है, विवेक-हीनता पनपती है और फिर साधक रागात्मक परिसीमा में बंधकर धर्म के आन्तरिक सम्बन्ध को भूल जाता है, उसके निर्मल और वास्तविक रूप की छाया में घृणा और द्वेष भाव जन्म लेने लगते हैं। ऐसे ही धर्म के नाम पर हिंसा का ताण्डव नृत्य जितना हुआ है, उतना शायद ही किसी और नाम पर हुआ हो। इसलिए साधारण व्यक्ति धर्म से बहिर्मुख हो जाता है, उसकी तथ्यात्मकता को समझे बिना