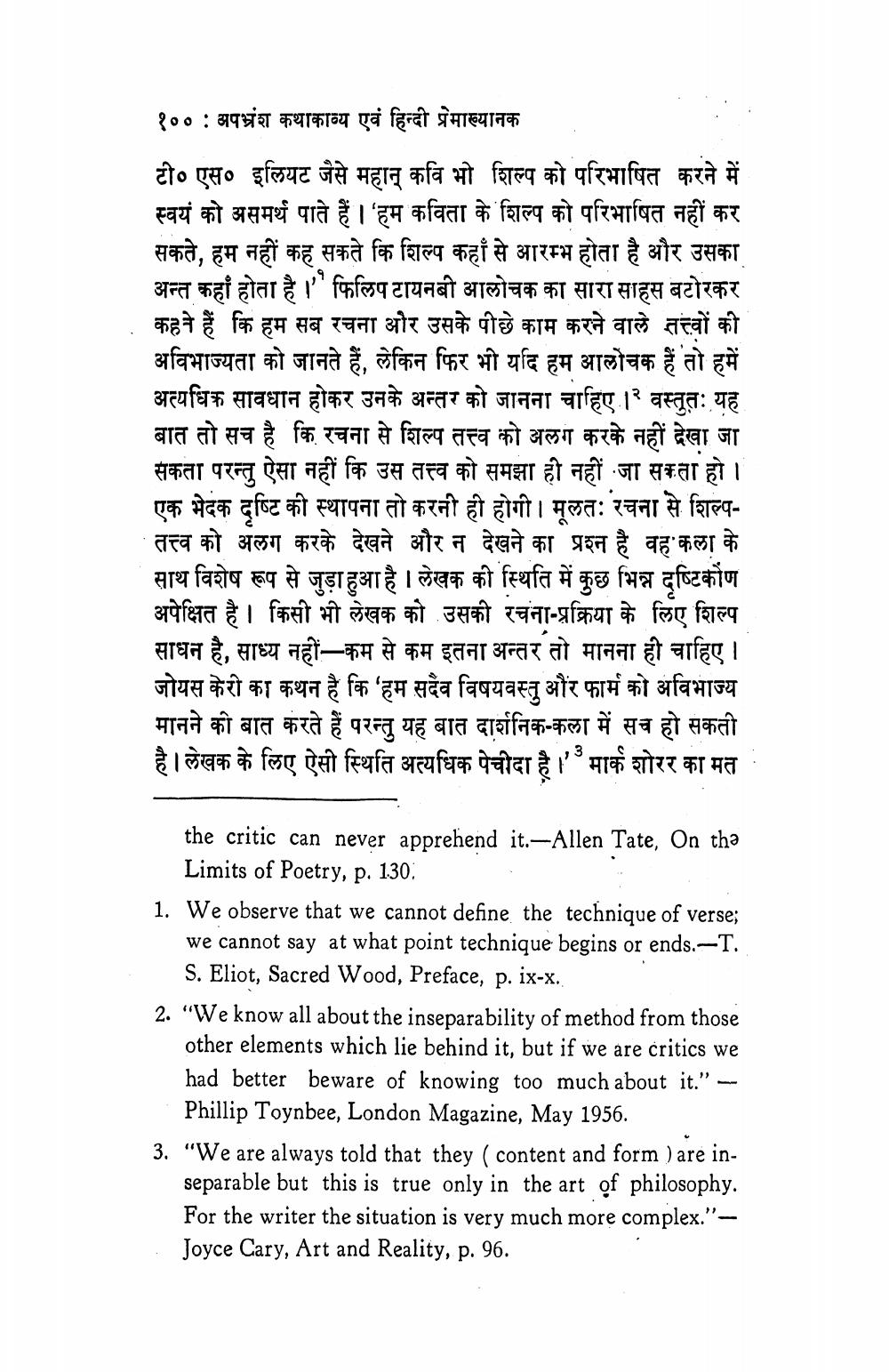________________
१०० : अपभ्रंश कथाकाव्य एवं हिन्दी प्रेमाख्यानक टी० एस० इलियट जैसे महान् कवि भो शिल्प को परिभाषित करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं । 'हम कविता के शिल्प को परिभाषित नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते कि शिल्प कहाँ से आरम्भ होता है और उसका अन्त कहाँ होता है । फिलिप टायनबी आलोचक का सारा साहस बटोरकर कहते हैं कि हम सब रचना और उसके पीछे काम करने वाले तत्त्वों की अविभाज्यता को जानते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम आलोचक हैं तो हमें अत्यधिक सावधान होकर उनके अन्तर को जानना चाहिए । वस्तुतः यह बात तो सच है कि रचना से शिल्प तत्त्व को अलग करके नहीं देखा जा सकता परन्तु ऐसा नहीं कि उस तत्त्व को समझा ही नहीं जा सकता हो । एक भेदक दृष्टि की स्थापना तो करनी ही होगी। मूलतः रचना से शिल्पतत्त्व को अलग करके देखने और न देखने का प्रश्न है वह कला के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है । लेखक की स्थिति में कुछ भिन्न दष्टिकोण अपेक्षित है। किसी भी लेखक को उसकी रचना-प्रक्रिया के लिए शिल्प साधन है, साध्य नहीं-कम से कम इतना अन्तर तो मानना ही चाहिए। जोयस केरी का कथन है कि 'हम सदैव विषयवस्तु और फार्म को अविभाज्य मानने की बात करते हैं परन्तु यह बात दार्शनिक-कला में सच हो सकती है। लेखक के लिए ऐसी स्थिति अत्यधिक पेचीदा है। मार्क शोरर का मत :
the critic can never apprehend it.-Allen Tate, On thə
Limits of Poetry, p. 130. 1. We observe that we cannot define the technique of verse;
we cannot say at what point technique begins or ends.-T.
S. Eliot, Sacred Wood, Preface, p. ix-x. 2. "We know all about the inseparability of method from those
other elements which lie behind it, but if we are critics we had better beware of knowing too much about it." —
Phillip Toynbee, London Magazine, May 1956. 3. "We are always told that they ( content and form ) are in
separable but this is true only in the art of philosophy. For the writer the situation is very much more complex.”— Joyce Cary, Art and Reality, p. 96.