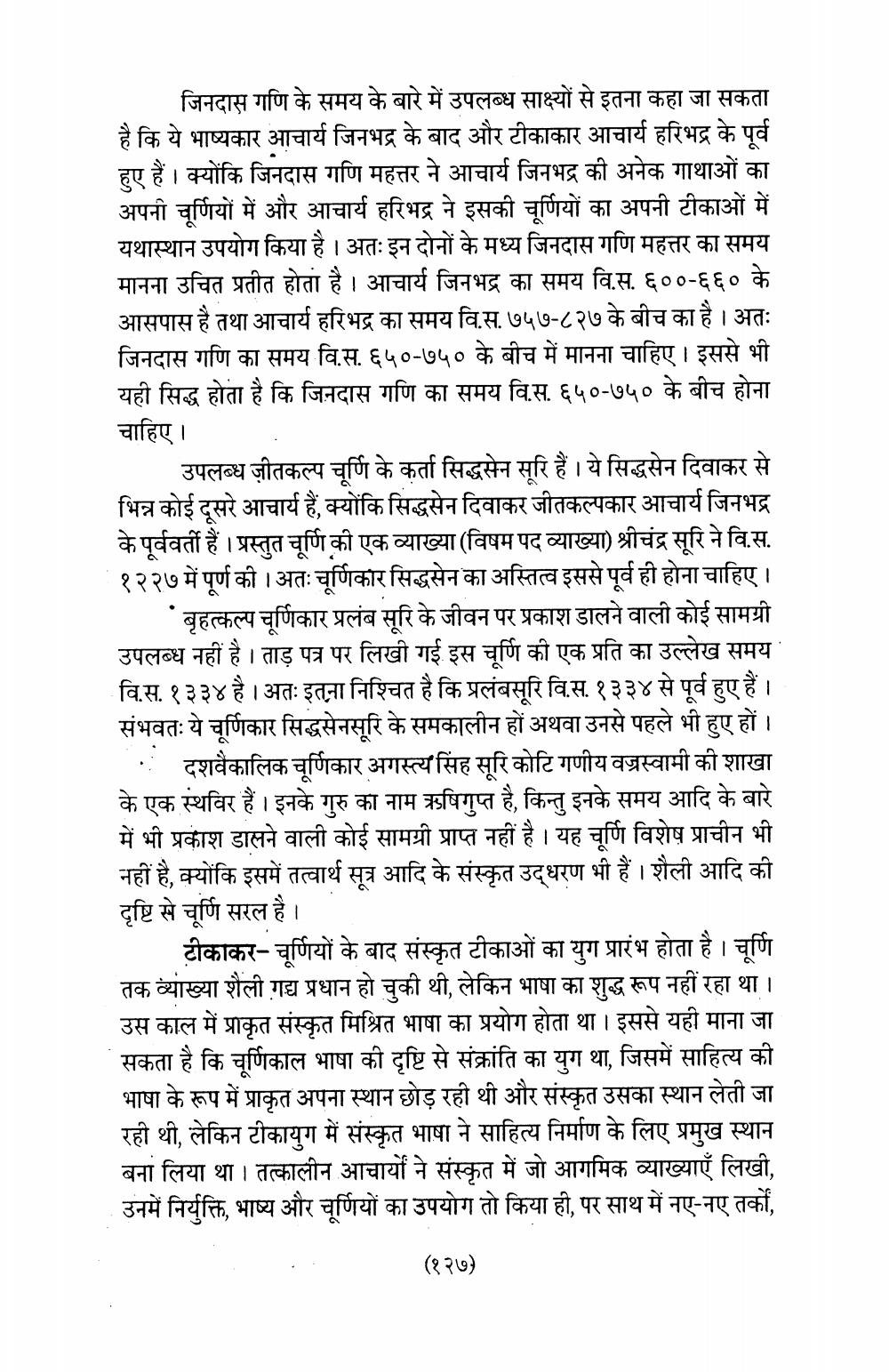________________
जिनदास गणि के समय के बारे में उपलब्ध साक्ष्यों से इतना कहा जा सकता है कि ये भाष्यकार आचार्य जिनभद्र के बाद और टीकाकार आचार्य हरिभद्र के पूर्व हुए हैं। क्योंकि जिनदास गणि महत्तर ने आचार्य जिनभद्र की अनेक गाथाओं का अपनी चूर्णियों में और आचार्य हरिभद्र ने इसकी चूर्णियों का अपनी टीकाओं में यथास्थान उपयोग किया है । अतः इन दोनों के मध्य जिनदास गणि महत्तर का समय मानना उचित प्रतीत होता है। आचार्य जिनभद्र का समय वि.स. ६००-६६० के आसपास है तथा आचार्य हरिभद्र का समय वि.स. ७५७-८२७ के बीच का है । अतः जिनदास गणि का समय वि.स. ६५०-७५० के बीच में मानना चाहिए । इससे भी यही सिद्ध होता है कि जिनदास गणि का समय वि.स. ६५०-७५० के बीच होना चाहिए ।
उपलब्ध जीतकल्प चूर्णि के कर्ता सिद्धसेन सूरि हैं । ये सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न कोई दूसरे आचार्य हैं, क्योंकि सिद्धसेन दिवाकर जीतकल्पकार आचार्य जिनभद्र पूर्ववर्ती हैं। प्रस्तुत चूर्णि की एक व्याख्या (विषम पद व्याख्या) श्रीचंद्र सूरि ने वि.स. १२२७ में पूर्ण की । अतः चूर्णिकार सिद्धसेन का अस्तित्व इससे पूर्व ही होना चाहिए ।
'बृहत्कल्प चूर्णिकार प्रलंब सूरि के जीवन पर प्रकाश डालने वाली कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है । ताड़ पत्र पर लिखी गई इस चूर्णि की एक प्रति का उल्लेख समय वि.स. १३३४ है । अतः इतना निश्चित है कि प्रलंबसूरि वि.स. १३३४ से पूर्व हुए हैं । संभवतः ये चूर्णिकार सिद्धसेनसूरि के समकालीन हों अथवा उनसे पहले भी हुए हों । दशवैकालिक चूर्णिकार अगस्त्य सिंह सूरि कोटि गणीय वज्रस्वामी की शाखा के एक स्थविर हैं । इनके गुरु का नाम ऋषिगुप्त है, किन्तु इनके समय आदि के बारे भी प्रकाश डालने वाली कोई सामग्री प्राप्त नहीं है। यह चूर्णि विशेष प्राचीन भी नहीं है, क्योंकि इसमें तत्वार्थ सूत्र आदि के संस्कृत उद्धरण भी हैं । शैली आदि की दृष्टि से चूर्णि सरल है ।
टीकाकर - चूर्णियों के बाद संस्कृत टीकाओं का युग प्रारंभ होता है । चूर्णि तक व्याख्या शैली गद्य प्रधान हो चुकी थी, लेकिन भाषा का शुद्ध रूप नहीं रहा था । उस काल में प्राकृत संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग होता था । इससे यही माना जा सकता है कि चूर्णिकाल भाषा की दृष्टि से संक्रांति का युग था, जिसमें साहित्य की भाषा के रूप में प्राकृत अपना स्थान छोड़ रही थी और संस्कृत उसका स्थान लेती जा रही थी, लेकिन टीकायुग में संस्कृत भाषा ने साहित्य निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बना लिया था । तत्कालीन आचार्यों ने संस्कृत में जो आगमिक व्याख्याएँ लिखी, उनमें नियुक्ति, भाष्य और चूर्णियों का उपयोग तो किया ही, पर साथ में नए-नए तर्कों,
(१२७)