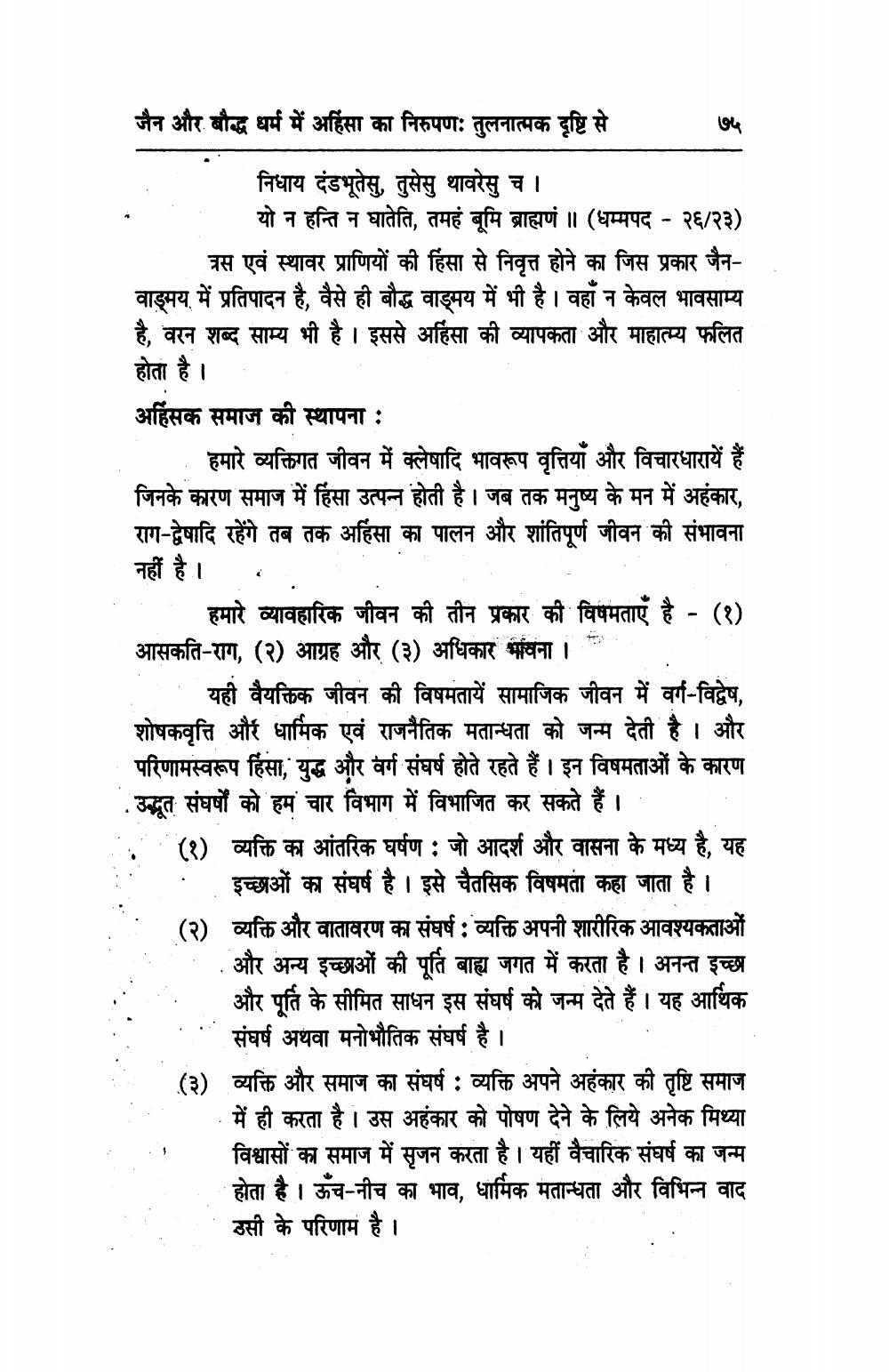________________
जैन और बौद्ध धर्म में अहिंसा का निरुपणः तुलनात्मक दृष्टि से
७५
निधाय दंडभूतेसु, तुसेसु थावरेसु च ।
यो न हन्ति न घातेति, तमहं बूमि ब्राह्मणं ॥ (धम्मपद - २६/२३) त्रस एवं स्थावर प्राणियों की हिंसा से निवृत्त होने का जिस प्रकार जैनवाङ्मय में प्रतिपादन है, वैसे ही बौद्ध वाङ्मय में भी है। वहाँ न केवल भावसाम्य है, वरन शब्द साम्य भी है। इससे अहिंसा की व्यापकता और माहात्म्य फलित होता है। अहिंसक समाज की स्थापना :
.. हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्लेषादि भावरूप वृत्तियाँ और विचारधारायें हैं जिनके कारण समाज में हिंसा उत्पन्न होती है। जब तक मनुष्य के मन में अहंकार, राग-द्वेषादि रहेंगे तब तक अहिंसा का पालन और शांतिपूर्ण जीवन की संभावना नहीं है।
हमारे व्यावहारिक जीवन की तीन प्रकार की विषमताएं है - (१) आसकति-राग, (२) आग्रह और (३) अधिकार भावना ।
यही वैयक्तिक जीवन की विषमतायें सामाजिक जीवन में वर्ग-विद्वेष, शोषकवृत्ति और धार्मिक एवं राजनैतिक मतान्धता को जन्म देती है । और परिणामस्वरूप हिंसा, युद्ध और वर्ग संघर्ष होते रहते हैं। इन विषमताओं के कारण उद्भूत संघर्षों को हम चार विभाग में विभाजित कर सकते हैं। . (१) व्यक्ति का आंतरिक घर्षण : जो आदर्श और वासना के मध्य है, यह
- इच्छाओं का संघर्ष है । इसे चैतसिक विषमता कहा जाता है । . (२) व्यक्ति और वातावरण का संघर्ष : व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं
. और अन्य इच्छाओं की पूर्ति बाह्य जगत में करता है । अनन्त इच्छा .. और पूर्ति के सीमित साधन इस संघर्ष को जन्म देते हैं । यह आर्थिक
संघर्ष अथवा मनोभौतिक संघर्ष है । (३) व्यक्ति और समाज का संघर्ष : व्यक्ति अपने अहंकार की तृष्टि समाज
. में ही करता है। उस अहंकार को पोषण देने के लिये अनेक मिथ्या विश्वासों का समाज में सृजन करता है। यहीं वैचारिक संघर्ष का जन्म होता है। ऊंच-नीच का भाव, धार्मिक मतान्धता और विभिन्न वाद उसी के परिणाम है।